|
इडियन एक्सप्रेस में 10 दिसम्बर 2015 को प्रकाशित इतिहासकार रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित 'भागवत के आंबेडकर' लेख रुचिपूर्वक पढ़ा। अचंभा हुआ अचंभित ये जानकर कि इतिहासकार केवल अतीत में रुचि रखते हैं जबकि उन्हें वर्तमान में भी उसी प्रकार रुचि रखनी चाहिए। लेकिन यदि समाज और सामाजिक संस्थान अतीत के द्वारा, वर्तमान के माध्यम से भविष्य को जानने के सुविज्ञ सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो क्या होगा। हिन्दू समाज कई युगों से इसी अनुकरणीय सिद्धांत का पालन करता आया है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एकदम सही कहा है- 'हिन्दुत्व एक आंदोलन है, कोई सत्ता नहीं, प्रक्रिया नहीं और न ही परिणाम यह एक विकसित होती प्रक्रिया है। यह कोई बंधी हुई अवधारणा नहीं है'(हिन्दू व्यू ऑफ लाइफ)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हिन्दुत्व के एक सशक्त अनुकर्ता के रूप में इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ा है।
यहां पहले कुछ तथ्यों पर विचार किया जाय-
1. पूर्वाग्रह से ग्रस्त लेखक ने लिखा है- 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न तो नमक सत्याग्रह में भाग लिया और न ही भारत छोड़ो आंदोलन में'। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? अनजान हैं, जैसे मैं। मैं सोचता हूं यह 1930 में हुआ था। रा.स्व.संघ के स्वयंसेवकों की औसत आयु उस समय 15-16 वर्ष होनी चाहिए। क्या उनसे उस सत्याग्रह में भाग लेने के लिए अपेक्षा की जाएगी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि श्रीमान गुहा जी, रा.स्व.संघ के संस्थापक डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार ने विदर्भ में जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था जो कि नमक सत्याग्रह के समान ही था। उन्हें बंदी बनाया गया था और 9 महीने के कड़े कारावास में भेजा गया था। श्री हेडगेवार के विषय में कुछ तथ्य जानने जरूरी होंगे-वे बचपन से ही क्रांतिकारी थे। उन्हें विद्यालय निरीक्षक के स्वागत में वंदेमातरम् का नारा लगाने के लिए विद्यालय से निष्कासित किया गया था। दसवीं परीक्षा के बाद वे कलकत्ता चले गए जहां से वे चिकित्सक बनकर ही लौटे। उन्होंने बंबई की अपेक्षा कलकत्ता में रहने को प्राथमिकता दी। जो तुलनात्मक दृष्टि से नागपुर से नजदीक पड़ता था। इसका कारण जानना बहुत सरल है। कलकत्ता से लौटकर वे कांग्रेस से जुड़ गए और उसके बाद ब्रिटिश विरोधी भाषणों के कारण उन्हें कठोर कारावास दिया गया। वे राज्य कांग्रेस समिति के सचिव थे और 1920 में नागपुर में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सत्र में स्वयंसेवक दल के प्रमुख थे।
2. जहां तक 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात है। मैं श्री गुहा का ध्यान इस ओर ले जाने का आग्रह करता हूं कि गांधीजी नहीं चाहते थे कि यह आंदोलन अगस्त में शुरू हो। उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए पूरे छह महीने का समय दिया था। अंग्रेज जानते थे कि गांधीजी ने उन्हें छह महीने का समय बिस्तर बांधने के लिए नहीं दिया बल्कि वे अपने आंदोलन को संगठित करने के लिए ये समय ले रहे हैं। मेरे दिमाग में एक संदर्भ है लेकिन मैं उसे यथावत् रूप में यहां उद्धृत नहीं कर सकता। मैं श्री गुहा से निवेदन करूंगा कि उन गोपनीय पत्रों को खंगालने का काम करें जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 'सत्ता का हस्तातंरण' शीर्षक से दिये गये थे और जो 1972 में प्रकाशित भी हो चुके हैं। एक पत्र में उस समय के यू.पी. (संयुक्त प्रांत) के गवर्नर ने ब्रिटिश वायसराय को लिखा था कि फरवरी-मार्च 1943 में जब सुभाषचंद्र बोस पूर्व से भारत पर आक्रमण करेंगे तब भारत में गांधीजी एक हिंसक आंदोलन प्रारंभ करने की योजना बनाएंगे। आपने अगस्त तक छह महीने जोड़े और आपको फरवरी 1943 मिल गया। उस समय ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने का निश्चय किया और उसी क्रम में योजनाबद्ध ढंग से कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी की योजना बनायी। सभी के गिरफ्तारी वारंट तैयार थे। कांग्रेस के नेताओं को धर-दबोचने की तैयारी पहले से ही थी। इन गिरफ्तारियों के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया लेकिन उसका दमन कर दिया गया। इसमें कहीं भी संगठित अखिल भारतीय योजना नहीं दिखायी दी। यह बिहार में तो पूरी तरह से फैला लेकिन संयुक्त प्रांत में नहीं, इसी प्रकार दक्षिण महाराष्ट्र के सतारा में इसका असर दिखा किंतु पुणे में नहीं। विदर्भ, चिमूर जो कि अब एक तहसील है एक हिंसक वारदात का गवाह बना। जबकि चंद्रपुर नामक जिला तुलनात्मक दृष्टि से बहुत शांतिपूर्ण रहा। यदि गांधीजी को समय मिलता तो वे पूरी योजना और संगठित ढंग से शायद रा.स्व.संघ से भी संपर्क कर सकते थे। जबकि संघ के स्वयंसेवकों ने अपने स्तर पर इस आंदोलन में भाग लिया। चिमूर आंदोलन में जो सक्रिय पाए गए थे उन्हें मौत की सजा सुनायी गयी जिनमें रा.स्व.संघ के कार्यकर्ता भी शामिल थे। रामटेक (नागपुर जिला) में जो व्यक्ति सरकारी भवन पर तिरंगा लहरा रहा था वह रा.स्व. संघ का स्वयंसेवक था। जब श्रीमती अरुणा आसफ अली भूमिगत हुईं तो उन्हें हंसराज गुप्ता ने दिल्ली में अपने घर में शरण दी थी। (श्री गुप्ता बाद में रा.स्व.संघ की दिल्ली इकाई के प्रमुख बने), सतारा के श्री नाना पाटिल जिन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन को कई दिन तक आगे बढ़ाया और पंडित सातवलेकर के घर में भूमिगत रहे वे बाद में नजदीकी कस्बे के संघचालक बने।
अब डॉ. आंबेडकर के विषय में
लेखक लिखता है कि रा.स्व.संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों ने 1949-1951 तक डॉ. आंबेडकर का पूरी तरह विरोध किया। प्रश्न यह उठता है कि 1949 से 1951 के बीच रा.स्व.संघ से जुड़ी कौन सी संस्थाएं थीं। मुझे यह जानकर बेहद खुशी होगी यदि लेखक अपने दुराग्रह से भी हमारे अज्ञात संकायों पर कुछ प्रकाश डाल देते। जनसंघ 1951 में प्रारंभ हुआ था। रा.स्व.संघ को 'हिन्दू कोड बिल' के विरोध के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है। क्या शंकराचार्य रा.स्व.संघ के सदस्य थे? जो लोग हिन्दू धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे वे आपको सूचित कर देंगे कि शंकराचार्यों, महंतों और मठाधिपतियों को एक मंच पर लाना कितना कठिन कार्य है। यह केवल 1964 में संभव हुआ वह भी रा.स्व.संघ के प्रयासों से। वे सब एक मंच पर आए और उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए यह घोषणा की कि अस्पृश्यता को हमारा धर्म मंजूर नहीं करता। उस समय नारा था- सभी हिन्दू भाई हैं कोई भी पतित नहीं होना चाहिए- 'हिन्दव: सोदरा सर्वे, न हिन्दू पतितो भवेत्।'
यह सत्य है कि रा.स्व.संघ विभाजन के खिलाफ था। लेकिन जनसंख्या की अदला-बदली का प्रस्ताव हमने नहीं किया था। उस समय डॉ. आंबेडकर ने ही जनसंख्या की अदला-बदली का प्रस्ताव दिया था। श्री गुहा को विभाजन पर केन्द्रित डॉ. आंबेडकर की पुस्तक को पढ़ना चाहिए और सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए।
यह भी एक तथ्य है कि रा.स्व.संघ भी जानता था कि महात्मा गांधी विभाजन को रोकने में समर्थ नहीं हो सकते थे। 1946 के चुनावों में कांग्रेस के घोषणापत्र का मुख्य बिन्दु अखंड भारत था। जबकि मुस्लिम लीग का विभाजन। मुस्लिम लीग और तो और एनडब्ल्यूएफपी में भी बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी थी। जहां 95 प्रतिशत जनसंख्या मुसलमानों की थी लेकिन कांग्रेस ने वहां बड़ी चतुराई से जीत हासिल की। इसी प्रकार पंजाब में मुस्लिम लीग को यूनियनिस्ट पार्टी ने धूल चटा दी। महात्मा गांधी ने कहा था- 'देश का विभाजन मेरी लाश के ऊपर होगा'। उसके बाद जो कुछ घटा वह एक रहस्य है। और जनमत को धोखा देकर कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया। रा.स्व.संघ की दैनिक शाखाओं में एकात्मता स्त्रोत्र (एकता का मंत्र) गाया जाता है। यह सबसे पहले पिछली शताब्दी के पंाचवें दशक में शुरू किया गया था। उस समय यह 'प्रात: स्मरण' के नाम से जाना जाता था जिसका अर्थ था एक अच्छी सुबह की कामना। यह पुराने श्लोकों (पदों) का संग्रह है। इसमें प्राचीन संतों, योद्धाओं और अवतारों की प्रार्थना है। सत्तर के दशक में इसे संशोधित किया गया और एकात्मता स्त्रोत्र नाम दिया गया। इसमें आधुनिक भारत के महापुरुषों जैसे- रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, रवीन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, दादाभाई नौरोजी, असम के गोपबंधु, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, रमन महर्षि, पंडित मदनमोहन मालवीय, सुब्रह्मण्य भारती, सुभाषचंद्र बोस, प्रणवानंद, वीर सावरकर, ठक्करभाई, डॉ. भीमराव आंबेडकर, महात्मा फुले, केरल के नारायण गुरु और अंत में डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार और पूजनीय गुरुजी इत्यादि के नाम जोड़े गए। डॉ.आंबेडकर की महानता रा.स्व.संघ 2015 में उजागर नहीं कर रहा है। ये नई स्तुतियां आपातकाल के दौरान जोड़ी गयी थीं। यह स्वीकार करना चाहिए कि रा.स्व.संघ को समझना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये वर्तमान समय में विद्यमान दलीय संस्थानों की तरह किसी प्रतिरूप या सांचे में सटीक नहीं बैठता। रा.स्व.संघ अपने में अपूर्व है। रा.स्व.संघ को जानने के लिए आपको अपना दिमाग पूर्वाग्रहों से मुक्त करना होगा। यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि रा.स्व.संघ का लक्ष्य 'संपूर्ण' समाज को संगठित करना है। 'संपूर्ण' शब्द बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। समाज एक जटिल अस्तित्व का प्रतीक है। यह विविध गतिविधियों से चलता है। राजनीति भी उनमें से एक है लेकिन केवल एक नहीं। शिक्षा, धर्म, श्रम, कृषि, स्वास्थ्य, सहकारिता और कई अन्य अलग-अलग सामाजिक व्यवहार के क्रियाकलाप हैं। संपूर्ण समाज को संगठित करने का अर्थ है सामाजिक जीवन के इन सभी क्षेत्रों को संगठित करना, और रा.स्व.संघ क्रमश: इन सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है। रा.स्व.संघ कोई राजनीतिक दल नहीं है, यह एक सांस्कृतिक संगठन है। सांस्कृतिक का अर्थ है एक निश्चित मूल्य परंपरा। हम संस्कृति को नृत्य, नाटक, संगीत इत्यादि की बंधी सीमा में समझते हैं। ऐसा नहीं है, संस्कृति मूल्य परंपरा है। एक ऐसी प्रणाली जो राष्ट्रवाद पर आधारित है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक आवधारणा है। एक नस्ल, एक धर्म, एक भाषा किसी राष्ट्र के एक बनने की अनिवार्य शर्त नहीं है।
राष्ट्र और राज्य दो अलग-अलग अवधारणा हैं। इन दोनों के बीच में जरूरी अंतर को विश्लेषित करने के लिए एक और निबंध की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार धर्म और रिलीजन को समझने के लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा। 'हिन्दुत्व रिलीजन नहीं है' जैसा कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है- यह कई धर्मों की एक समेकित पूंजी है।' और वास्तव में यह रिलीजन से अधिक बड़ा है। धर्म इहलोक और परलोक दोनों से जुड़ा हुआ है। वह दोनों ही रूपों में है- भौतिक रूप में भी और उसी प्रकार आध्यात्मिक रूप में भी।
मा.गो. वैद्य











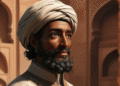
टिप्पणियाँ