भारतीय समाज-साहित्य का अंतर्संबंध
|
विख्यात राष्ट्रवादी चिंतक डा. ब्रह्मदत्त अवस्थी अपने प्रखर और गंभीर विचारों के लिए जाने जाते हैं। उनके चिंतन का आकाश अत्यंत विस्तृत है। इसके अंतर्गत केवल समाज और देश ही नहीं बल्कि साहित्य, राजनीति और आर्थिक पक्ष भी सम्मिलित रहते हैं। उनका चिंतन प्रवाह जाति और वर्ग से ऊपर उठकर लोक कल्याण पर आधारित रहता है। डा. अवस्थी के ऐसे ही कुछ गंभीर चिंतनशील निबंधों का संग्रह 'साहित्य, समाज और भारतीयता' कुछ समय पूर्व प्रकाशित होकर आया है। समीक्ष्य पुस्तक में लेखक देश के गौरवमयी अतीत का स्मरण करते हुए वर्तमान दशा पर गहन चिंतन कराते हैं और फिर भविष्य का भी विचार है। जहां अतीत को याद करते हुए लेखक को गर्वानुभूति होती है वहीं वर्तमान लोकतांत्रिक-सामाजिक-राजनीतिक दशा पर क्षोभ होता है। सांस्कृतिक शैली में विभिन्न विषयों पर आत्म-स्फूर्त प्रवाह से लिखे गए ये निबंध किसी भी चेतना संपन्न पाठक को सम्मोहित करने की क्षमता रखते हैं।
पुस्तक में कुल इक्कीस निबंध संकलित हैं। पहले ही निबंध 'अपनी धरती के आकाश तले' में तमाम तरह की सामाजिक विषमताओं के बाद भी वे आह्वान करते हैं; 'हम अपनी राह पर चलें, अपने को पहचानें, अपने स्वभाव को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों। अपना तंत्र हो, अपना मंत्र हो, अपनी धरा हो और उस पर अपना कर्म हो। अपने आकाश के तले अपने पसीने से वैभव की खेती उगायें, और अपने राष्ट्र मन्दिर में अपने विराट पुरुष की आरती उतारें।' अगले अध्याय 'अकर्मण्यता की जंजीरों में जकड़ा देश' में कर्म की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लेखक कहते हैं; 'कर्म जोड़ने वाला तत्व है। समाज की आधारशिला है कर्म। समाज के सम्बंध कर्म की डोर से बंधे हैं। कर्म न करने वाला व्यक्ति समाज को तोड़ता है, जोड़ता नहीं। इसीलिए तो कर्म समाज का पावन धर्म है।' वहीं कर्म और अकर्म के भेद को लेखक अगले अध्याय 'लोक कर्त्तव्य के निर्वाह का साधन' में स्पष्ट करते हैं। वे लिखते हैं, 'व्यर्थ है वह कर्म जो कुछ दे न सका। व्यर्थ है वह जीवन जो न बना, न बना सका। व्यर्थ है वह व्यवस्था, जो न बंधी, न बांध सकी। कर्म का, जीवन का, व्यवस्था का कुछ मूल्य है। मूल्य न रहा तो कर्म कैसा?' इसी तरह 'राष्ट्र-स्वरूप! साधना!! समस्या!!!' शीर्षक अध्याय में लेखक ने नीति और नैतिकता को बहुत सरल ढंग से स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं, 'व्यक्ति का पूर्ण विकास हो, समाज का स्वस्थ स्वरूप निखरे, विश्व को दिशा मिले, इसी लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला मार्ग ही नीति है। व्यक्ति की श्रेष्ठ धारणा जिन गुणों से हो, समाज का उत्कर्ष जिन मूल्यों से हो-और विश्व का हित जिन आदर्शों से हो-वही गुण, वही मूल्य और वही आदर्श हैं हमारी नीति के। उन्हीं का पालन करना है-नैतिकता।'
आज के समाज, लोकतंत्र और देश में श्रीराम की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए लेखक कहते हैं, 'लोकतंत्र के लिए लोक-आराध्य राम का आदर्श स्वीकारें। समाजवाद के लिए समाजहित पूर्ण समर्पित राम का जीवन देखें। आज हम देश की अखण्डता के लिए उन्हीं का आराधन करें।' भारतीय समाज की वास्तविक छवि को साहित्य के द्वारा प्रस्तुत करने वाले साहित्यकारों की चर्चा करते हुए लेखक मानते हैं, 'सूर ने जीवन को सरलता दी, तुलती ने आदर्श और प्रेमचंद ने यथार्थ अनुभूति। प्रेमचंद ने गीत नहीं गुनगुनाए, जनता की पीर जनता की भाषा में रोई है, जनता का आक्रोश, जनता के स्वरों में दिया है। जनजागरण की ज्योति, जनता की लौ में फूटी है।' प्रेमचंद के महत्व को रेखांकित करते हुए लेखक कहते हैं, भारतीय जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं रहा है जो प्रेमचंद की दृष्टि से ओझल हो।'
इस पुस्तक के सभी अध्याय अपने आपमें नए विचार को प्रेरित करने वाले हैं। मीरा और महादेवी वर्मा के साहित्य में नारी की क्या छवि है? लोक चिंतन की धारा, स्वतंत्र भारत में शिक्षा को उद्देश्य और कर्म की भागीरथी ऐसे ही महत्वपूर्ण निबंध हैं जो पाठक के मन में विचारपुंज पैदा कर देते हैं। निरंतर अनैतिक और मूल्यहीन होते जा रहे समय में देश-समाज-संस्कृति और साहित्य के प्रति एक सकारात्मक मोड़ देती यह पुस्तक पठनीय व संग्रहणीय है।
पुस्तक का नाम – साहित्य, समाज
और भारतीयता
लेखक – डा. ब्रह्मदत्त अवस्थी
प्रकाशक – नार्दन बुक सेंटर
4221/1 अंसारी रोड
दरियागंज, नई दिल्ली-2
मूल्य – 490 पृष्ठ – 145
दूरभाष – (011)-23264519
बेबसाइट : www.northernbook.com
आत्मानुभूति कराती नाट्यकृति
सुपरिचित नाट्यकर्मी और लेखक विमल लाठ प्राय: प्रेरक साहित्य रचने के लिए जाने जाते हैं। 'साकार होता सपना' जैसी उत्कृष्ट नाट्यकृति के बाद हाल में ही 'खुली किताब' शीर्षक से उनकी नई नाट्यकृति प्रकाशित हुई है। वास्तव में यह नाट्यकृति हर उस चैतन्य व्यक्ति की कहानी है जो अपने आस-पास फैल रही विषमताओं को लेकर चिंतित रहता है। उसे इस बात का तो ज्ञान रहता है कि इस दुनिया, समाज और अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है लेकिन आत्मबोध न होने के कारण या कह सकते हैं कि चेतना पर अज्ञानता की धुंध छाने के कारण वह स्वयं को अक्षम मान लेता है। उसे लगता है कि उसके करने से ये शुरू नहीं होगा। या फिर भाग्य को शायद मंजूर नहीं कि वह कोई बड़ा काम करे। या फिर कि एक अकेले उसके करने से क्या और कितना कुछ बदल सकता है? ऐसा ही एक व्यक्ति नाटक का मुख्य पात्र (जिसे इसमें संख्या 2 से प्रदर्शित किया गया है) अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर कैसे अग्रसर होता है, इसी कथानक को इस पुस्तक में रोचक ढंग से बताया गया है। नाटक का सूत्रधार/पथ प्रदर्शक (जिसे इसमें संख्या 1 से प्रदर्शित किया गया है) मुख्य पात्र के मन में मौजूद भ्रांतियों को कैसे दूर करना चाहता है और किस तरह वह मुख्य पात्र को जीवन की 'खुली किताब' का ज्ञान कराता है, यही इस कृति का मूल कथानक है।
वास्तव में यह जीवन का ही एक नाटक है, जिसमें इस बात का बोध होता है कि जीवन को कठिन या सरल बनाना, जीवन को अर्थवान या निरर्थक बनाना यह सब हमारे ही हाथों में है। अगर वास्तव में जीवन को सार्थक करने की चाह रखते हैं तो हमें अपनी आत्मदृष्टि को जाग्रत करना होगा। अपने चारों ओर स्पंदित होते जीवन को पहचान कर अपने कदम बढ़ाने होंगे। यही गहन जीवन दर्शन इसमें समझाया गया है।
पात्रों के बीच में संवाद की शैली सरल और भाषा भी बोधगम्य है। इससे गहन दर्शन को सरलता से समझा जा सकता है। जिस तरह अपने कर्म से विरत अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण ने आत्मप्रेरित किया था, कुछ इसी तरह मुख्य पात्र को नाटक का सूत्रधार प्रेरित करता है। उसकी उलझनों, उसकी दुविधाओं का दार्शनिक तर्कों पर समाधान कई स्थलों पर पाठक को प्रेरित करने वाला है। पात्र 2 के यह दुविधा जताने पर कि, 'हो सकता है जीवन के काम का बोध कराने वाली किताब व्यक्ति को जीवन भर मिले ही न!' सूत्रधार (पात्र 1) कहता है, 'यह नहीं हो सकता, जिसने जन्म लिया है, उसे पग-पग पर यह किताब मिलती रहती है। कभी वह चिल्ला-चिल्लाकर चेतावनी देती है। कभी बोलकर, समझाकर कुछ कहती है और कभी केवल चुप रहकर।'
सूत्रधार के तमाम तर्क और आत्मबोध कराने पर पात्र (2) को आभास होता है कि वास्तव में आत्मोत्थान के मार्ग पर, जनहित के मार्ग पर न चल पाने का कारण उसकी खुद की निष्क्रियता या अज्ञानता थी। वह आत्म-स्वीकृति करता है- 'यही चूक हो गई मुझसे। मैं सिर्फ अच्छा आदमा बना रहा। कभी योजक नहीं बना, संसार के दांव-पेच को भला-बुरा कहता रहा; उनसे दूर भागता रहा, अपने आपको सुलझा हुआ आदमी मानता रहा, लेकिन उन्हें दूर करने के लिए कभी कुछ किया नहीं, जबकि कुछ किया जा सकता था।'
आत्म जागरण का बोध कराती इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति और अस्मिता की भी विशेषताएं बताई गई हैं, 'भारतीय संस्कृति समग्रता में जीती है। पशु-पक्षी, वृक्ष-पर्वत नदी-सब लोक हैं, केवल मनुष्य ही नहीं। जीवन का हर दिन इसकी खोज है। इसकी खोज करनी है तो वह संपूर्णता में करनी होगी।' कह सकते हैं कि इस पुस्तक का अध्ययन हर उस चेतनशील व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने आस-पास के समाज-जीवन में बेहतर बदलाव का सपना देखता है।







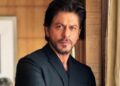






टिप्पणियाँ