25 जून 1975 भारत की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश में जो आपातकाल घोषित किया था, या कहें, आपातकाल थोपा था, जिसे स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला दिवस भी कहा गया है, उसकी 49वीं बरसी पर केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत प्रतिवर्ष 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।
सरकार का यह निर्णय बड़ा है, चुनौती पूर्ण है तथा राष्ट्रीय सन्दर्भ में अपेक्षित है,जिसने विपक्ष को और विशेषकर कांग्रेस पार्टी को असहज किया है। 2024 लोकसभा चुनाव अभियान में विपक्षी नेताओं ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर मुद्दा बनाया था कि भाजपा प्रचण्ड बहुमत इसलिये चाहती है, ताकि वह संविधान में अपने विचारों के अनुरूप परिवर्तन कर सके। यह भी कहा गया कि, सरकार संविधान को ही बदल देना चाहती है। चुनाव परिणामों में इस भ्रामक प्रचार का किञ्चित प्रभाव भी दिखाई दिया और एनडीए सरकार को उनकी उम्मीद से कम सीटें प्राप्त हुईं।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय की आपातकाल विषयक इस अधिसूचना पर निरन्तर बहस गर्म है। जो चर्चा, वार्ता मीडिया के माध्यम से, और विशेषकर दूरदर्शन के विविध चैनलों पर प्रसारित हुई है, उसमें देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पत्रकार, तथा विश्लेषक सम्मिलित रहे हैं। किन्तु जिन्होंने आपातकाल के उस कालखण्ड को देखा तथा भोगा, देशभर में रह रहे वे लोकतंत्र सेनानी इस चर्चा, डिबेट में सहभागी नहीं थे। इस औपचारिक चर्चा से आपातकाल का यथार्थ, तथा उसकी विभीषिका का अनुमान नहीं होता, उस काले अध्याय में व्याप्त सरकार तथा पुलिस द्वारा किये गये उत्पीड़न का आभास नहीं होता।
प्रश्न यह है कि कैसा था वह आपातकाल? यहां उसका सम्पूर्ण वर्णन सीमित शब्दों में सम्भव नहीं। उसकी लम्बी चौड़ी कथा व्यथा है, जो स्वयं में एक दुखान्त वृतान्त है। वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई वजह नहीं थी, कोई कारण नहीं था, जिससे आपातकाल घोषित करने की बाध्यता हो। देश में अराजकता का माहौल नहीं था, सीमाओं पर कोई व्यवधान नहीं था, आन्तरिक, बाह्य सुरक्षा को खतरे का कोई संकेत नही था। बिहार और गुजरात में छात्र, युवाओं के धरना प्रदर्शन थे, जिनमें सरकार की नीतियों के प्रति रोष था। वे संवैधानिक तरीके से अपने सुरक्षित भविष्य के लिये जायज मांग कर रहे थे। संयोगवश उस आन्दोलन को वयोवृद्ध समाजसेवी, लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण का प्रभावशाली नेतृत्व प्राप्त था, तथा उनके सहयोगी थे, कुशल संगठनकर्ता श्री नाना जी देशमुख।
इमरजेसी थोपने के पीछे श्रीमती इन्दिरा गांधी की हताशा तथा दुराग्रह निहित था, जो न्यायालय से मिली पराजय तथा अपकीर्ति की प्रतिक्रिया थी, झुंझलाहट थी। 25 जून के दिन देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई । न कोई चर्चा न कोई वार्ता,, न संसद की सहमति, किसी की संस्तुति या परामर्श की कोई आवश्यकता नही समझी गई। इन्दिरा गांधी प्रजातंत्रिक देश में तानाशाह हो गईं। मध्य रात्रि से ही जो धरपकड़ शुरू हुई, उसने सारे देश को जेलखाना बना दिया। नियम, कानून, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार,जनतन्त्र के ये सभी उपांग कुचल दिये गये, दरकिनार कर दिये गये। अनेक विरोधी दलों के नेता पकड़े गये। सरकार का एक और सनकीपन कहें तो पूरे देश के राजनैतिक बन्दियों का आरोपपत्र मानों एक ही जगह पर तैयार हुआ हो। इसमें चुनिन्दा तीन बातें,- इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद कह रहे थे, भीड़ को उकसा रहे थे, तथा सरकारी सम्पत्ति का नुकसान। विचित्र उदाहरण है, प्रख्यात साहित्यकार डा. रघुवंश की कोर्ट मे पेशी हुई, मजिस्ट्रेट ने देखा वे दोनों हाथों से दिव्यांग हैं और उनके आरोप पत्र पर हास्यास्पद आरोप अंकित था कि वे टेलीफोन के खम्बे पर चढ़कर तार काट रहे थे।
उस समय के राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारवादी संगठनों तथा उपलब्ध संचार माध्यमों ने दुनिया भर में इन्दिरा गांधी के इस तानाशाही रवैये की निन्दा की। प्रेस की स्वतंत्रता छिन गई, राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने विरोध स्वरूप सम्पादकीय कॉलम रिक्त छोड़ दिये, पूरे देश मे अकारण गिरफ्तारियों का क्रम निरन्तर चलता रहा। काग्रेस सरकार का मुख्य निशाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके अनुसांगिक संगठन, तथा संघ समर्थक व्यक्ति व संस्थायें थीं। संघ को प्रतिबन्धित संगठन घोषित कर दिया गया। देशभर के एक लाख से अधिक स्वयंसेवक जेलों में निरुद्ध थे। इन पर डीआई आर तथा नवसृजित कानून मीसा की धारायें आरोपित की गईं। अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी हुई पर वे संख्या में बहुत कम थे। संघ के लोग यद्यपि भूमिगत आन्दोलन के विशेषज्ञ नहीं थे किन्तु पूरे आपातकाल में जिस साहस व सातित्य से अनथक कार्य उन्होने किया, दुनिया उनकी योजना क्षमता की कायल है। विश्व के इतिहास में जो भी बड़े आन्दोलन हुए हैं, उनमें आपातकाल के खिलाफ यह आन्दोलन पूर्णतः अहिंसक था, यह उल्लेखनीय है।
संघ ने अपने कार्यकर्ताओं के आत्मानुशासन,समर्पण, साहस का उल्लेख संस्था द्वारा प्रकाशित साहित्य में, बैठकों तथा प्रशिक्षण वर्गों में गर्व के साथ किया है। आपातकाल के विरुद्ध इस संघर्ष व बलिदान को जनतंत्र की रक्षा के लिये की गई लड़ाई की संज्ञा दी है। वर्ष 201 में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के एक निर्णय में कहा गया कि आगे आने वाली पीढ़ियों यह संघर्ष व कार्यकर्ताओं का उत्सर्ग प्रेरणा देगा । आज केन्द्र सहित अनेक राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। उन्होंने आपातकाल के सेनानियों की चिन्ता का प्रयास प्रारम्भ तो किया है किंतु इस विषय पर समग्र विचार की आवश्यकता है। अर्धशताब्दी के इस बड़े अन्तराल मे अनेकों परलोक सिधार गये। सत्य यह है कि, आन्दोलनकारियों की सूची में सम्मिलित होकर उन्हें कभी भी किसी सरकारी सुविधा की चाह नहीं रही। इन कार्यकर्ताओं ने आपातकाल के अपने योगदान तथा कठिनाई की चर्चा तक नहीं की। उनकी मान्यता है कि देश पर आये आन्तरिक या बाह्य संकट में कटिबद्ध रहना हमारी पहली जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि, 1925 में संघ के स्थापना काल से आई अनेक विपत्तियों में, अनेक प्रतिबन्धो में अडिग रहने की एक शताब्दी से चली आ रही हमारी यह अखण्ड परम्परा है।
आपातकाल की त्रासदी की गाथा को आगे बढ़ायें तो, 18 से 20 वर्ष तक की आयु वर्ग के हजारों तरुण एक एक वर्ष तक कारागारों में बन्द रहे, सजा भी हुई पर माथे पर सिकन तक नहीं थी। अनेक की उपचार के अभाव में जेल मे ही मृत्यु हो गई और उनका पार्थिव शरीर ही जेल से बाहर आया, ऐसे भी उदाहरण हैं। मीसा कानून की तो परिभाषा ही प्रचलित हो गयी थी; नो वकील, नो दलील, नो अपील। ऐसा भी हुआ है कि व्यक्ति डी.आई.आर. से छूटकर बाहर आ रहा है और पुलिस जेल के द्वार पर मीसा का वारंट लिये खड़ी है, कानून का राज न होकर उत्पीड़न का साम्राज्य था।
देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन्दिरा गांधी की आंख की किरकिरी था। संघ के प्रति घृणा की दृष्टि जो उन्हें उनके पिता से विरासत की परम्परा से मिली थी,उससे आपातकाल की पहली चोट संघ पर लगा प्रतिबन्ध था। कार्यकर्ता जेलों में थे तथा अनेको भूमिगत। पू० सरसंघचालक श्री बालासाहब देवरस प्रारम्भ में ही गिरफ्तार हो गये। तथा संघ के तत्कालीन अखिल भारतीय अधिकारी प्रो० रज्जू भैया ने इस कठिन समय में भूमिगत रहकर धैर्यपूर्वक एक कुशल नायक की तरह मार्गदर्शन किया। उनकी परिवारिक प्रतिष्ठा, एक वैज्ञानिक, शिक्षाविद के नाते देशभर के प्रबुद्धजनों, राजनेताओं तथा प्रशासनिक वर्ग से उनका धनिष्ठ सम्बन्ध था । परिणामतः उनके नेतृत्व तथा पश्चात् पू० बालासाहब देवरस के कुशल मार्गदर्शन में आपातकाल के बाद खुली हवा में संघ के देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं के प्रयास से संघ विचार तथा संगठन का अप्रत्याशित विस्तार हुआ।
21 मार्च 1977 को आपातकाल हटने के बाद इस नीति पर विचार हुआ कि आपात्काल के इस सपूर्ण संघर्ष के वृतान्त को एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध किया जाये । वर्ष 1978 में मथुरा, उ०प्र० के वरिष्ठ प्राध्यापक तथा संघ के अनुभवी कार्यकर्ता प्रो० चन्द्रभानु गुप्त द्वारा लिखी पुस्तक, ‘तानाशाही को चुनौती’ में आपातकाल के संक्षिप्त किन्तु सटीक वृतान्त में आन्दोलन का वर्णन छपा है। यह पुस्तक मुख्य रूप से पश्चिमी उ० प्र ० पर केन्द्रित थी । कालान्तर में अनेक पत्र पात्रिकाओं में आपात्काल की संघर्षगाथा, इसकी त्रासदी, शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना, तथा समाज के द्वारा प्राप्त संरक्षण तथा अनन्य सहयोग के अनुभवों पर बहुत कुछ लिखा गया है, कहा गया है। आज इस सबका स्मरण आते ही । कल्पना होती है कि ब्रिटिश काल का क्रूर अध्याय भी ऐसा ही रहा होगा।
भारत सरकार के गृहमंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना में इस कृत्य लिए ‘संविधान की हत्या’ शब्द प्रयोग किया है, इसके पीछे संविधान की आत्मा के साथ हुई छेड़छाड़ के प्रति आक्रोश की अभिव्यक्ति है, जो विषय की गम्भीरता की ओर संकेत करती हैं। राजपत्र पर लिखा गया है कि आपात्काल के विरुद्ध संघर्ष करने वालों को श्रद्धाँजलि देना भी 25 जून के इस ‘काला दिवस’ का हेतु है। यह विचार ठीक ही है, किन्तु जो उस कालखण्ड के जेलयात्री आज मौजूद हैं, आयु के अन्तिम पड़ाव पर हैं, आज भी समाज सेवा के कार्यों में लगे हैं, उनकी कुशलक्षेम भी इस आयाम का प्रमुख हिस्सा होना चाहिये। देश के कई राज्यों में भाजपा-नीति की सरकारों ने इस विषय की चिन्ता की है, वे राज्य सरकारें आपातकाल के बन्दियों का हालचाल पूछती हैं। अब तो कुछ वर्षो से अनेक राज्य सरकारों ने ऐक्ट बनाये है, तथा इन्हें ‘लोकतंत्र सेनानी’ के रूप में मान्यता दी है।
अन्य राज्यों की तरह उत्तराखण्ड प्रदेश में भी राज्य सरकार के द्वारा एक्ट बने। 25 जून को आपातकाल की बरसी पर विमर्श के हेतु कोई आयोजन हो, इस कार्य के लिये एक छोटी सी समिति गठित हो जिसके माध्यम से जुड़कर लोकतंत्र सेनानी अपने अनुभवो के द्वारा इस अभियान में अपना योगदान कर सकें। आपातकाल की चर्चा, सिंहावलोकन, केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है, या देश को जनता तथा लोकतंत्र से जुड़ा सन्दर्भ है । अतः इस योजना में समाज की सहभागिता रहे,ऐसा प्रयास हो।
वर्ष 1975 का अकारण आपातकाल जनतंत्र पर एक कुठाराघात था, एक ही व्यक्ति, इंदिरा गांधी की तानाशाही जिद थी, जनता के मौलिक अधिकारों का हनन था, तथा यह एक नितान्त अविवेकपूर्ण निर्णय था। इस गलत निर्णय का सामना करने के लिये देश का जनमानस प्रत्यक्ष खड़ा रहा। सरकारी संवाद माध्यमों पर सेन्सरशिप थी, स्वतन्त्र प्रकाशनों पर सीलबन्दी भी हुई । कुछ साहसी पत्र पत्रिकाओं तथा यत्र तत्र प्रकाशित हो रहे भूमिगत न्यूज बुलेटिनों पर लेखकों की प्रतिक्रियायें तथा विरोध के स्वर खूब मुखर होते थे, जिन्हें उत्सुकता से देखा, पढ़ी जाता था । सामाजिक संस्थाओं की छोटी बड़ी गोष्ठियों में लोग मुखर होकर सरकार की जनविरोधी नीति की अलोचना करते थे। विरोध के इन स्वरों को कुचलने के लिये सरकार के पास एक ही हथियार था, देशद्रोह को धाराओं में धर पकड़ और फिर अमानुषिक व्यवहार ।
आपातकाल में सत्ता के द्वारा किये जा रहे अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस सरकार के प्रति आक्रोश की जो आग आम नागरिकों के मन मे सुलग रही थी उसका प्रगटीकरण 1977 के संसदीय चुनाव में हुआ। समूचे उत्तर भारत से कांग्रेस शून्य हो गयी और आपातकाल के गर्भ से प्रगट हुई जनता पार्टी को अप्रतिम सफलता मिली। इस विषय का एक उल्लेखनीय पक्ष यह भी है कि आन्दोलन में जनसंघ पक्ष की भूमिका राष्ट्रव्यापी थी, अर्थात् उसका संगठन देश के सभी राज्यों में था। जनसंघ के सर्वाधिक कार्यकर्ता सक्रिय थे, उनमें अधिकांश संघ कार्य से जुड़े थे । वे जेलों में रहे,तथा प्रताड़ित भी हुए। किन्तु नवोदित जनता पार्टी सरकार में उनकी चाहत केवल जनतंत्र की रक्षा की थी,सात्विक परिवर्तन की थी, सत्ता में त्यागपूर्ण सहभागिता की थी, सत्तालोलुपता की नहीं। इसीलिये श्रीमोरारजी देसाई के नेतृत्व को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, समर्थन दिया । इसीलिये संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में रहे भारतीय जनसंघ ने सरकार में कोई मांग नहीं की, कोई शर्त नहीं रखी। 1980 में ‘भारतीय जनता पार्टी’ गठन के मुम्बई महाधिवेशन में अटल जी ने भावुक होते हुए कहा था;- हमने तो अपने दल का नाम, उसका निशान, और पार्टी ध्वज सब कुछ त्याग दिया लेकिन दोहरी सदस्यता के नाम पर हमें अछूत माना गया, हमारा तिरष्कार भी हुआ । हम पवित्र मन से कहते हैं, जनता पार्टी को तोड़ने के महापाप में हम शामिल नहीं हैं । किन्तु आज जनआकाँक्षाओं तथा अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बूते हम पुनः खड़े हैं और हमारा संकल्प है कि हम सब ओर कमल खिलायेंगे, अपने सपनों का सशक्त भारत बनायेंगे।
आम चुनाव के रूप में 1977 का जनादेश स्पष्ट था कि स्वतन्त्र भारत ने जिस लोकतंत्र तथा संविधान को राज्यकार्य पद्धति के रूप में स्वीकार किया, उन पर आघात बर्दाश्त नहीं होगा । देश की वर्तमान तथा भावी पीढ़ी को इस ऐतिहासिक त्रुटि की जानकारी रहे ,जनतन्त्र में जन और तन्त्र दोनो पुष्ट हों, लोकतंत्र में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसीलिये इसका निरन्तर स्मरण रखना राष्ट्रीय सन्दर्भ में प्रत्येक भारतीय का नैतिक दायित्व है। भारत सरकार की इस अधिसूचना का मन्तव्य भी यही है, जो औचित्यपूर्ण है।
(लेखक आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं)




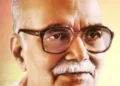













टिप्पणियाँ