योग का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। इसका उल्लेख रामायण और महाभारत के कालखंड से लेकर भगवान शिवजी, भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों में मिलता है। ऋग्वेद में ऋषियों द्वारा ध्यान, तप और आत्मा की खोज का उल्लेख मिलता है, जो योग की प्रारंभिक चेतना को दर्शाता है। उपनिषदों में यह चेतना और विकसित होकर ‘प्रणव साधना’, ‘ध्यान योग’ और ‘ब्रह्मविद्या’ के रूप में दर्शन की परिपक्व अवस्था में पहुँचती है।
योग को विधिपूर्वक और व्यवस्थित रूप में महर्षि पतंजलि ने प्रस्तुत किया। उनके द्वारा रचित ‘योगसूत्र’ में योग को केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन के समग्र दर्शन के रूप में प्रतिपादित किया गया। योग का व्यावहारिक पक्ष हठयोग के माध्यम से अधिक विस्तारित हुआ, जिसका वर्णन घेरण्ड संहिता, हठयोग प्रदीपिका और शिव संहिता जैसे ग्रंथों में मिलता है। मध्यकाल में योग का प्रसार संत परंपरा के माध्यम से हुआ – जैसे गुरु गोरखनाथ, गोस्वामी तुलसीदास आदि।
आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, श्री अरविंद, महर्षि महेश योगी आदि योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख साधक और विचारक बने। आज योग भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का जीवंत प्रतीक बन चुका है। वह केवल स्वास्थ्य या व्यायाम की पद्धति नहीं, बल्कि आत्मविकास, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक मार्ग है।
योग- भारतीय वेदों और दर्शनों और सम्प्रदायों में
- भूतं भव्यं भविष्यं च सर्व वेदात् प्रसिध्यति’ (मनु १२।९७) के अनुसार योग का मूल वेदों में निहित है।
- ऋग्वेद में योग का उल्लेख अत्यंत प्राचीन और गूढ़ रूप में हुआ है। कल्याण – योगतत्त्व अंक में उद्धृत मंत्र, ‘यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन। स धीनां योगमिन्वति॥‘ (ऋग्वेद 1.18.7) — में ‘योग’ का तात्पर्य बुद्धि, चित्त और कर्म को ईश्वर में समर्पित करने से है। वैदिक ऋषियों ने योग को केवल शारीरिक साधना नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच की गहन चेतनात्मक एकता के रूप में परिभाषित किया। इस ग्रंथ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऋग्वेद की अनेक ऋचाएँ — जैसे 10.177.3, 10.13.1 आदि — योग की ओर संकेत करती हैं। योग का मूल अर्थ ‘जोड़ना’ या ‘एकाग्रता’ रहा है, और वैदिक यज्ञों, ध्यान और आत्मबोध की साधनाओं के केंद्र में यही भाव रहा है। अतः ऋग्वेद योग का आदि स्रोत और उसका आध्यात्मिक आधारभूत स्तंभ माना जाता है।
- यजुर्वेद के मंत्रों में हमें कहीं दो, कहीं तीन, कहीं चार और एक दो स्थलों पर पांचों प्राणों का भी युग्म रूप से उल्लेख मिलता है। प्राणों के यजुर्वेद संहिता में प्राण, अपान, व्यान और उदान का उल्लेख है जबकि समान नामक प्राण को यत्र-तत्र ही स्मरण किया गया है।
- यजुर्वेद की एक ऋचा इन प्राणों को ऋषि कह कर संबोधित करती है। शरीर में विद्यमान प्राण रूप यह ऋषि ही मन-मस्तिष्क को ऋषि रूप में विकसित और प्रतिष्ठापित करते हैं। ऋषि अर्थात् अंतर्निहित तथ्यों और रहस्यों को यथावत जानने समझने की दृष्टि विशेष। तार्किक और बौद्धिक उत्कर्ष की चरमावस्था है यह ऋषित्व। ऋषित्व के अभाव में शास्त्रोक्त तथ्यों और विष्ट गानों का सम्यक परिज्ञान असंभव प्रायः ही है। योगचर्या के अभाव में ऋषित्व की प्राप्ति असंभाव्य है। अतः स्पष्ट ही है कि योगजन्य प्रज्ञाविवेक से ही वेद मंत्रं में अंतर्भूत तत्वों को जाना जा सकता है।
- अथर्ववेद (19.8.2) में हम बीजरूप में ‘योग’ शब्द विद्यमान पाते हैं। ‘योग’ प्रक्रिया के सबसे अहं सोपान प्राण-विद्या का हम वैदिक ऋचाओं में महती विस्तार देखते हैं।
- अथर्ववेद के 11वें कांड का चौथा सूक्त प्राणविद्या का अनुपम विवरण प्रस्तुत करता है। इस सूक्त में व्यष्टि से समष्टि तक प्राण के विभिन्न आधारों एवं क्रियाकलापों को स्मरण कर नमन किया गया है। सूक्त का प्रथम मंत्र ही प्राण की व्यापकता को रेखांकित करते हुए कहता है कि उस प्राण के प्रति सबका नमन, जिसके वश में यह सब कुछ है। जो समस्त प्राणियों का ईश्वर है, और जिसमें यह सब प्रतिष्ठित है।
- कठोपनिषद् में कहा गया है : ‘यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्। अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ॥‘ (कठोपनिषद् २।३।१०-११)। इससे स्पष्ट है कि योग केवल आसन न होकर आंतरिक स्थिरता और आत्मसाक्षात्कार की चरम अवस्था है।
- वैदिक संहिताओं में प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान-प्राणों का हमें अधिकांशतः उल्लेख मिलता है। यद्यपि प्राण एक ही है परंतु कार्य वैभिन्य एवं स्थान, स्थिति और चेष्टा भेद से इनके अनेक नाम रख लिए गए हैं।
- वैशेषिक-दर्शन में आत्मस्वरूप में स्थित निष्क्रिय और नि्दुःख-मनःस्थिति योग है। प्रकारान्तर से चित्तनिरोध योग है।
- न्यायशास्त्र में योगदर्शन के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशरूप पञ्चविध श्लोकों का राग, द्वेष और मोह के रूप में वर्णन किया गया है। आत्मसाक्षात्कार से इनकी निवृत्ति होती है। इस प्रकार न्यायशास्त्र में योग का अत्यन्त महत्त्व है।
- नाथ संप्रदाय की योग साधना को शिवविद्या या महायोगविद्या कहा गया है। इस परंपरा की मूल अवधारणा अलख निरंजन तत्व के स्वसंवेदन और पिंड-ब्रह्मांड के सामरस्य के अंतर्बाह्य साक्षात्कार पर आधारित है। इसके प्रवर्तक भगवान योगिराज शिव माने जाते हैं, जिन्होंने आदिशक्ति पार्वती को उपदेश दिया : ‘शिवविद्या महाविद्या गुप्ता चाग्रे महेश्वरी’ (शिवसंहिता।
- नाथ पंथ में परम उपास्य अद्वैत से परे परमेश्वर, परमशिव को माना गया है जो निराकार, निर्मल और ज्योति रूप हैं। गोरक्षनाथ को इस संप्रदाय का सर्वप्रसिद्ध सिद्ध माना गया, जिन्हें उनके गुरु मत्स्येन्द्रनाथ से दीक्षा प्राप्त हुई थी। गोरक्षनाथ ने न केवल गुरु के बताए मार्ग का पालन किया, अपितु स्वानुभव से साधना में और अधिक प्रगति की। उन्होंने गोरक्षशतक, गोरक्षसंहिता, गोरक्षगीता, गोरक्षकल्प, गोरक्षपिष्टिका और विवेकमार्तण्ड जैसे संस्कृत ग्रंथों की रचना की।
- नाथ परंपरा के दो भेद हठयोग में माने गए हैं : (1) मार्कण्डेय हठयोग, (2) नाथपंथी हठयोग। हठयोग के प्रमुख अंगों में प्राणायाम को मूल आधार माना गया है “हठिनामधिकस्त्वेक: प्राणायामपरिश्रमः।“ (प्राणायाम में मन की स्थिरता- यही योगसिद्धि का मुख्य साधन है)।





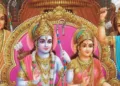












टिप्पणियाँ