पाश्चात्य नारी विमर्श ‘स्त्री बनाम पुरुष’ के समीकरण को व्यक्त करता है। परिणामस्वरूप वह नारीत्व को समुचित रूप से आमंत्रित करने की स्थिति में नहीं है। इस संदर्भ में भारतीय स्त्री विमर्श के भाष्य की आवश्यकता है और उसकी सम्पूर्ति में यह पुस्तक ‘शक्ति : वीमेन जेंडर एंड सोसाइटी इन इंडिया : पर्सपेक्टिव्स ऑन फेमिनिज्म’ एक समयानुकूल और बहु-प्रतीक्षित प्रयास है। भूमिका में डॉ. महेश चंद्र शर्मा लिखते हैं, ”यह परिवार का विस्तार ही है जो मानव जाति को स्वयं को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, एक वास्तविकता जिसे भारत ने ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ कहा है। मध्यकालीन युग की बर्बरता ने महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए कवच के पिंजरे में बंद कर दिया था। आधी सहस्राब्दी तक महिलाओं को संरक्षित किया जाना था। परिणामस्वरूप महिलाएं अशिक्षा में फंस गईं। ‘परिवार’ भारतीय समाज की महत्वपूर्ण संस्था है और इसका उचित और पर्याप्त समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाना चाहिए।”
एक गहन विश्लेषण प्रदान करते हुए 26 लेखकों द्वारा इस संदर्भ को अधिक सार-गर्भित और समग्र बनाने का प्रयास नैना सहस्रबुद्धे ने इस पुस्तक के मुख्य संपादक की भूमिका के माध्यम से निष्पादित किया है।
यह पुस्तक भारत में नारीवादी विमर्श पर उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करती है। यह नारीवाद पर समकालीन दृष्टिकोण में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और स्त्री विमर्श आधारित अवधारणाओं पर पुनर्विचार और पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर पर प्रकाश डालती है। यह नारीवादी सिद्धांत को उपनिवेशवाद से मुक्त करने और भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसी प्रमुख अवधारणाओं की पुनर्व्याख्या पर बल देती है। इस प्रकार यह स्त्री विमर्श पर एक वैकल्पिक ढांचा प्रस्तुत करती है जो आयातित पश्चिमी संरचनाओं के बजाय स्वदेशी दर्शन के महत्व पर प्रकाश डालता है।
इस पुस्तक में चार खंडों के अंतर्गत स्त्री विमर्श को कई आयामों से विश्लेषित करने और उसे समझने का प्रयास किया गया है। पुस्तक का प्रथम खंड स्त्री विमर्श को भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में इसको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से विश्लेषित करने का सार्थक प्रयास है। इसमें स्त्री-पुरुष के मध्य भेदात्मक दृष्टि रखने से और उसे पोषित करने की पाश्चात्य परंपरा की प्रतिक्रिया स्वरूप संसार में स्त्री विमर्श के अंतर्गत अनेक एवं समानांतर विमर्श उठ खड़े हुए, जिनमें अश्वेत, समाजवादी, अतिवादी एवं दलित नारीवादी विमर्श मुख्य हैं। अधिसंरचना, सामाजिक संरचना एवं क्रिया—कलापों के द्वारा यदि पुरुष स्त्री के ऊपर आधिपत्य रखने का प्रयास करता है तो उसे पितृ-सत्तात्मक व्यवस्था कहते हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह मात्र पुरुषों के लिए कार्य करता है या उन्हें भी इस व्यवस्था से हानि होती है? इन प्रश्नो के उत्तर भी खोजे गए हैं।
पुस्तक के द्वितीय खंड में स्त्री-विमर्श को बहु-आयामी दृष्टिकोण से देखा गया है। पुस्तक के तीसरे खंड का नाम ‘सामाजिक जीवन में महिलाओं के पदचिन्ह’ है, जिसके अंतर्गत प्रफुल्ल केतकर, ओमकार जोशी, माधवी नरसाले, मनीषा कोठेकर, सिंधु कपूर, जया फूकन और अभिराम भद्कामकर ने अपने-अपने लेखों के माध्यम से इस आयाम को स्पर्श करने का सार्थक प्रयास किया है। पुस्तक का चौथा और अंतिम खंड नारीवादी विमर्श के समकालीन मुद्दों पर प्रकाश डालता है। इस खंड में विविध शोध लेखों के माध्यम से स्त्रियों के सामाजिक जीवन, अर्थव्यवस्था और शासन में उनके योगदान जैसे विषयों को शामिल किया गया है।
इसमें चर्चा की गई है कि कैसे एक महिला अपनी आकांक्षाओं और व्यावसायिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बैठाते हुए समकालीन मुद्दों से निबटती है। इस खंड में यह भी चर्चा की गई है कि पड़ोसी देशों में प्रणय निवेदन, विवाह और माता-पिता बनने के तरीके कैसे बदल रहे हैं। अंत में यह एक सर्वविदित सत्य है कि मानवतावाद अपनी सर्वोच्च अभिव्यक्ति केवल सामाजिक संबंधों में पाता है, अराजकता में नहीं। पुरुष और महिला के बीच का संबंध सामाजिक और मानवीय रिश्तों के संदर्भ में पूर्णता प्राप्त करता है। इस संदर्भ में भारतीय स्त्री विमर्श का यह अध्ययन ‘भारतीय स्त्री शक्ति’ की प्रेरणा से इसके प्रधान संपादक द्वारा द्वारा करना एक सराहनीय प्रयास है।

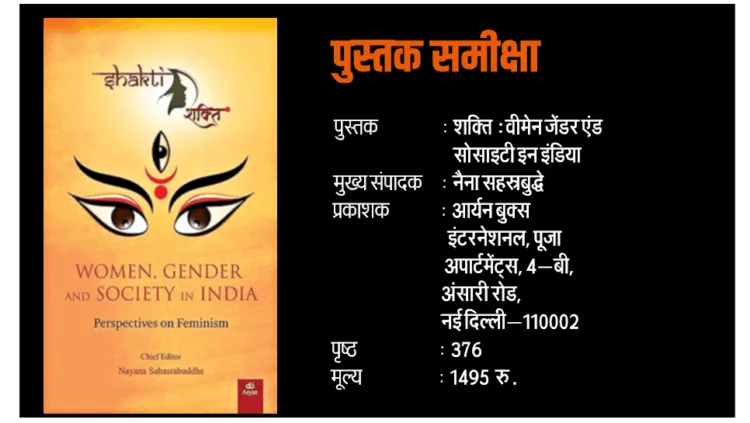















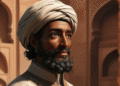
टिप्पणियाँ