बौद्ध मत के संस्थापक गौतम क्षत्रिय थे और शाक्य वंश से थे। अब उनका भूभाग नेपाल की तराई के उस हिस्से द्वारा दर्शाया जाता है जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के ठीक उत्तर में स्थित है।
बाद की प्रसिद्ध किंवदंतियों में उन्हें एक शक्तिशाली राजा के पुत्र के रूप में दर्शाया गया है, जो एक स्थान के सुख-सुविधाओं के बीच पैदा हुआ और पला-बढ़ा था। हालाँकि, तथ्य यह है कि शाक्य का संविधान गणतांत्रिक था और गौतम के पिता को संभवतः कुछ समय के लिए राज्य के प्रमुख पद पर चुना गया था। उनकी जन्मतिथि विवाद का विषय है, लेकिन हम तर्कसंगत रूप से इसे 566 ईसा पूर्व मान सकते हैं। जैसे-जैसे वह वयस्क हुए, वह उस समय की प्रचलित भावना से प्रभावित हुए, जो एक प्रकार का निराशावाद था जो आध्यात्मिक आकांक्षाओं की ओर ले जाता था।
लोकप्रिय परम्परा में नाटकीय ढंग से दर्शाया गया है कि किस प्रकार गौतम एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति और एक शव को देखकर भयभीत हो गए थे, और फिर एक तपस्वी के संत स्वरूप से आकर्षित होकर, उन्होंने अचानक ही त्याग की भावना में अपना घर, पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया था। तथ्य यह प्रतीत होता है कि संसार की बुराइयों से छुटकारा पाने की समस्या, जिनमें बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सबसे प्रमुख हैं, युवाओं के बेहतर दिमागों को आंदोलित कर रही थी, जिन्हें यह एहसास हो गया था कि उनके चारों ओर मौजूद भौतिक विलासिता व्यर्थ है।
गौतम ने उस समय की बढ़ती निराशा को स्वीकार किया और उच्चतर सत्य की खोज में अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने कुछ समय तक राजगृह के दो प्रसिद्ध शिक्षकों के दार्शनिक विद्यालयों में अध्ययन किया और फिर गया के पास उरुविल्वा चले गए। छह वर्षों की एकाग्रता और गहन ध्यान के परिणामस्वरूप उन्हें ऐसे सत्यों की खोज हुई, जिनके बारे में उनका दावा था कि वे संसार की बीमारियों को दूर कर देंगे, और इस प्रकार गौतम बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए।
मौलिक सिद्धांत
बुद्ध की शिक्षाओं के मूल सिद्धांत चार आर्य सत्य (आर्य-सत्यनि) द्वारा दर्शाए गए हैं-
- यह संसार दुःखों से भरा हुआ है।
- प्यास, इच्छा, आसक्ति आदि सांसारिक अस्तित्व के कारण हैं।
- जिसे प्यास आदि के नाश से रोका जा सके।
- ऐसा करने के लिए, व्यक्ति को सही तरीका पता होना चाहिए।
दुःखों के कारणों की श्रृंखला का विस्तार से वर्णन किया गया है, तथा इन दुःखों से मुक्ति के साधनों को भी विस्तार से समझाया गया है। यह प्रसिद्ध अष्टांगिक मार्ग है, अर्थात सही भाषण, सही कर्म और आजीविका के उपयुक्त साधन, उचित परिश्रम, सही जागरूकता, सही ध्यान और उपयुक्त संकल्प और सही दृष्टिकोण। जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, जो शांति और आनंद की शाश्वत अवस्था है, जो दुःख और इच्छा, क्षय या बीमारी से मुक्त है, और निश्चित रूप से, आगे जन्म और मृत्यु से भी मुक्त है।
बुद्ध द्वारा प्रचारित नैतिक सिद्धांत काफी सरल थे: मनुष्य अपने भाग्य का निर्णायक है, कोई ईश्वर या देवता नहीं। यदि वह इस जीवन में अच्छे कर्म करता है, तो उसे उच्चतर योनि में पुनर्जन्म मिलेगा, जब तक कि वह मोक्ष या जन्म की बुराइयों से अंतिम मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। दूसरी ओर, बुरे कर्मों का दण्ड अवश्य मिलेगा, और इससे न केवल मोक्ष में बाधा होगी, बल्कि मनुष्य निम्न से निम्नतर योनियों में पुनर्जन्म लेगा। मनुष्य को दोनों अतियों से बचना चाहिए, अर्थात् विलासितापूर्ण जीवन और कठोर तप – सामान्य नैतिक संहिता, जैसे सत्य, दान, पवित्रता और वासनाओं पर नियंत्रण के अतिरिक्त मध्यम मार्ग सर्वोत्तम है। बौद्ध धर्म प्रेम, करुणा, समता और विचार, शब्द या कर्म के माध्यम से जीवित प्राणियों को क्षति न पहुँचाने पर जोर देता है।
यात्रा और शिक्षाएँ
गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की उम्र में एक धार्मिक शिक्षक का जीवन अपनाया और मगध, कोसल और आसपास के प्रदेशों में विभिन्न स्थानों पर घूमकर अपने धर्म का प्रचार किया। इस प्रकार उन्होंने जिन शिष्यों की भर्ती की, वे दो श्रेणियों में आते थे: उपासक या सामान्य शिष्य, जो परिवार के साथ रहते थे, और भिक्षु या भिक्षु, जो संसार को त्याग कर तपस्वी का जीवन व्यतीत करते थे। बुद्ध में महान संगठन क्षमता थी और उनके द्वारा स्थापित बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय, जिसे संघ कहा जाता था, विश्व में अब तक देखे गए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक संगठनों में से एक बन गया।
यहां बौद्ध मत की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं देखी जा सकती हैं। उनमें से एक था उनके मंदिर में महिला सदस्यों को भिक्षुणी और भिक्षुणी के रूप में प्रवेश देना। बुद्ध ने शुरू में इसका विरोध किया, लेकिन अंततः उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उन्हें अपने मंदिर के भविष्य के बारे में सहमति देने के लिए राजी कर लिया (हालांकि इसमें बहुत अधिक आशंकाएं थीं)। दूसरे, मंदिर में सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त थे, चाहे वे किसी भी वर्ग या जाति से संबंधित हों। तीसरा, बुद्ध ने सामान्य लोगों की भाषा में धार्मिक प्रवचन देने की प्रथा शुरू की, न कि अत्यधिक जटिल संस्कृत भाषा में, जो आम लोगों के लिए समझ से बाहर थी।
इन सभी कारकों ने बुद्ध के धर्म को अत्यधिक लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया। जब अस्सी वर्ष की आयु में (486 ई.पू.) कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई, तो भिक्षुओं और शिष्यों के एक बड़े समूह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।
गौतम बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद, उनके शिष्यों की राजगृह में एक सामान्य परिषद् हुई। उन्होंने गुरु की शिक्षाओं का यथासंभव पूर्ण एवं प्रामाणिक संग्रह बनाया। यह और भी महत्वपूर्ण था क्योंकि बुद्ध ने मंदिर के प्रमुख के रूप में अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने शिष्यों से स्पष्ट रूप से कहा था: “मैंने जो सत्य और संघ के नियम तुम्हारे लिए निर्धारित किए हैं, मेरे जाने के बाद वे ही तुम्हारे शिक्षक बनें।”
बौद्धों का पवित्र साहित्य, जिसने संभवतः एक या दो शताब्दी बाद अपना अंतिम रूप लिया, त्रिपिटक या तीन टोकरियाँ के नाम से जाना जाता है। पहला है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के मार्गदर्शन और मंदिर के सामान्य प्रबंधन के लिए नियम और विनियम निर्धारित किए गए थे। दूसरा, सुत्त-(सूत्र) पिटक, बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संग्रह था; तीसरे, अभिधिअम्म-पिटक में धर्म के अंतर्निहित दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई थी।
बुद्ध और त्रिपिटक में निहित उनके सिद्धांतों के अलावा एक तीसरा कारक भी था जो समान रूप से महत्वपूर्ण था। यह संघ या बौद्ध मंदिर था। आज भी, लाखों बौद्ध प्रतिदिन पवित्र त्रिदेवों में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए यह पवित्र सूत्र बोलते हैं, “मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, मैं संघ की शरण लेता हूँ।”
मंदिर, या किसी विशेष धार्मिक विश्वास का पालन करने वाले पुरुषों के एक कॉर्पोरेट निकाय का विचार परिचित था, और गौतम बुद्ध के समय में और उससे पहले इस प्रकार के कई संगठन थे। हालाँकि, उनका श्रेय इन संगठनों को दिए गए संपूर्ण और व्यवस्थित चरित्र में निहित है।
बौद्ध मंदिर की सदस्यता सभी व्यक्तियों के लिए खुली थी, चाहे वे पुरुष हों या महिला, पंद्रह वर्ष से अधिक आयु के हों, चाहे उनमें किसी भी वर्ग या जाति का भेद हो, सिवाय कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों के, जैसे कुष्ठ रोग और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोग, अपराधी, दास आदि।
नये धर्मान्तरित व्यक्ति को एक गुरु चुनना होता था जो उसे भिक्षुओं की सभा के समक्ष ले जाता था और औपचारिक रूप से उसे मंदिर में प्रवेश देने का प्रस्ताव रखता था। सहमति प्राप्त होने के बाद, धर्मांतरित व्यक्ति को औपचारिक रूप से धर्मगुरु बना दिया गया, तथा उसे गरीबी और कठोर नैतिकता वाला जीवन जीने की पूरी जानकारी दी गई।
नये विचारों और आदतों को अपनाने के लिए उसे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता थी और पहले दस वर्षों तक उसे अपने गुरु पर पूर्ण निर्भरता में रहना पड़ा। इस अनुशासनात्मक अवधि के बाद, वह उत्कृष्ट धार्मिक निगम का अभिन्न अंग बन गए। इसके बाद, उनके आचरण को, सूक्ष्मतम विवरण तक, विशिष्ट अध्यादेशों द्वारा विनियमित किया गया; यहां तक कि थोड़ा सा भी उल्लंघन करने पर उसे निश्चित रूप से उचित दंड दिया जाएगा। बौद्ध चर्च का प्रमुख सिद्धांत यह था कि संप्रदाय का कोई भी संस्थापक बिरादरी के लिए कानून नहीं बना सकता था। अन्य लोग उन्हें समझा सकते थे और व्याख्या कर सकते थे, लेकिन नये कानून बनाने के लिए उन्हें सहायता की आवश्यकता होती थी।
बौद्ध मंदिरों की संरचना
बौद्ध मंदिर विभिन्न स्थानीय संघों या भिक्षुओं के समुदायों से मिलकर बने होते थे। कोई भी केंद्रीय संगठन विभिन्न स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय स्थापित नहीं कर रहा था, और जब भी कोई अवसर आता था, सामान्य परिषदों की बैठक आयोजित करके इस दोष को दूर करने का प्रयास किया जाता था। सिद्धांततः, ये सभी स्थानीय निकाय एक सार्वभौमिक मंदिर के भाग मात्र थे। इस प्रकार, कोई भी स्थानीय निकाय सदस्य स्वतः ही किसी भी अन्य क्षेत्रीय समुदाय का सदस्य हो जाता था, जहां वह जाता था। ये स्थानीय निकाय सख्ती से लोकतांत्रिक सिद्धांतों द्वारा शासित थे; किसी इलाके में रहने वाले सभी भिक्षुओं की आम सभा सर्वोच्च प्राधिकारी होती थी, तथा मतों से मामलों का निर्णय होता था।
प्रत्येक सभा की बैठक वैध थी यदि सभी सदस्य उपस्थित होते या अनुपस्थित रहते हुए औपचारिक रूप से अपनी सहमति व्यक्त करते। सभा, जिसके संविधान और कार्यप्रणाली से वर्तमान समय के अति-लोकतंत्रवादी भी संतुष्ट हो जाते थे, को व्यक्तिगत भिक्षुओं पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था तथा उनके अपराधों के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की सजा दी जा सकती थी। वे अपने द्वारा नियुक्त अनेक अधिकारियों के माध्यम से मठ के आवश्यक धर्मनिरपेक्ष कार्यों को संचालित करते थे।
भिक्षुणियाँ एक अलग समुदाय का गठन करती थीं जो व्यावहारिक रूप से भिक्षुओं के समुदाय के अधीन थी। बौद्ध धर्म के कानून की सामान्य प्रवृत्ति भिक्षुणियों को स्पष्ट रूप से निम्न दर्जा देने की थी, क्योंकि महान बुद्ध का मत था कि बौद्ध चर्च में उनका प्रवेश उसकी पवित्रता को नष्ट करने के लिए किया गया था। इस बुराई को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय तैयार किए गए थे, लेकिन भिक्षुओं के संघ को दिशा देने वाले आवश्यक सिद्धांत भिक्षुणियों की सुविधा के लिए भी समान रूप से लागू थे।
बौद्ध संघ की दो आवश्यक प्रथाओं का विशेष उल्लेख किया जा सकता है; पहला, प्रत्येक पखवाड़े के आठवें, चौदहवें और पंद्रहवें दिन स्थानीय भिक्षुओं की धर्म-पाठ के लिए नियमित सभा थी। अंतिम दो दिनों में से एक दिन, एक विद्वान भिक्षु ने ‘पतिमोक्खा’ नामक एक लघु ग्रंथ का पाठ किया, जिसमें उन अपराधों और अपराधों की सूची दी गई थी, जिनसे बौद्ध भिक्षुओं को बचना चाहिए। जैसे-जैसे पाठ आगे बढ़ता गया, और प्रत्येक प्रकार के अपराधों के वर्णन के अंत में, एकत्रित भिक्षुओं और भिक्षुणियों से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या वे इसके बारे में शुद्ध थे। इनमें से किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को अपना अपराध स्वीकार करना पड़ता था, तथा उसके मामले को नियमों और विनियमों के अनुसार निपटाया जाता था।
एक अन्य विशिष्ट संस्था है वासिया, या रिट्रीट, जो वर्षा ऋतु के दौरान आयोजित होती है। यह आदेश दिया गया था कि प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु के दौरान तीन महीने तक भिक्षुओं को एक स्थायी निवास में रहना चाहिए तथा आपातकालीन स्थिति को छोड़कर उसे छोड़ना नहीं चाहिए। शेष वर्ष में भिक्षु पूरे देश में घूमते रहते थे।
ऊपर चित्रित मंदिर के संगठन को विकसित होने में सदियाँ लगी होंगी, लेकिन इसकी आधारशिला स्वयं बुद्ध ने रखी थी। इसका मुख्य दोष किसी समन्वयकारी केन्द्रीय प्राधिकरण का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप चर्च के भीतर बार-बार मतभेद उत्पन्न होते रहे। बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद, वैशाली के भिक्षुओं ने कुछ ऐसी प्रथाओं का पालन किया जिन्हें कुछ भिक्षुओं ने गैरकानूनी माना। बौद्धों की एक आम परिषद आयोजित की गई, और उत्तरी भारत के विभिन्न भागों से भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया। इस परिषद के विवरण को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन इसके बाद एक बड़ा मतभेद उत्पन्न हो गया और एक नया संप्रदाय स्थापित हो गया।

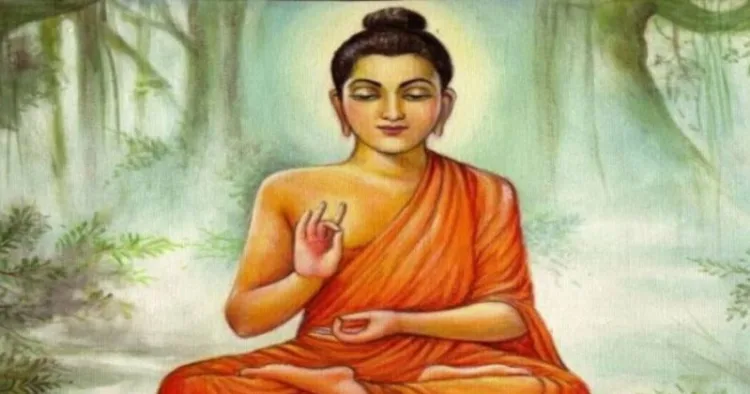















टिप्पणियाँ