वर्तमान की विषम वैश्विक परिस्थितियों में तथागत का पंचशील दर्शन अपने समय से कई गुना अधिक प्रासंगिक है। तनाव, विग्रह, क्रूरता व हिंसा से भरे वर्तमान समाज में महात्मा बुद्ध की सरल, व्यवहारिक और मन को छू लेने वाली शिक्षाएं व्यक्ति को समाधान की ओर ले जाती हैं। यही वजह है कि गौतम बुद्ध शताब्दियों से समूचे विश्व में एक ऐसी आध्यात्मिक विभूति के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने पीड़ित मानव समाज के उद्धार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।
सामान्यतया बाहरी तौर से देखने पर भगवान बुद्ध का चरित्र एक व्यक्ति विशेष की उपलब्धि मानी जा सकती है किन्तु तात्विक दृष्टि से इसे एक क्रांति कहना अधिक समीचीन होगा। महात्मा बुद्ध विश्व के साकार विवेक हैं। उनका जीवन दर्शन और उनके नैतिक उपदेश विज्ञान के प्रेमी आधुनिक विचारकों को भी बहुत सुहाते हैं क्योंकि उनका दृष्टिकोण तर्कपूर्ण और अनुभवपरक है।
वर्जनाओं का दर्शन
बुद्ध का दर्शन वस्तुतः वर्जनाओं का दर्शन है। बुद्ध का मूल प्रतिपादन सार रूप में तीन सूत्रों में है – बुद्धं शरणं गच्छामि ! संघं शरणं गच्छामि ! धम्मं शरणं गच्छामि। अर्थात हम बुद्धि व विवेक की शरण में जाते हैं। हम संघबद्ध होकर एकजुट रहने का व्रत लेते हैं। हम धर्म की नीति निष्ठा का वरण करते हैं। ये तीन सूत्र जो बौद्ध धर्म के आधार माने जाते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने समय में समाज में व्याप्त कुरीतियों व विसंगतियों का निदान करते हुए कहा कि यदि बुद्धि को शुद्ध न किया गया तो परिणाम भयावह होंगे। इस बुद्धि शुद्धि की प्रक्रिया के लिए वे मनुष्य को पांच पापों से दूर रहने को कहते हैं। ये पांच पाप हैं-हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ और मादक द्रव्यों व मांसाहार का सेवन। मनुष्य के आचरण को नैतिक बनाने के लिए बुद्ध ने पंचशीलों के अनुशीलन पर बल दिया। त्रिपिटक ग्रंथों में इन पंचशीलों की विस्तृत व्याख्या मिलती है। इन पंचशीलों के द्वारा महात्मा बुद्ध ने समूची दुनिया को मर्यादित जीवन जीने की सीख दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ उतना संजोकर रखो जितनी कि तुम्हें जरूरत है।
तृष्णा का नकार और जीवमात्र से प्यार। बुद्ध कहते हैं कि झूठ भी हिंसा है क्योंकि वह सत्य का दमन करती है। वे मनुष्य को सिर्फ अपने श्रम पर भरोसा रखने की बात करते हुए कहते हैं कि उसी वस्तु को अपना समझो जिसको तुमने न्यायपूर्ण ढंग से अर्जित किया है। जिस तरह आज हमारे समाज में व्यभिचार, बलात्कार व अप्राकृतिक यौन संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं, आत्मीय संबंधों का भी आदर नहीं हो रहा, समाज में हिंसा, भय व अशांति बढ़ रही है। सख्त कानून के बावजूद दहेज हत्या और भ्रूणहत्या की घटनाएं रुक नहीं रहीं हैं। मानव जीवन में तनाव और अवसाद तेजी से गहरा रहा है। समाज के इस नैतिक व चारित्रिक पतन को इन पंचशीलों के पालन से ही रोका जा सकता है और मनुष्य के अंतस में प्रज्ञा, शील, मैत्री व करुणा जैसे जीवन मूल्य विकसित किये जा सकते हैं।
मद्यनिषेध के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाले प्रथम व्यक्ति
ज्ञात हो कि स्वामी विवेकानन्द ने महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा था, ‘’ बुद्ध वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मद्यनिषेध के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। आज जिस तरह हमारे समाज में शराब व नशीले पदार्थों के सेवन का प्रचलन तेजी से बढ़ता रहा है; पंचशील के पालन से ही इस दुर्व्यसन से छुटकारा पाया जा सकता है। पुरानी कहावत है- धन खो गया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खो गया तो कुछ खो गया, जब चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। अत: चरित्र निर्माण के लिए पंचशील का पालन आवश्यक है।
“अप्प दीपो भव’’ के प्रतिपादक
तथागत गौतम न स्वयं कहीं बंधे और न ही उन्होंने अपने शिष्यों-अनुयायियों को बंधने को कहा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आज का मनुष्य जिन दुखों से पीड़ित है, उसमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने अपने खुद के अज्ञान या मिथ्या दृष्टि से पैदा किया है। इन दुखों का निराकरण सम्यक ज्ञान द्वारा ही किया जा सकता है; किसी के आशीर्वाद या वरदान से नहीं। सत्य या यथार्थ का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। अत: दु:ख से मुक्ति के लिए सत्य की खोज परम आवश्यक है। गौरतलब हो कि बुद्ध ने पहली बार धर्म को तार्किक कसौटी जाने की आवश्यकता को सामने रखा।
बुद्ध का दर्शन किसी का अनुगामी होना स्वीकार नहीं करता। वरन कहता है “अप्प दीपो भव!” अर्थात अपना दीपक आप बनो। तुम्हें किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं हैं। किसी मार्गदर्शक की खोज में भटकने से अच्छा है कि अपने विवेक को अपना पथप्रदर्शक चुनो। समस्याओं के निदान का रास्ता, मुश्किलों से हल का रास्ता हमारे खुद के पास है। सिर्फ अपने विवेक की सुनो। करो वही जो तुम्हारी बुद्धि को जंचे।
मित्रता ही सनातन नियम
बुद्ध विश्व कल्याण के लिए मैत्री भावना पर बहुत बल देते हैं। वे कहते हैं कि बैर से बैर कभी नहीं मिट सकता। मित्रता ही सनातन नियम है। पूरी दुनिया को शांति व प्रेम का संदेश देने वाले बौद्ध धर्म में कुछ ऐसे दिव्य सूत्र मिलते हैं जिन्हें अगर हम अपनी सोच का हिस्सा बना सकें तो सही मायनों में खुद को मानव कहला सकेंगे। हम वह हैं जो हम सोचते हैं, हम अपने विचारों से ही ऊपर उठते हैं और अपना संसार बनाते हैं। बुद्ध ने चेताया कि बुद्धि के दो ही रूप संभव हैं- कुटिल और करुण। बुद्धि यदि कुसंस्कारों में लिपटी है, स्वार्थ के मोहपाश और अहं के उन्माद से पीड़ित है तो उससे केवल कुटिलता ही निकलेगी, परन्तु यदि इसे शुद्ध कर लिया गया तो उसमें करुणा के फूल खिल सकते हैं। बुद्धि अपनी अशुद्ध दशा में इंसान को शैतान बनाती है तो इसकी परम शुद्ध दशा में व्यक्ति “बुद्ध” बन सकता है, उसमें भगवत सत्ता अवतरित हो सकती है। तथागत की यह विचार संजीवनी आज की महा औषधि है जो मनुष्य के मुरझाये प्राणों में नवचेतना का संचार कर सकती है।
संतुलन की धारणा को सर्वाधिक महत्व
गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में संतुलन की धारणा को सर्वाधिक महत्व दिया है। वे कहते हैं कि भोग की अति से बचना जितना आवश्यक है उतना ही तपस्या की अति से भी। बोधि वृक्ष के नीचे साधना करते समय बुद्ध को समझ आया था कि जीवन वीणा के तारों की तरह भांति है। ढीला छोड़ने पर सुर नहीं निकलते। अधिक कसने पर तार टूट भी सकते हैं।
इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का आग्रह किया। उनका कहना था कि जो बुद्धिमान होते हैं वे शास्त्रों से ज्ञान हासिल कर लेने के बाद उसे उसी तरह छोड़ देते हैं, जैसे धान से चावल निकालने के बाद भूसे को फेंक दिया जाता है। इसी बात को बुद्ध ने “मझ्झिम निकाय” में नौका की उपमा देकर बेहद खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई मनुष्य नदी पार करने के लिए नौका बनाता है और नदी पार करने के बाद भी उसे पीठ पर लादे चलता है, तो उसे समझदार कतई नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बुद्ध के बारे में कहना है, गीताकार के शब्दों में बुद्ध “स्थितप्रज्ञ” हो चुके थे। उन्हें “ब्रह्म-निर्वाण” का साक्षात्कार हो चुका था। सरल शब्दों में कहें तो उन्होंने देवत्व प्राप्त कर लिया था।‘’
पालि भाषा में रचित बुद्ध वाणी
बुद्ध वाणी से जुड़ा पालि भाषा का संपूर्ण साहित्य 52,602 पृष्ठों और 74,48,248 शब्दों का माना जाता है। इन सबमें धम्मपदं को बहुत ऊंचा और विशेष माना गया है। इसकी 423 गाथाओं या श्लोकों में ही बुद्ध के समस्त उपदेशों का सार निहित है। बुद्ध के उपदेशों पर जितना भी तात्विक और दार्शनिक विमर्श देखने को मिलता है, वह उनके बहुत बाद हुआ। नागसेन, बुद्धघोष, अनिरुद्ध, आचार्य, नागार्जुन और मैत्रेय नाथ जैसे विद्वानों और दार्शनिकों ने बुद्ध के दार्शनिक पक्ष को समाज के सामने रखा। ये ग्रंथ हमारी ज्ञान-परंपरा के लिए अमूल्य निधि हैं। बुद्ध का दर्शन मानव जीवन को संपूर्ण और परिपक्व बनाने के लिए आग्रहशील है।
गणतंत्र के प्रबल हिमायती
बुद्ध गणतंत्र के प्रबल हिमायती थे। इसलिए उनके दर्शन चिंतन में भी गणतंत्र की खूबियां स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। वे न केवल सामाजिक समानता पर जोर देते हैं और उसके लिए सामाजिक समाज के जातीय विभाजन को दोषी ठहराते हैं वरन आर्थिक अधिकार देकर व्याक्ति को उन सामंती संस्कारों से बचाए रखना चाहते हैं, जो धर्म और राजनीति की कुटिल संधियों की उपज थे।
जन्म, बोध प्राप्ति और परिनिर्वाण की साक्षी बैसाख पूर्णिमा
जानना दिलचस्प होगा कि बैसाख माह की पूर्णिमा बुद्ध के जीवन की तीन महत्वपूर्ण घटनाओं से अर्थात बुद्ध के जन्म, बोध प्राप्ति और परिनिर्वाण से जुड़ी है। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले इस महान विभूति ने महाराज शुद्धोधन के यहां राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया था। इसके बाद एक-एक करके कई बैसाख पूर्णिमा आयी और चली गयीं। फिर से एक महापुण्यवती बैसाख पूर्णिमा आयी, जब महातपस्वी सिद्धार्थ की अन्तर्चेतना में बुद्ध ने जन्म लिया। इस पुण्य घड़ी में सिद्धार्थ सम्यक् सम्बुद्ध बन गए और बैसाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा में रूपांतरित हो गयी। फिर संसार में सद्ज्ञान का आलोक फैलाने के बाद 80 वर्ष की अवस्था में एक अन्य महान बैसाख पूर्णिमा इस महामानव में महापरिनिर्वाण की साक्षी बनी।



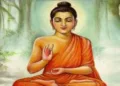













टिप्पणियाँ