संगठन में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने पर्याप्त सतर्कता रखी थी। डॉक्टर जी द्वारा निर्मित परंपरा के अनुसार, संघ का संपूर्ण कार्य लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। संघ की कार्यपद्वति का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें प्रत्येक स्तर पर विचार-विमर्श, चर्चा, मुक्तमत प्रदर्शन, व्यक्तिगत उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता, सामूहिक निर्णय तथा उसका एक मत से अनुसरण करने जैसे मूल्य समाहित रहते हैं
हमारे देश में प्रतिवर्ष 26 नवम्बर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत का संविधान अंगीकार किया गया था। भारत स्वतंत्र, सार्वभौम एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्वाभिमान के साथ विश्व के राष्ट्र-समूह में खड़ा हुआ था। संविधान की प्रस्तावना ‘हम भारत के लोग’ से प्रारंभ होती है। भीड़ को ‘लोग’ की संज्ञा नहीं दी जाती। ‘लोग’ यानी अपने स्वभाव के अनुसार, एक दिशा में चलने वाला समूह।
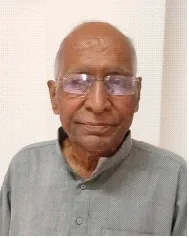
वरिष्ठ प्रचारक, रा.स्व.संघ
ऐसा नहीं है कि हमारा यह राष्ट्र संविधान के तहत ही लोकतंत्र है। हम प्राचीन काल से ही लोकतांत्रिक मानसिकता के हैं, इस कारण हमारा संविधान लोकतांत्रिक राज्य स्थापित करने वाला संविधान हुआ। लोकतंत्र यानी निरंतर विचार-विमर्श, चर्चा, मत प्रदर्शन की पूर्ण स्वतंत्रता, उपासना पद्धति की पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरे का मत सुनने की मानसिकता, केवल दूसरे के मत के प्रति ही सहिष्णुता नहीं, वरन् दूसरे के मत का आदर करना। भारतीय लोक जीवन में ये लोकतांत्रिक जीवन मूल्य गहराई तक समाए दिखते हैं।
वेद काल से भारत में ‘लोक सभ्यता’ विकसित होती आ रही है। इस काल में असंख्य मत-मतान्तरों का जन्म हुआ। अनेक पंथ, उपपंथ, संप्रदाय निर्मित हुए। अलग-अलग दर्शन निर्मित हुए। अनेक भाषाओं तथा कलाओं का विकास हुआ। हमारे अंदर ऐसा भाव रहता है कि ये सब हमारे हैं। तीर्थ यात्रा करते समय यह विविधता बाधा नहीं बनती। ‘भारतीय समाज तो गत हजारों वर्ष से लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों पर जीने वाला समाज है।’ इस समाज का लोकतांत्रिक जीवन, संविधान बनाने वालों ने शब्दबद्ध किया था। गुलामी के लंबे कालखंड के बाद भारतीय जीवन मूल्य संविधान के रूप में विश्व के सामने प्रकट हुए। यह युग प्रवर्तक काम है। संविधान समिति के सभी विद्वानों ने इसके लिए सामूहिक बुद्धिमत्ता के अनुसार निर्णय लिए थे।
हमारा संविधान स्वतंत्रता, समता और बंधुता के त्रिसूत्र पर आधारित है। स्पष्ट दिखता है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसके लिए अथक परिश्रम करने वाले डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तार व विकास करते समय इन तीनों जीवन मूल्यों को संगठन में रोपने का प्रयत्न प्रारंभ से ही किया था। यह निम्नलिखित बिन्दुओं से परिलक्षित होता है-
- उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय अनेक नेताओं से विचार-विमर्श करने के बाद ही संघ स्थापना का निर्णय लिया था।
- . संगठन कार्य का नाम 6 महीने बाद निश्चित हुआ था। 26 लोग उस बैठक में उपस्थित थे। बैठक में तीन नामों का सुझाव आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपटका मंडल और भारतोद्धारक मंडल। बैठक में मुक्त चर्चा हुई, विचार- विमर्श हुआ, मतदान हुआ। ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ नाम पर 20 लोगों ने अपनी सहमति दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विस्तार से सामने रखने के लिए दो-तीन लोगों के वक्तव्य हुए। इस नाम का चुनाव होने के बाद डॉक्टर जी का छोटा भाषण हुआ।
- नामकरण होने के बाद डॉक्टर जी ने एक प्रयोग किया। कुछ प्रमुख स्वयंसेवकों को इन विषयों पर लेख लिखने को कहा गया कि संघ का ध्येय और नीति क्या होनी चाहिए, नियमावली क्या होनी चाहिए, संघ में किसे प्रवेश देना चाहिए, हमें संघ का विस्तार करना है आदि।
 कुछ स्वयंसेवकों का मत था कि रामटेक यात्रा में व्यवस्था के लिए हमें जाना चाहिए। यात्रा की सुव्यवस्था करना केवल संघ का विषय नहीं था। डॉक्टर जी ने अनाथ विद्यार्थी गृह के संचालक, बजरंग मंडल के पदाधिकारी और संघ के स्वयंसेवकों की संयुक्त बैठक बुलाई। सबका यही मानना था कि रामटेक यात्रा की व्यवस्था पर ध्यान देना आवश्यक है। उसके लिए एक वेष भी निश्चित किया गया।
कुछ स्वयंसेवकों का मत था कि रामटेक यात्रा में व्यवस्था के लिए हमें जाना चाहिए। यात्रा की सुव्यवस्था करना केवल संघ का विषय नहीं था। डॉक्टर जी ने अनाथ विद्यार्थी गृह के संचालक, बजरंग मंडल के पदाधिकारी और संघ के स्वयंसेवकों की संयुक्त बैठक बुलाई। सबका यही मानना था कि रामटेक यात्रा की व्यवस्था पर ध्यान देना आवश्यक है। उसके लिए एक वेष भी निश्चित किया गया। - यह आवश्यक महसूस हुआ कि संघ के बढ़ते काम के साथ संगठन की व्यवस्था में भी कुछ बदलाव होना चाहिए। संघ चालकों की बैठक में सरसंघचालक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के सहायक के रूप में मा. सरकार्यवाह श्री बालासाहेब हुद्दार तथा सर सेनापति के रूप में मार्तंड राव जोग का नाम निश्चित हुआ। शाखा में डॉक्टर जी को ‘सरसंघचालक प्रणाम’ दिया गया। उस दिन की डॉक्टर जी ने डायरी में जो लिखा, वह पढ़ने व सुनने लायक है-‘संघ का जन्मदाता मैं नहीं, आप हैं, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं।’ ‘ जब तक आपकी इच्छा व आज्ञा रहेगी तब तक मैं यह दायित्व संभाले रहूंगा।’ ‘परंतु अगर कभी आपको यह लगे कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं और मेरे कारण संघ का नुकसान हो रहा है, तो आप अन्य कोई योग्य व्यक्ति इस पद के लिए निर्वाचित कर सकते हैं।’
- 1929 के दौरान शाखाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। तरुण कार्यकर्ताओं का उत्साह सतत बढ़ रहा था। कार्यकर्ता एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करने के लिए डॉक्टर जी से आग्रह करने लगे। कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि शिव राज्याभिषेक के दिन विराट शक्ति प्रदर्शन करने से स्वयंसेवकों का आत्मविश्वास तथा उत्साह बढ़ेगा। परंतु डॉक्टर जी का मन कह रहा था कि जल्दबाजी में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे अंग्रेजों की सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। लेकिन उन्होंने युवाओं को स्वत: मना नहीं किया। माननीय संघचालकों को पत्र लिखकर इस विषय पर उनकी राय मांगी कि एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना कहां तक हितकर होगा। उसके बाद तय हुआ कि अभी कोई बड़ा आयोजन नहीं करना चाहिए।7. यह तब की बात है जब स्वयंसेवकों को लगा कि डॉक्टर जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है और कि उनका बचना अब संभव नहीं दिखता। सभी को ऐसा लग रहा था तो निसंदेह डॉक्टर जी को भी यह भान हुआ होगा। अपने पास ही बैठे श्री यादव राव जोशी से उन्होंने पूछा, ‘संघ के वरिष्ठ अधिकारी के दिवंगत होने के बाद उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ करोगे क्या? संघ एक बड़ा परिवार है, परिवार प्रमुख का स्वरूप भी सादगी से परिपूर्ण होना चाहिए।’
डॉक्टर जी के जीवन के उक्त सात चुनिंदा प्रसंग बताने के पीछे उद्देश्य यही है कि हम यह समझें कि संगठन में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में डॉक्टर जी ने कितनी सतर्कता रखी थी। डॉक्टर जी द्वारा निर्मित परंपरा के अनुसार, संघ का संपूर्ण कार्य लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। संघ की कार्यपद्वति का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें प्रत्येक स्तर पर विचार-विमर्श, चर्चा, मुक्तमत प्रदर्शन, व्यक्तिगत उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता, सामूहिक निर्णय तथा उसका एक मत से अनुसरण करने जैसे मूल्य समाहित रहते हैं।
संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल तथा अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठकें प्रत्येक वर्ष होती हंै। संपूर्ण कार्यवाही लिखित रूप में रखी जाती है। गत वर्ष की बैठक की कार्यवाही पढ़ी जाती है व उसका अनुमोदन कराया जाता है। प्रस्तावों पर मुक्त चर्चा होती है। किसी को भी उसमें भाग लेने से रोका नहीं जाता। प्रस्ताव प्रसार माध्यमों को दिए जाते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष में संगठन के चुनाव होते हैं।
1948 में महात्मा गांधी की हत्या में संघ के हाथ होने का झूठा एवं गलत आरोप लगाकर स्वतंत्र भारत की तत्कालीन सरकार ने संघ पर पाबंदी लगाई थी। कानून का पूर्णत: पालन करते हुए संघ ने उस प्रतिबंध को सहा। जगह-जगह सत्याग्रह किया गया। कहीं से भी हिंसा की खबर अपवाद स्वरूप में भी नहीं मिली। पदेन सरसंघचालक माननीय क्षेत्र संघचालकों से चर्चा कर नए सरसंघचालक का नाम निश्चित करते हैं। अधिकारी एवं स्वयंसेवक (बाल शिशु स्वयंसेवक भी) के बीच कोई भेद नहीं होता, सभी स्वयंसेवक होते हैं।
शाखा, संघ का प्रतिनिधिक स्वरूप है। संघ शाखा का कोई दरवाजा नहीं होता यानी यह ‘ओपन नेशनल स्कूल’ जैसी होती है। शाखा के 8-10 सेवकों की कार्यसमिति होती है। संघ में उसे शाखा टोली कहते हैं। कार्यसमिति की साप्ताहिक तथा पाक्षिक बैठकें होती हैं। चर्चा में, विचार विमर्श में तथा निर्णय प्रक्रिया में सभी शामिल होते हैं। इसमें गत बैठक की समीक्षा एवं आगामी योजना का विचार होता है। कितने और कौन नए स्वयंसेवक बने, इसकी जानकारी दी जाती है। बस्ती के घरों में संपर्क करने व उन्हें संघ की जानकारी देने का काम सहज रूप से होता रहता है। प्रत्येक शाखा अपना वार्षिक उत्सव आयोजित करती है। उसमें वर्ष भर का वृत्त सबके सामने रखा जाता है।
लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों के अनुसार, संघ स्वयंसेवकों का आचार-विचार सहजता से होता रहता है, जिसका उदाहरण 1975 में आपातकाल में दिखा था। तब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार ने लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों पर आधारित सभी मानवीय अधिकार रद्द कर दिए थे। अन्याय के विरुद्ध शिकायतों के लिए न्यायालयों के दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे। आपातकाल समाप्त हो तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना हो, इस हेतु ‘लोक संघर्ष समिति’ के नेतृत्व में सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। उस आंदोलन में सत्याग्रह में भाग लेना अंधेरे कुएं में छलांग लगाने जैसा था। आगे क्या होगा, उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। ऐसी अनिश्चितता की स्थिति में भी एक लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह में भाग लिया था। इस कारण आपातकाल अंतत: समाप्त हुआ। कैद हुए सभी लोगों को कारागृह से मुक्त कर दिया गया। लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों की पुन: स्थापना हुई। कुछ लोगों की जेल में ही मृत्यु हो गई। कहीं भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा।

स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इन तीन तत्वों के बारे में डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर के विचार पढ़ने योग्य हैं-‘‘मेरे तत्वज्ञान में स्वतंत्रता और समता के अतिक्रमण से संरक्षण मिले, इसलिए केवल कानून का स्थान परिकल्पित किया गया है। परंतु इसे मैं बहुत गौण मानता हूं। कारण, मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्रता और समता के उल्लंघन के विषय में कानून निश्चित रूप से समर्थ होगा। मैं बंधुत्व को सर्वोच्च स्थान देने की इच्छा करता हूं। कारण, स्वतंत्रता और समता को यदि नकार दिया जाए तो बंधु भाव ही सच्चा रक्षक होता है। सहभाव बंधुत्व का दूसरा नाम है और बंधुत्व या मानवता धर्म का दूसरा नाम। कानून धर्म के परे होने के कारण कोई भी उसका उल्लंघन कर सकता है। इसके विपरीत सहभाव या धर्म पवित्र हैं, इस कारण उनका सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य समझा जाता है।’’(पुस्तक ‘बोल महामानव के’, पृष्ठ क्र.125)
बंधुभाव धर्म तत्व है, ऐसी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति के अंत:करण में निर्माण करना एक बड़ा राष्ट्रीय कार्य है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है-‘व्यक्ति की प्रतिष्ठा, राष्ट्र की एकता तथा एकात्मता का आश्वासन देने वाली बंधुता प्रवर्धित करने का संकल्प’-बंधु भाव का विकास ही स्वतंत्रता तथा समता है,यही इन जीवन मूल्यों का आश्वासन दे सकता है। संघ शाखा चलाने का उद्देश्य है हिंदू समाज में बंधु भाव जाग्रत करके उसे मजबूत करना। शाखा में गाए जाने वाले एक गीत की एक पंक्ति है-‘सभी हिंदू सहोदर हैं यह जन-जन को कहना’। निसंदेह सामूहिक रूप से ‘भारत माता की जय’ कहने में भातृत्व भावना का विकास होता है।




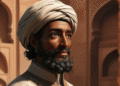

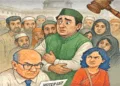












टिप्पणियाँ