जनता ने फरमान सुना दिया। आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली के विधानसभा चुनावों में महज 22 सीट पर सिमट गई और पार्टी सुप्रीमो व दस साल तक मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल सहित मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज भी सत्ता-विरोधी लहर में डूब गए। यह महज चुनाव नहीं बल्कि अण्णा हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली और राजनीति बदलने के दावे करने वाली पार्टी को एक संदेश है कि कथनी और करनी में फर्क ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। केजरीवाल बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे के दावों के साथ दिल्ली की सत्ता में आए थे, लेकिन जब ‘शीशमहल’ से आप का कब्जा हटेगा तो वे उन्हीं नेताओं की पांत में नजर आएंगे जिनके नाम वे कभी रोजाना भ्रष्ट नेताओं की सूची में लहराते थे।
किसी भी मायने में दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों को सामान्य नहीं माना जा सकता। भाजपा की जीत के कई कारण हो सकते हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी केजरीवाल की हार के कारणों की पड़ताल है क्योंकि जनता की राजनीतिक स्मृति कमजोर होती है। यह किसी चेहरे की आड़ में एक एनजीओ मार्का और करीने से बुनी गई डिजाइनर राजनीति के उत्थान और पतन की दास्तान है। अप्रैल 2011 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर अण्णा हजारे के चेहरे के साथ केजरीवाल और उनके साथियों के अनशन ने यूपीए-2 सरकार में जारी भ्रष्टाचार और नीतिगत पंगुता के खिलाफ जनाक्रोश को हवा दी और फिर रामलीला मैदान में अण्णा हजारे के अनशन के साथ माहौल इसी मैदान में राष्ट्रकवि दिनकर के उद्घोष, ‘सिहासन खाली करो कि जनता आती है, वाला हो चुका था। अण्णा के साथी केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के योद्धा और चेहरे के तौर पर उभरे। इस आंदोलन की मांग थी केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति। लोकपाल यानी वह जो निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी ऊपर होगा और उन्हें भ्रष्टाचार से रोकेगा। और इस आंदोलन के दौरान केजरीवाल लगातार खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ गैरराजनीतिक ‘क्रूसेडर’ बताते रहे। लेकिन उन्होंने 2012 में एक राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी बनाई और चुनावी राजनीति में उतर गए। उसके बाद 2013 से अब तक की राजनीति उनके लिए एक बेहद सुखद यात्रा रही है। दिसंबर 2013 में चंद दिनों के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाने के बाद केजरीवाल अकेले दम पर 2015 और 2020 में प्रचंड बहुमत से दिल्ली की सत्ता में आए।
लोकपाल को भुला दिया
कहते हैं कि किसी क्रांतिकारी को सत्ता मिल जाए तो जल्दी ही वह भ्रष्ट और निरंकुश तानाशाह हो जाता है। 2015 में 67 सीटें जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने केजरीवाल ने उसके बाद फिर कभी लोकपाल की चर्चा नहीं की। यहां तक कि फरवरी में मुख्यमंत्री बनने के बाद मार्च में उन्होंने पार्टी के ही लोकपाल एडमिरल (सेवानिवृत्त) एल. रामदास को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ ही, उस दौर की खबरें बताती हैं कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे संस्थापक सदस्यों के साथ तनाव इतना बढ़ा कि पार्टी की सुप्रीम काउंसिल की बैठक में योगेंद्र यादव के साथ मारपीट हुई जिसमें उनका पैर टूट गया। इस बैठक के बाद योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और प्रो. आनंद कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मेधा पाटकर ने विरोध में इस्तीफा दिया तो कुमार विश्वास जैसे लोग किनारे कर दिए गए।
टकराव की राजनीति में माहिर
यहां से एक अलग केजरीवाल का उदय हुआ जो पार्टी और सरकार, दोनों में सर्वेसर्वा थे। सत्ता की राजनीति नहीं करने वाले केजरीवाल इसके खिलाड़ी बन गए। मीडिया और टीवी कैमरों की बदौलत सत्ता में आए केजरीवाल आरोप-प्रत्यारोप और टकराव की राजनीति के माहिर थे। प्रचार की ताकत में उनका अखंड विश्वास ऐसा था कि मानों इसकी बदौलत वे अनंत काल तक सत्ता में रहेंगे। भारी प्रचार बजट की बदौलत उन्होंने उन्हीं मीडिया समूहों का मुंह जिसे आप कार्यकर्ता गोदी मीडिया कहते थे, अशर्फियों से बंद कर दिया। इसी का नतीजा ये रहा कि केजरीवाल के आए दिन के आरोप तो छपते रहे लेकिन उनके माफीनामे कभी चर्चा का विषय नहीं बने। एक सड़क के उद्घाटन की खबर तो छपी लेकिन पानी और सीवर की समस्या मीडिया से गायब रही। यह एक ऐसा राजनीतिक दौर था जहां राजनीति की शैली नेता की तरह नहीं बल्कि किसी माफिया सरगना की तरह थी। योगेंद्र यादव की घटना तो थी ही, केजरीवाल व उनके सहयोगियों पर कभी दिल्ली के मुख्य सचिव को घर बुला कर पीटने के आरोप लगे तो कभी अपनी रिश्तेदार और पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल को ‘शीशमहल’ में बुला कर पिटवाने के आरोप लगे। यह देश की राजधानी में अविश्वसनीय था।
ये केजरीवाल के आविष्कार
आरोप लगाकर छूमंतर होने, जवाब मांगे जाने पर खुद को पीड़ित की तरह पेश करने और टकराव की राजनीति केजरीवाल के अविष्कार हैं। इसकी बदौलत जितनी सफलताएं मिल सकती थीं, वो उन्हें मिली। नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी के तौर पर खुद को स्थापित करने के प्रयासों में वे यहां तक कह गए कि उनकी हत्या करा सकते हैं। और चुनाव से ऐन पहले उन्होंने भारतीय राजनीति का सबसे ऐतिहासिक बयान दिया कि हरियाणा सरकार यमुना के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली के लोगों की हत्या के प्रयास कर रही है।
जनता अब शायद ही किसी आंदोलन पर विश्वास करे
लेकिन इस राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और केजरीवाल की हार से कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, यह कि राजनीति में जनता को कुछ रेवड़ियों के साथ कुछ बुनियादी सुविधाएं भी देनी होंगी। बुनियादी सुविधाओं के मामले में वे फेल रहे। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा तो ठीक है लेकिन घर से निकल कर बस स्टाप तक जाने के लिए उन्हें सीवर के पानी से बजबजाती सड़कों से नहीं गुजरना पड़े, यह भी सुनिश्चित करना होगा। दूसरे, आप यह नहीं समझ पाई कि आरोप साबित नहीं कर पाने से विश्वसनीयता को चोट पहुंचती है और इसके नुकसान होंगे। तीसरा, यह कि कि सिर्फ आत्ममुग्ध प्रचार और मीडिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कला जनसुविधाओं के अकाल को नहीं भर सकती। लेकिन अंत में केजरीवाल के उत्थान और पतन का सबसे बड़ा सबक यह है कि कथनी और करनी में भारी अंतर से जनमानस में राजनीति के प्रति संशय पैदा होता है। जब दूसरों पर आरोप लगाने वाले और खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल शीशमहल, शराब घोटाले में घिरे तो ‘मेरी कमीज तुमसे ज्यादा सफेद है’, की उनकी पूरी राजनीति ढह गई।
केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा हिंदी लेखक सुदर्शन की कालजयी कहानी ‘बाबा भारती का घोड़ा’ से मेल खाती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की राजनीति से उपजे स्वघोषित ‘अराजकतावादी’ और ‘कट्टर ईमानदार’ केजरीवाल ने उसी तंत्र का हिस्सा बनकर इस लड़ाई को ही अविश्वसनीय बना दिया। केजरीवाल की विदाई नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी क्षति यह है कि अब जनता शायद ही किसी आंदोलन या इससे निकले नेतृत्व पर विश्वास करे। यह कभी उम्मीद जगाने वाले एक राजनीतिक प्रयोग का त्रासद अंत है।
(लेखक मीडिया रणनीतिकार व राजनीतिक विश्लेषक हैं)

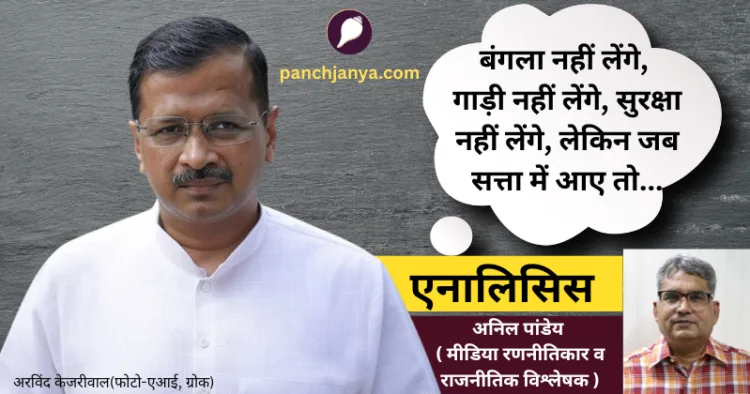
















टिप्पणियाँ