आज पूरे भारतवर्ष का सड़क, रेल और यहाँ तक कि वायु मार्ग भी प्रयागराज की तरफ रुख कर चुका है, सारी सड़के रोम ना जाकर कुम्भ को ओर मुड़ गयी प्रतीत होती है। कुम्भ की तरफ बढती भीड़ को देख लगता है कि अपनी सभ्यता और संस्कृति की तरफ नयी पीढ़ी में आये आकर्षण के साथ-साथ सोशल मीडिया और दिखावा संस्कृति ने इस ओर उकसाया है। पर गंगा-यमुना या कहे कि हर नदी और तालाब की पवित्रता भारत के लोक में गहराई से रची-बसी हुई है। मकर संक्रांति का दिन हो या मौनी अमावस्या का तो हर नदी तालाब गंगा बन जाती है और हम भारतीय किसी भी नदी में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र महसूस कर लेते है। मिथक, धर्म और विज्ञान की इस पहेली में प्रयाग में कुम्भ स्नान जो इतना विराट हो सकता है जिसे सुलझा पाना बड़ी ही टेढ़ी खीर है। इंडिया टुडे की माने तो पिछले मौनी अमास्या के दिन 5.71 करोड़ लोगो ने प्रयाग में स्नान किया, जैसे पूरा का पूरा इटली प्रयाग के घाट पर पहुँच गया हो। साधु-संतों की जमात के साथ आमजन का यह सैलाब कहीं-न-कहीं यह नदी-पानी के उत्सव की मनसा की ओर इंगित करता है, जहाँ नदी देव स्वरुप मानी गयी जिसे कुंभ नाम दिया होगा। आज जब गंगा और यमुना के अस्तित्व का उत्सव मनाया जा रहा है तो सहज ही ध्यान इसकी उत्पति और अब तक के सफ़र पर ध्यान तरफ चला जाता है।
प्रयाग का महत्व न केवल धार्मिक ग्रंथों में है, बल्कि यह हमारे इतिहास, संस्कृति, और परंपराओं में गहरे से समाहित है, जो हमारे अस्तित्व और पहचान से जुड़ा हुआ है। पुराणों में इस क्षेत्र की उपमा जनन तंत्र से की गयी है जहाँ गंगा और यमुना रूपी दो जंघाए प्रयाग में मिलती है और समूचे दोआब क्षेत्र जिसका आखिरी सिरा प्रयाग है को उपजाऊ और समृद्ध बनाती है। प्रतीकात्मक रूप से प्रयाग की भूमि जीवन की उत्पत्ति और पोषण की भूमि है। नदियों का मिलना अपने-आप में एक अभूतपूर्व घटना है, जो प्रयाग है, जो मानव जीवन को पोषित करती है, शायद इसी वजह से किसी भी दो नदियों की मिलन स्थली प्रयाग बन गयी जैसे देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, और नंद प्रयाग। गंगा के अतिरिक्त नदियों के मिलन को प्रयाग बुलाने का चलन है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास भी दो नदियाँ मिलती हैं, जिसे भी प्रयाग कहा जाता है, जो इस बात को बताने हेतु काफी है कि प्रयाग हमारे सभ्यता की सांस्कृतिक कड़ी है।
भारतीय वांग्मय में वेद,उपनिषद,पुराण के साथ-साथ इतिहस के ग्रन्थ रामायण और महाभारत भी गंगा-यमुना की वेणी यानी संगम प्रयाग के भौगोलिक और धार्मिक संदर्भों से भरे पड़े हैं। गंगा और यमुना के मिलन का जिक्र पहली बार ऋग्वेद के खिलसूक्त में आया है, पर वहां इसे प्रयाग नाम नहीं मिला है बल्कि इसे सित-असित संगम के रूप में दर्शाया गया है। “सित” का अर्थ श्वेत, धवल यानि गंगा) और “असित” यानी गहरे रंग वाली यमुना से है।
सितासिते सरिते यत्र सङ्गते तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतंतई I
ये वै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते II
इस पवित्र संगम को पहली बार प्रयाग नाम उपनिषद में मिलता है। पुराण तो प्रयाग के महात्म से भरे पड़े हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार प्रयाग ही वो जगह है जहाँ शंखासुर से वेदों को मुक्त करने के लिए भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, जहाँ बह्मा ने बहुत बड़े पैमाने पर यज्ञ का आयोजन किया जहाँ वेदों को रखा गया। और यही घटना प्रयाग के नामकरण का आधार भी बनी ‘प्र’ माने बहुत बड़ा ‘याग’ माने यज्ञ। पौराणिक यज्ञ का प्रसार पूरब में गया से लेकर पश्चिम में कुरुक्षेत्र और पुष्कर तक था और यही कारण है कि ये सारे क्षेत्र अनेकानेक तीर्थ से भरे पड़े हैं और उनमें प्रयाग तीर्थराज है। ऋग्वेद में सित-असित संगम का जिक्र विशुद्ध भौगोलिक सन्दर्भ में है। धीरे-धीरे सभ्यता के विकास के साथ-साथ तीर्थ केंद्र विकसित हुए, तीर्थ यात्रा का भी रिवाज शुरू हुआ और गंगा-यमुना का संगम हमारी संस्कृति की शुरुवाती तीर्थ क्षेत्र के रूप में उभर, प्रयाग के रूप में सामने आया, जिसका जिक्र पहली बार उपनिषद में आया और पौराणिक आख्यानों का आधार बना।
महाभारत में प्रयाग का विवरण अग्रणी तीर्थ के रूप में हुआ है साथ ही साथ तीर्थ यात्रा के मार्ग का भी जिक्र है। आदि पर्व में सोम, वरुण और प्रजापति की जन्मस्थली प्रयाग में गंगा यमुना संगम सहित यहाँ के स्थानीय भूगोल और स्थान का वर्णन है, जिसकी निशानदेही प्रयाग क्षेत्र में मौजूद आज के स्थानों से की जा सकती है। वही आदिकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित वाल्मीकि रामायण में सम्पूर्ण प्रयाग क्षेत्र बार-बार ऋषियों की ताप और यज्ञस्थली के रूप में स्थापित होता है, चाहे राम-लक्ष्मण के वनगमन का समय हो, भरत का चित्रकुट आगमन हो या भी पुष्पक विमान से लंका वापसी समय आकाश से संगम का अवलोकन हो। यह संस्कृति के विकास का यज्ञ या अरण्यक कालखंड का द्योतक है, जो वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक से परिलक्षित भी होता है
यत्र भागीरथी गंगा यमुना भिप्रवर्तते।
जगमुस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्ययसुमदृद्वनम।।
मनुस्मृति जैसे स्मृति ग्रन्थ प्रयाग का जिक्र हिमालय और विंध्याचल के बीच बसे मध्य देश का भूगोल बताने के लिए करते है जिसके पूर्वी सिरे पर गंगा-यमुना का संगम है।
भारतीय वांग्मय ही नहीं भारत के साहित्यिक रचना संसार और विभिन्न कालखंडों के काव्य गंगा-यमुना के संगम प्रयाग क्षेत्र का सांस्कृतिक, धार्मिक, और प्रतीकात्मक महत्व दर्शाते हैं। कालिदास के काव्य संसार में तो गंगा और यमुना के संगम, दोनों नदी के पानी के बारीक़ अंतर और संगम स्नान के महात्म उपमा अलंकार के माध्यम से विस्तार से वर्णित है। प्रयाग में स्नान को दार्शनिक तत्वबोध के बिना भी मोक्ष मिलने का रास्ता बताया है। हजारों सालों से अनेकों ग्रन्थ, साहित्यकार संगम पर दोनों नदियों के पानी के अलग-अलग रंग और प्रकृति का जिक्र करते आये हैं, जो आज भी संगम पर दीखता है जहा गंगा का साफ़ पानी यमुना के गहरे रंग वाले पानी से मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी दोनों नदियों में बह के आ रही अलग-अलग मिटटी की मात्रा और प्रवृति के कारण दोनों नदियों के पानी का रंग अलग-अलग होता है, जिसका जिक्र कालिदास बखूबी करते हैं। इस बात का भारतीय साहित्य में सबसे पहला जिक्र दूसरी शताब्दी में नाटककार भास की रामकथा पर आधारित प्रतिमानाटकम में है जिसमे अपनी माँ कैकई से क्षुब्ध भरत उनकी उपमा गंगा और यमुना के बीच एक प्रदूषित नदी से किया है।
भास के बाद के संस्कृत साहित्यकारों के बीच तो गंगा यमुना के संगम और पानी के वर्णन के लिए साहित्यकारों में होड़ सी लग जाती है। सुबंधु ने ‘वासवदत्ता’ में संगम की तरंगो की तुलना नायक वासवदत्ता के मोतियों के हार से की है, तो बाणभट्ट (हर्षचरित में), दण्डी, दामोदरगुप्त, मुरारी, श्रीहर्ष, केशवदास सहित अनेकों ने अपनी कृति में अनोखे उपमा से संगम के महत्व को दर्शाया है, कहीं संगम के चमक की तुलना मोती के हार से की गयी है तो कोई अपने राजा के प्रताप और ओज देख रहा है। केशवदास जो कि अलंकर सम्प्रदाय के कवि माने गए, का संगम का वर्णन प्रभावी साहित्यिक अभिव्यक्ति की प्रकाष्ठा है। अपनी एक रचना में संगम पर बिखरे रेत के कण मानो छोटे-छोटे देव स्वरुप है जो गंगा-यमुना का सत्कार कर रहे हैं। बाद के काल में जब मानव बसावट पूर्ण रूप से गंगा के मैदान में पसर जाती है, तब प्रयाग को एक पवित्र त्तीर्थ के रूप में प्रसिद्धि मिलती है, अरण्यक से तीर्थ संस्कृति का दौर आता है। भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों, उनकी महिमा और तीर्थ यात्रा के तरीकों पर अनेक ग्रन्थ लिखे गए और सब में प्रयाग को एक बार फिर विशिष्ट स्थान मिला। शुरुवाती लक्ष्मीधर भट्ट लिखित तीर्थ टीका से लेकर, नारायण भट्ट, जिनप्रभु सूरी, वाचस्पति मिश्र, मित्र मिश्र तक सबमें प्रयाग का विशेष वर्णन मिलता है और सब एक सुर में साथ प्रयाग की तीर्थ यात्रा नंगे पैर करने की बाध्यता बताते हैं।
भारतीय धर्म ग्रन्थ वेद-पुराण इतिहास से लेकर तमाम साहित्यिक रचनायें प्रयाग की ऐतिहासिकता की गवाही देते हैं। शुरुवाती दौर में सब इसे गंगा और यमुना नदी के संगम तीर्थराज के रूप में इसकी पवित्रता को प्रतिस्थापित करते हैं। वर्तमान में प्रयाग ना सिर्फ गंगा यमुना बल्कि अदृश्य नदी सरस्वती के संगम के रूप में जन मानस में रचा बसा है, यह गंगा यमुना की वेणी नहीं बल्कि गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है। इस बात की पहली निशानदेही महाकवि विद्यापति की रचना भू-परिक्रमण में मिलती है, जहाँ तीर्थराज प्रयाग में दो नहीं तीन नदियों के समन्वय जिक्र है। विद्यापति के बाद की रचनाओ में सरस्वती नदी गंगा यमुना के साथ-साथ संगम में स्थान पाती है, हालांकि तुलसीदास प्रयाग के लिए वेणी यानी दो नदियों का संगम बताते हैं पर सरस्वती नदी का स्पष्ट रूप से गंगा-यमुना के साथ उल्लेख भी करते हैं। वही केशवदास की रचनाओं में प्रयाग का संगम त्रिवेणी है जिसमें सरस्वती नदी गंगा यमुना के साथ अदृश्य रूप में शामिल है। यहाँ तक कुछ पुराण भी प्रयाग के संगम में सरस्वती के अदृश्य अस्तित्व को स्वीकारते हैं जिसमें पद्मपुराण, ब्रह्मपुराण और नारदीयपुराण प्रमुख है। भारतीय जन-मानस का प्रभाव मुस्लमान लेखको द्वारा उस दौर के पर्सियन में लिखे ग्रंथों में भी झलकता है जिसमें प्रयाग पर गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का जिक्र मिलता है।
सरस्वती नदी भारत की सभ्यता की आदि नदी है, जिसके किनारे भारतीय सभ्यता पनपी, जिसके तट पर वेद की ऋचाएँ वजूद में आई, भारतीय संस्कृति ने शुरुवाती आकार लिया और जिसका अमिट छाप आज भी दृष्टिगोचर है। बाद में भले बड़े पैमाने पर आये पर्यावरणीय बदलाव के कारण सरस्वती नदी भले सूख गयी पर जनमानस नदी को कभी भूल नहीं पाया। प्रयाग में सरस्वती एक अंतर्ध्यान मुद्रा में गंगा-यमुना के साथ संगम करती हुई निरुपित होती है जो सरस्वती नदी से सभ्यतागत जुडाव की लोक स्मृति का निरूपण है, जिसे भारतीय समाज ने लोक व्यहार में संजो लिया है।
प्रयाग हमारी समृद्ध जल और नदी संस्कृति का प्राचीनतम आयाम है,भारतीय ज्ञान परम्परा के सतत प्रवाह जैसे हजारो साल से कुंभ स्नान के रूप में अनवरत जारी है। प्रयाग संगम और कुम्भ के ऐतिहासिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, और सभ्यतागत लोक समृति के सम्बन्ध इसे अजर अमर बनाते है। गंगा-यमुना और सरस्वती के संगम का तीर्थ स्वरुप आज भी लगभग उसी रूप में है, आज भी गंगा की धवल और यमुना की मटमैली धारा उसी तरह संगम में मिलती है जैसे ऋग्वेद के खिलसुक्त में वर्णित है। तभी तो भारतीय सभ्यता इस धरा की एक मात्र जीवित सभ्यता है यही सतत ज्ञान गंगा का प्रवाह है यही सनातन है।





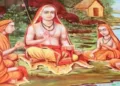












टिप्पणियाँ