क्या कांग्रेस और डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर का प्रभाव परस्पर विपरीत काम करता है? जवाब है, हां। जहां भारत की राजनीति में कांग्रेस की स्थिति दिन प्रति दिन खराब हो रही है, वहीं देश के वर्तमान कथानक में आंबेडकर का व्यक्तित्व परिवर्तन, चेतना और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप तेजी से उभर रहा है। डॉ. आंबेडकर से कौन नफरत करता था और क्यों? कौन 20वीं सदी के इस महान भारतीय समाज सुधारक का 1956 में उनके निधन से पहले के कुछ वर्षों में तिरस्कार करता रहा और उन्हें भारतीय राजनीति में हाशिये पर ही रखा?

कांग्रेस का पाखंड व अवसरवाद

स्तंभकार एवं भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व अध्यक्षं
डॉ. आंबेडकर की विरासत पर दावा करने के प्रयासों में कांग्रेस वैचारिक भ्रम के भंवर में डूबती जा रही है। दुनिया जानती है कि बाबासाहेब की नेहरू कितनी अवहेलना करते थे। 1955 में प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को ‘भारत रत्न’ से सम्मानित करने में उन्हें तनिक संकोच नहीं हुआ, जबकि बाबासाहेब को इस सम्मान को पाने के लिए 35 साल इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस के बागी नेता वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार (भाजपा और वाम दलों द्वारा समर्थित) ने 1990 में इतिहास के इस अन्याय का अंत करते हुए डॉ. आंबेडकर को मरणोपरांत ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया। संसद के केंद्रीय सभागार में उनका चित्र लगाया गया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू हुआ। नेहरू ने डॉ. आंबेडकर को ‘खलनायक’ के रूप में चित्रित किया था और भारतीय जनमानस में बसी उनकी महान छवि को धूमिल करने की हर संभव कोशिश की। आज उसी कांगेस पार्टी को अपनी डूबती राजनीतिक नाव को पार लगाने और किस्मत को चमकाने के लिए डॉ. आंबेडकर के नाम का उपयोग करने में कोई हिचक नहीं है। यह कांग्रेस नेतृत्व के पाखंड और अवसरवाद की पराकाष्ठा है।
आंबेडकर के साथ अप्रिय संबंध
डॉ. आंबेडकर के साथ कांग्रेस के संबंधों को स्पष्ट रूप से दो अलग-अलग चरणों में बांटा जा सकता है। पहला, वह दौर जब गांधी जी जीवित थे और दूसरा, 30 जनवरी, 1948 को गांधी जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद का कालखंड। लौह पुरुष सरदार पटेल की मृत्यु (15 दिसंबर, 1950) के बाद कांग्रेस की प्रभुतापूर्ण शक्ति नेहरू के हाथों में थी। प्रधानमंत्री के शक्तिशाली पद पर आसीन होने के बाद नेहरू की सत्तावादी प्रवृत्ति का आवरण खुलने लगा। वे उन सभी नेताओं (कांग्रेस के भीतर या बाहर) के राजनीतिक जीवन का अंत करते गए जो वैचारिक मुद्दों पर उनसे असहमत थे या जिनके प्रति उनकी व्यक्तिगत रंजिश थी।
नेहरू अपने वंश के अन्य लोगों की तरह ही प्रभुता की भावना से ग्रसित थे। नेहरू की आधिपत्यपूर्ण भावना उन लोगों के अनुभव, योग्यता, ज्ञान और बौद्धिक क्षमताओं का तिरस्कार करती रही, जो उनकी हां में हां मिलाने से इनकार करते। हालांकि, गांधी जी का दृष्टिकोण समावेशी था। उन्होंने नेहरू को अपने मंत्रिमंडल में तीन गैर-कांग्रेसी नेताओं को शामिल करने के लिए राजी कर लिया था। वे थे- डॉ. आंबेडकर, (जो बाद में भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए), डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार बलदेव सिंह। डॉ. मुखर्जी की कश्मीर जेल में नेहरू के मित्र शेख अब्दुल्ला सरकार के कैदी के रूप में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। डॉ. आंबेडकर को भी नेहरू के प्रतिशोध की आंच झेलनी पड़ी थी। संसदीय चुनाव (माना जाता है कि नेहरू के वरदहस्त में इसमें धांधली की गई) में पराजित होने के बाद आंबेडकर को भारतीय राजनीति की सत्तात्मक संरचना से हमेशा बाहर ही रखा गया।
नेहरू के प्रतिशोध का शिकार
1952 में डॉ. आंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर उत्तरी बॉम्बे से चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने उनके खिलाफ एक ग्वाले, नारायण काजरोलकर, को उम्मीदवार बनाया। श्रीपाद अमृत डांगे के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने बाबासाहेब को अपमानित करने के लिए उन्हें ‘गद्दार’ करार दिया। डॉ. आंबेडकर लगभग 14,000 वोटों से चुनाव हार गए, जबकि 78,000 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया था। स्पष्ट है, चुनाव में धांधली हुई थी।
आंबेडकर की हार पर नेहरू ने खुशियां मनाईं। 16 जनवरी 1952 को उन्होंने अपनी करीबी दोस्त लेडी एडविना माउंटबेटन को लिखा, ‘बॉम्बे शहर में और खासकर, पूरे बॉम्बे प्रांत में हमारी कामयाबी उम्मीद से अधिक रही। आंबेडकर को हरा दिया गया है।’’ इससे पहले राजकुमारी अमृत कौर को लिखे पत्र (26 जनवरी, 1946) में नेहरू ने बाबासाहेब के प्रति अपनी दुर्भावना इन शब्दों में जाहिर की थी, ‘‘… मैं सबसे ज्यादा इस बात पर बल दे रहा था कि आंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार से गठजोड़ कर लिया है और वह कांग्रेस के खिलाफ हैं और हम उनसे कोई बातचीत नहीं कर सकते थे।’’
क्या विडंबना है कि आज वही कांग्रेस और नेहरू के परनाती भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए डॉ. आंबेडकर की विरासत से खुद को जोड़ने की पुरजोर कवायद में लगे हैं।
नेहरू का मुस्लिम प्रेम
नेहरू और डॉ. आंबेडकर, दोनों एक-दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे। नेहरू की मुसलमानों के प्रति आसक्ति इतनी गहरी थी कि उन्हें अन्य कमजोर वर्ग दिखाई ही नहीं देता था। बाबासाहेब को इस बात से चिढ़ थी। 10 अक्तूबर, 1951 को इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा था, ‘‘प्रधानमंत्री का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा को समर्पित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ मुसलमानों को ही सुरक्षा की जरूरत है? क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भारतीय ईसाइयों को सुरक्षा की जरूरत नहीं?’’
क्या राहुल की कांग्रेस बाबासाहेब की राजनीतिक विरासत को अपना सकती है? नेहरू की बाबासाहेब के प्रति नफरत जिस हद तक थी, उनकी नापसंदगी और आंबेडकर के नेहरू के प्रति अविश्वास को देखते हुए तो यह लगभग असंभव दिखता है। कांग्रेस एक ही समय में यह दावा नहीं कर सकती कि नेहरू और डॉ. आंबेडकर, दोनों उसके अस्तित्व का हिस्सा हैं। हो सकता है कि पार्टी मानती हो कि लोगों की याददाश्त कमजोर होती है और वे सब भूल चुके होंगे। कांग्रेस का यह नाटक कब तक चलेगा? इसका जवाब सिर्फ समय के पास है।
हालांकि, बाबासाहेब के गांधी जी के साथ भी मतभेद थे। कभी-कभी मतभेद बहुत कड़वे भी हो जाते थे। फिर भी, दोनों एक ही राह के पथिक थे, क्योंकि उनका एजेंडा कुछ हद तक एक जैसा था।
गांधी जी का मुख्य लक्ष्य था भारत को ब्रिटिश पराधीनता से मुक्त कराना और लाखों लोगों की सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक स्वाधीनता की दिशा में काम करना। जातियों में बंटी हिंदू सामाजिक व्यवस्था में छुआछूत जैसी पिछड़ी सामाजिक प्रथाओं की व्यथा झेलने वालों को गांधी जी ने हरिजन (ईश्वर की संतान) नाम दिया। यह विषय उनके लिए बेहद संवेदनशील था। एक दलित के रूप में जन्मे बाबासाहेब ने दलित होने के दर्द और अपमान को खुद झेला था। इसलिए अस्पृश्यता का अंत और अपने समुदाय के लोगों की स्थिति को सुधारने की दिशा में काम करना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। दोनों नेताओं का लक्ष्य एक ही था, बस उनके तरीके अलग-अलग थे। जब अंग्रेजों ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान करते हुए एक विभाजनकारी सांप्रदायिक प्रस्ताव पेश किया, तब दोनों के बीच मतभेद बढ़ गया था, क्योंकि बाबासाहेब ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। उनका मानना था कि इससे दलितों के हितों की पूर्ति की दिशा में सकारात्मक बदलाव होंगे।
1933 में महात्मा गांधी ने डॉ. आंबेडकर से अपनी पत्रिका ‘हरिजन’ के लिए एक संदेश लिखने को कहा। आंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर तीखा हमला करते हुए लिखा, ‘‘जाति-बहिष्कृत लोग जातीय व्यवस्था का ही एक परिणाम है। जब तक जातियां रहेंगी, तब तक जाति-बहिष्कृत लोग भी रहेंगे। बहिष्कृत लोगों की मुक्ति जाति व्यवस्था की समाप्ति के बिना नहीं हो सकती। आने वाले संघर्ष में हिंदुओं का अस्तित्व तभी बच सकता है, जब इस घृणित और क्रूर रूढ़िवाद से हिंदू धर्म को मुक्त किया जाए।’’
बाबासाहेब तब किस ‘आने वाले संघर्ष’ की ओर संकेत कर रहे थे? स्पष्ट रूप से उनका इशारा उस समय (1930 के बाद) बढ़ रहे हिंदू-मुस्लिम तनाव की ओर था, जो अंतत: एक रक्तरंजित विभाजन के बाद अलग इस्लामिक देश पाकिस्तान के निर्माण में तब्दील हुआ, जिसमें हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के लिए कोई स्थान नहीं था। बाबासाहेब में देश के क्षितिज पर मंडरा रहे विनाश को पहले ही भांप लेने की राजनीतिक सूझ-बूझ थी। दुख की बात है कि नेहरू सहित उस समय के ज्यादातर नेताओं में ऐसी समझ की भारी कमी थी।
आंबेडकर और हिंदुत्व : स्वाभाविक नाता
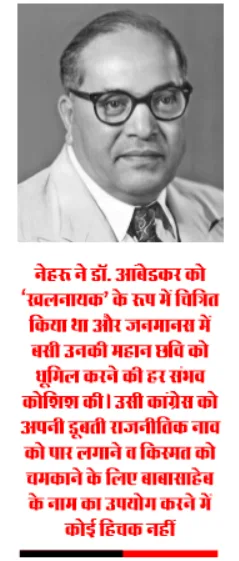 डॉ. आंबेडकर और हिंदुत्व आंदोलन के बीच एक स्वाभाविक नाता है। बाबासाहेब ‘हिंदुुत्व’ शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले चंद लोगों में से एक थे। 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान से जुड़े एक सेमिनार में एक अध्ययन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, ‘‘सांस्कृतिक एकता ही समरूपता का आधार है। इसे मानते हुए मैं निर्भीकता से कहता हूं कि ऐसा कोई देश नहीं, जो अपनी सांस्कृतिक एकता के संबंध में भारतीय उपमहाद्वीप की बराबरी कर सके। यहां न केवल भौगोलिक अखंडता है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण और आधारभूत एकता है- एक निर्विवाद सांस्कृतिक एकता, जिससे पूरा देश एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़ा है।’’
डॉ. आंबेडकर और हिंदुत्व आंदोलन के बीच एक स्वाभाविक नाता है। बाबासाहेब ‘हिंदुुत्व’ शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले चंद लोगों में से एक थे। 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान से जुड़े एक सेमिनार में एक अध्ययन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, ‘‘सांस्कृतिक एकता ही समरूपता का आधार है। इसे मानते हुए मैं निर्भीकता से कहता हूं कि ऐसा कोई देश नहीं, जो अपनी सांस्कृतिक एकता के संबंध में भारतीय उपमहाद्वीप की बराबरी कर सके। यहां न केवल भौगोलिक अखंडता है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण और आधारभूत एकता है- एक निर्विवाद सांस्कृतिक एकता, जिससे पूरा देश एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़ा है।’’
मंदिर में प्रवेश के मुद्दे पर 1927 में जारी एक बयान में बाबासाहेब ने कहा था, ‘‘हम जिस महत्वपूर्ण बात पर जोर देना चाहते हैं, वह यह नहीं है कि आपको भगवान की पूजा करने से संतुष्टि मिलती है…हिंदुत्व उतना ही अछूत हिंदुओं का है, जितना बाकी हिंदुओं का। हिंदुत्व के विकास और गौरव में वाल्मीकि, व्याध गीता के संत, संत चोखामेला और संत रैदास आदि ने उतना ही योगदान दिया, जितना महर्षि वशिष्ठ जैसे ब्राह्मणों, कृष्ण जैसे क्षत्रियों, हर्ष जैसे वैश्यों और तुकाराम जैसे शूद्रों ने। हिंदुओं की रक्षा के लिए शिदनाक महार जैसे अनगिनत वीरों ने लड़ाई लड़ी। हिंदुत्व के नाम पर बनाया गया मंदिर, जो धीरे-धीरे विकसित और समृद्ध हुआ, उसमें अस्पृश्य सहित सभी हिंदुओं का बलिदान शामिल है। इसलिए ऐसा मंदिर सभी हिंदुओं के लिए खुला रहना चाहिए चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। (बहिष्कृत भारत, 27 नवंबर 1927; धनंजय कीर लिखित ‘डॉ आंबेडकर : लाइफ एंड मिशन’, 1954 से उद्धूत)
बाबासाहेब और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
बाबासाहेब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े थे। रा.स्व.संघ अभिलेखागार के अनुसार 1939 में उन्हें पुणे के एक प्रशिक्षण शिविर में औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया था, जहां उनकी भेंट डॉ. हेडगेवार से हुई थी। वे यह देख कर खुश हुए कि शिविर में 500 लोग थे, जिनके बीच कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। 1949 में रा.स्व.संघ के सरसंघचालक श्री गुरुजी ने गांधी जी की हत्या के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा संघ पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने में सहायता करने पर आभार व्यक्त करने के लिए दिल्ली में बाबासाहेब से मुलाकात की थी। बाद में बड़े विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी (तब रा.स्व.संघ के युवा प्रचारक थे) ने 1954 के उपचुनावों में बाबासाहेब के मतदान एजेंट के रूप में काम किया था। उन्होंने बाबासाहेब के साथ बातचीत और अनुभवों को अपनी पुस्तक ‘डॉ. आंबेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा’ में लिखा।
बाबासाहेब का सम्मान
 भारतीय राजनीति की हिंदुत्व विचारधारा और बाबासाहेब के विचारों में बहुत समानता है। इसलिए भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने बाबासाहेब की स्मृति के साथ हुए अन्याय का अंत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने उनके जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों को ‘पंच तीर्थ’ के नाम से विकसित करने की योजना तैयार की है, जिसमें मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्मस्थान, लंदन स्थित उनका निवास, मुंबई स्थित बाबासाहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्मारक और चैत्य भूमि का विकास शामिल है।
भारतीय राजनीति की हिंदुत्व विचारधारा और बाबासाहेब के विचारों में बहुत समानता है। इसलिए भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने बाबासाहेब की स्मृति के साथ हुए अन्याय का अंत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने उनके जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों को ‘पंच तीर्थ’ के नाम से विकसित करने की योजना तैयार की है, जिसमें मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्मस्थान, लंदन स्थित उनका निवास, मुंबई स्थित बाबासाहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्मारक और चैत्य भूमि का विकास शामिल है।
मुंबई में डॉ. आंबेडकर की 430 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है, जो 25-30 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देगी। अलीपुर रोड पर बंगला नंबर 26 को एक प्रतिष्ठित स्मारक में बदला जा रहा है, जहां बाबासाहेब ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। उनकी स्मृति को अमर बनाने के लिए कांग्रेस यह सब क्यों नहीं कर पाई जो भाजपा कर रही है? क्योंकि कांग्रेस बाबासाहेब से और उनके सामाजिक समानता और सद्भाव के संदेश से घृणा करती रही है।
हिंदू धर्म से अन्य मतों में होने वाले कन्वर्जन के मुद्दे पर डॉ. आंबेडकर और हिंदुत्व नेताओं के विचार एक थे। अपनी चिंता जताते हुए उन्होंने कहा था, ‘‘कन्वर्जन के परिणाम पूरे देश पर क्या होंगे, इस पर ध्यान देना होगा। इस्लाम या ईसाई अपनाने से दलित वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना कमजोर पड़ने लगेगी। अगर वे इस्लाम अपनाते हैं तो मुसलमानों की संख्या दोगुनी हो जाएगी और मुस्लिम वर्चस्व का खतरा मंडराने लगेगा। वहीं, अगर वे ईसाइयत अपनाते हैं तो ईसाइयों की संख्या पांच से छह करोड़ हो जाएगी।’’ (टाइम्स आॅफ इंडिया, 24 जुलाई, 1936)
अराजकता का व्याकरण
बड़े हिंदू नेताओं की तरह बाबासाहेब साम्यवाद और उसके तौर-तरीकों को लोकतंत्र और बहुलवाद के लिए खतरा मानते थे। 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में उन्होंने कहा था, ‘‘हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को पाने के लिए संवैधानिक तरीकों को अपनाना चाहिए। जब ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई संवैधानिक साधन नहीं था, तब असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करना कुछ हद तक औचित्यपूर्ण कहा जा सकता था। लेकिन अब जबकि हमारे सामने संवैधानिक तरीके हैं, तो इन असंवैधानिक साधनों का कोई औचित्य नहीं। ये तरीके अराजकता के कारक हैं और कुछ नहीं। अत: जितनी जल्दी इनका त्याग किया जाए, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा।’’
अपनी रचना ‘बुद्ध आर कार्ल मार्क्स’ में डॉ. आंबेडकर लिखते हैं, ‘‘कम्युनिस्ट कहते हैं कि साम्यवाद स्थापित करने के केवल दो तरीके हैं। पहला है हिंसा; मौजूदा व्यवस्था को तोड़ने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं। दूसरा है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही; नई व्यवस्था को जारी रखने के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं।’’
इस्लाम पर बाबासाहेब के विचार
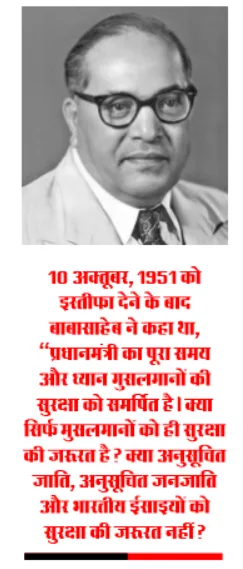 अपने निधन से 53 दिन पहले 14 अक्तूबर, 1956 को बाबासाहेब ने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध मत अपना लिया था। लेकिन हिंदू संस्कृति का त्याग नहीं किया। वे जानते थे कि अब्राहमिक मत एकेश्वरवादी रिवाजों से बंधे थे और सजातीय सामाजिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते थे। तीनों अब्राहमिक मतों में उन्हें इस्लाम से सबसे अधिक नफरत थी। शायद इस्लाम से जुड़े उनके व्यक्तिगत अनुभवों ने उन्हें इसका कटु आलोचक बना दिया था।
अपने निधन से 53 दिन पहले 14 अक्तूबर, 1956 को बाबासाहेब ने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध मत अपना लिया था। लेकिन हिंदू संस्कृति का त्याग नहीं किया। वे जानते थे कि अब्राहमिक मत एकेश्वरवादी रिवाजों से बंधे थे और सजातीय सामाजिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते थे। तीनों अब्राहमिक मतों में उन्हें इस्लाम से सबसे अधिक नफरत थी। शायद इस्लाम से जुड़े उनके व्यक्तिगत अनुभवों ने उन्हें इसका कटु आलोचक बना दिया था।
1934 में जब वे अपने साथियों के साथ अजंता की बौद्ध गुफाएं देखने गए, तो उस दौरान वे संभाजीनगर में दौलताबाद किला भी देखना चाहते थे। ‘वेटिंग फॉर वीजा’ नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है, ‘‘रमजान का महीना था। मुसलमानों के लिए उपवास का महीना। किले के दरवाजे के ठीक बाहर एक छोटा-सा तालाब है, जो लबालब भरा हुआ है। चौड़े पत्थर का फर्श है। यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर और कपड़े धूल से सन गए थे और हम सब नहाना चाहते थे। इसी बीच, लहराती सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा मुसलमान पीछे से चिल्लाता हुआ आया, ‘‘ढेडों (अछूतों) ने तालाब को गंदा कर दिया है!’ देखते-देखते आस-पास के युवा और बूढ़े मुसलमान भी वहां इकट्ठा हो गए और सब हमें बुरा-भला कहने लगे। आंबेडकर कहते हैं, ‘‘जो व्यक्ति हिंदू के लिए अछूत है, वह मुसलमान के लिए भी अछूत है।’’
इसी तरह, ‘पाकिस्तान आर द पार्टीशन आफ इंडिया’ में उन्होंने इस्लाम और पाकिस्तान का विश्लेषण किया है। वह लिखते हैं, ‘‘हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता है कि यह लोगों को विभाजित करता है, वहीं इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि यह लोगों को एक सूत्र में जोड़ता है। यह केवल आधा सच है, क्योंकि इस्लाम जितनी मजबूती से जोड़ता है, उतनी ही मजबूती से विभाजित भी करता है। इस्लाम एक घेराबंद समूह है और यह मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के बीच जो अंतर स्थापित करता है वह बहुत वास्तविक, बहुत कट्टर और बहुत ही अलगावकारी है। इस्लाम का भाईचारा मानव समुदाय का सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है। यह मुसलमानों का और केवल मुसलमानों के लिए बनाया गया भाईचारा है। भाईचारे की इस भावना का लाभ उस समूह के भीतर के लोगों तक ही सीमित है। जो लोग इसके बाहर हैं, उनके लिए मन में घृणा और शत्रुता की भावना के अलावा कुछ नहीं।
इस्लाम कभी भी एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में अपनाने और एक हिंदू को अपना सगा-संबंधी मानने की अनुमति नहीं देता।’’ अपने देश के प्रति मुसलमानों की वफादारी बनाम इस्लाम के प्रति उनकी वफादारी पर बात करते हुए बाबासाहेब ने लिखा है, ‘‘इस्लाम कहता है कि एक देश जो मुस्लिम शासन के अधीन नहीं, वहां जब भी मुस्लिम कानून और देश के कानून के बीच टकराव होगा, तब देश के कानून पर मुस्लिम कानून को ही वरीयता देनी होगी। एक मुसलमान तभी सच्चा माना जाएगा, जब वह देश के कानून की अवहेलना करके मुस्लिम कानून का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हो। मुसलमान चाहे नागरिक हो या सैनिक, चाहे मुस्लिम या गैर-मुस्लिम प्रशासन के अधीन हो, उसे कुरान के आदेश के तहत अपनी निष्ठा सिर्फ अल्लाह, उसके पैगंबर के प्रति और सत्ता में बैठे लोगों में सिर्फ मुसलमानों के प्रति ही निभानी होगी।’’
डॉ. आंबेडकर ने यह समझने के लिए इस्लामी सिद्धांतों का अध्ययन किया कि मुसलमानों को उनकी मान्यताओं के अनुसार किसी देश में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक होने पर कैसा व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है। उनका निष्कर्ष था, ‘‘मुस्लिम कानून के अनुसार दुनिया दो खेमों में विभाजित है, दार-उल-इस्लाम (इस्लाम का घर) और दार-उल-हर्ब (युद्ध का घर)। कोई देश दार-उल-इस्लाम तब होता है, जब उस पर मुसलमानों का शासन होता है और दार-उल-हर्ब तब होता है, जहां मुसलमान केवल निवास करते हैं, वहां उनका शासन नहीं होता। मुस्लिम कानून के अनुसार, भारत हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक साझा मातृभूमि नहीं बन सकता। यह मुसलमानों की जमीन तो हो सकती है, लेकिन ‘हिंदुओं और मुसलमानों की समानता के साथ रहने’ की जमीन नहीं हो सकती। यह मुसलमानों की जमीन तभी कहलाएगी, जब इस पर मुसलमानों का शासन हो, जैसे ही कोई जमीन किसी गैर-मुस्लिम शासन के अधीन हो जाती है, वह मुसलमानों की भूमि नहीं रहती। यह दार-उल-इस्लाम बनने के बजाय, दार-उल-हर्ब बन जाती है।’’
केंद्र में हिंदू बहुमत वाली सरकार के प्रति मुसलमानों की प्रतिक्रिया को रेखांकित करते हुए बाबासाहेब ने कहा था, ‘‘मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है। काफिर सम्मान के लायक नहीं है। वह निम्न कुल का है और उसका कोई दर्जा नहीं है। इसलिए काफिर द्वारा शासित देश मुसलमानों के लिए दार-उल-हर्ब है। इसे देखते हुए, यह साबित करने के लिए कोई और सबूत देने की जरूरत नहीं कि मुसलमान हिंदू शासन का पालन नहीं करने वाले हैं। सम्मान और सहानुभूति की बुनियादी भावनाएं, जो लोगों को किसी शासन के अधीन काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, वह इनके अंदर मौजूद नहीं हैं। फिर भी सबूत चाहिए तो इसकी कोई कमी नहीं है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि क्या पेश किया जाए और क्या छोड़ा जाए, कहना मुश्किल है। खिलाफत आंदोलन के दौरान जब हिंदू हर तरह से मुसलमानों की मदद कर रहे थे, तब भी मुसलमान यह नहीं भूल पाए कि उनकी तुलना में हिंदू एक नीच और हीन जाति है।’’
सावरकर और बाबासाहेब
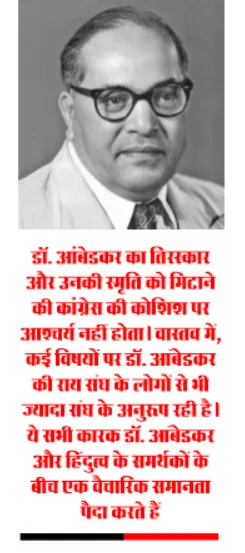 ‘एनीहिलेशन आफ कास्ट’ (Annihilation of Caste) में बाबासाहेब ने मजबूत हिंदू धर्म-मजबूत भारत के अपने दृष्टिकोण को साझा किया है। उनका मानना था कि हिंदुओं का विभिन्न जातियों में बंटे रहना उनके सपने को साकार करने की राह की सबसे बड़ी बाधा है। वे कहते थे, ‘‘जब तक जाति रहेगी, तब तक संगठन नहीं बन सकता और जब तक संगठन नहीं बनता, हिंदू कमजोर और दब्बू रहेंगे। उदासीनता सबसे बुरा रोग है, जो लोगों को संक्रमित कर सकता है। आखिर हिंदू इतने उदासीन क्यों हैं? मेरी राय में यह उदासीनता जाति व्यवस्था का परिणाम है, जिसके कारण संगठन और अच्छे उद्देश्य के लिए भी सहयोग की भावना का जागना असंभव लगता है।’’
‘एनीहिलेशन आफ कास्ट’ (Annihilation of Caste) में बाबासाहेब ने मजबूत हिंदू धर्म-मजबूत भारत के अपने दृष्टिकोण को साझा किया है। उनका मानना था कि हिंदुओं का विभिन्न जातियों में बंटे रहना उनके सपने को साकार करने की राह की सबसे बड़ी बाधा है। वे कहते थे, ‘‘जब तक जाति रहेगी, तब तक संगठन नहीं बन सकता और जब तक संगठन नहीं बनता, हिंदू कमजोर और दब्बू रहेंगे। उदासीनता सबसे बुरा रोग है, जो लोगों को संक्रमित कर सकता है। आखिर हिंदू इतने उदासीन क्यों हैं? मेरी राय में यह उदासीनता जाति व्यवस्था का परिणाम है, जिसके कारण संगठन और अच्छे उद्देश्य के लिए भी सहयोग की भावना का जागना असंभव लगता है।’’
1930 में ‘एसेज आन द अबॉलीशन आफ कास्ट’ में वीर सावरकर ने भी इसी भावना को व्यक्त किया है। वे लिखते हैं, ‘‘हमारे लाखों सह-मतावलंबियों को ‘अछूत’ और पशुओं से भी बदतर मानना न केवल मानवता, बल्कि हमारी आत्मा की पवित्रता का भी अपमान है। अत: मैं दृढ़ता से मानता हूं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी में हमारे हिंदू समाज का हित निहित है। अगर थोड़ी देर के लिए माना जाए कि इस प्रथा से हिंदू समाज को कुछ अच्छा मिल रहा है, तब भी मेरा विरोध इतना ही कड़ा होता। जब मैं किसी को छूने से मना करता हूं, क्योंकि वह किसी खास समुदाय में पैदा हुआ है और दूसरी तरफ बिल्लियों और कुत्तों के साथ खेलता हूं, तो मैं मानवता के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध कर रहा हूं। अस्पृश्यता का उन्मूलन केवल इसलिए नहीं कि यह हमारा कर्तव्य है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि जब धर्म के किसी भी आयाम पर हम विचार करेंगे, तब इस अमानवीय प्रथा को उचित ठहराने के लिए हमारे पास कोई भी न्यायसंगत तर्क नहीं होगा।’’
विदेश नीति पर अलग राय
8 नवंबर, 1951 को लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की सभा को संबोधित करते हुए बाबासाहेब ने कहा था, ‘‘सरकार की विदेश नीति भारत को मजबूत बनाने में विफल रही है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? प्रधानमंत्री ने इसके लिए प्रयास क्यों नहीं किया? भारत को संसदीय लोकतंत्र और तानाशाही के साम्यवादी तरीके के बीच किसी एक को चुनना होगा और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना होगा।’’ तिब्बत और चीन के मामले में उनकी राय नेहरू से अलग थी, ‘‘अगर माओ को पंचशील में कोई आस्था होती, तो वह निश्चित रूप से अपने देश में बौद्धों के साथ अलग तरीके से पेश आते। राजनीति में पंचशील के लिए कोई जगह नहीं।’’
भाजपा (पहले भारतीय जनसंघ) की तरह बाबासाहेब भी नेहरू की चीन समर्थक नीति और तिब्बत मुद्दे पर उनकी हिचक को सही नहीं मानते थे। दोनों ही अस्पृश्यता के उन्मूलन और दलितों की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध रहे। दोनों ने ही कट्टरपंथी इस्लाम को गलत ठहराया तथा भारत और लोकतंत्र के विचार के प्रति साम्यवादियों की प्रतिबद्धता पर कभी विश्वास नहीं किया। वहीं, कांग्रेस का दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास दर्शाता है कि वह जिहादी मानसिकता के राजनीतिक चेहरे ‘वामपंथी और मुस्लिम लीग’, दोनों के साथ सहयोग करती रही।
डॉ. आंबेडकर का तिरस्कार और उनकी स्मृति को मिटाने की कांग्रेस की कोशिश पर आश्चर्य नहीं होता। वास्तव में, कई विषयों पर (पाकिस्तान, इस्लाम और आदिवासियों की स्थिति) डॉ. आंबेडकर की राय संघ के लोगों से भी ज्यादा संघ के अनुरूप रही है। ये सभी कारक डॉ. आंबेडकर और हिंदुत्व के समर्थकों के बीच एक वैचारिक समानता पैदा करते हैं। नेहरू ने डॉ. आंबेडकर को बाहर रखा। कांग्रेस उन्हें नजरअंदाज करके जनता के मन से उनकी स्मृति को मिटाने में लगी रही। लेकिन आज, उनकी मृत्यु के 68 साल बाद डॉ. आंबेडकर के महान व्यक्तित्व का प्रभाव भारतीय संसद की कार्यवाही पर छाया हुआ है। कल तक जिन लोगों ने डॉ. आंबेडकर का मजाक उड़ाया, उन्हें ‘देशद्रोही’ कहा और धांधली करके लोकसभा चुनाव में पराजित किया, आज वही उनके नाम और उनके विचारों की कसमें खाने के लिए विवश हैं।



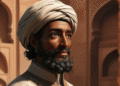

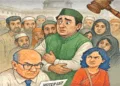











टिप्पणियाँ