प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति एवं प्रकृति के बीच अंतर्संबंध रहा है। उसी के अनुरूप भारतीय संस्कृति एवं जल के बीच आत्मीय संबंध स्थापित हुआ। भौगोलिक-सांस्कृतिक भिन्नता की तरह यहां जल संस्कृति में भी विविधता रही। अनंतकाल से भारतीय परंपराओं, पुरातात्विक अवशेषों यथा-अभिलेखों, शिलालेखों, भवनों, कलाकृतियों एवं अनेक प्राचीन ग्रंथों में जल प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे पुरातन पारंपरिक जलीय ढांचे देखने को मिलते हैं। ये केवल जल की व्यवस्था के संसाधन नहीं थे, अपितु उनके जीवन के आधार केंद्र भी थे, जिनके इर्द-गिर्द उनकी समस्त सामाजिक-सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती थीं। ठीक इसी प्रकार जलीय संस्कृति न्यूनाधिक रूप में आज भी कायम है। इस जल संस्कृति को हम अपने दैनिक व्यवहार से लेकर उत्सव-त्योहारों एवं समग्र लोक संस्कृति में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
थार मरुस्थल से लेकर दोआब के क्षेत्र में जल की समुचित व्यवस्था कैसे बनी रहे? इन सबके लिए हमारे पुरखों ने ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी थी कि जिससे जल के साथ भावनात्मक संबंध बना रहे। इस भावनात्मक संबंध का परिणाम यह रहा कि सदियों तक जलाशयों में जल की निर्बाध उपलब्धता बनी रही। जल संस्कृति अर्थात् जल से संबद्ध मानवीय जीवन की वह प्रक्रिया, जिसमें जल चक्र वर्षा विज्ञान जल व जलीय संसाधनों के भिन्न-भिन्न रूप, जल संग्रहण के पारंपरिक तौर-तरीके, जलाशयों की साफ-सफाई, जल की निर्बाध उपलब्धता एवं पारंपरिक समाज के अनुभव का महती वर्णन लोककथाओं, लोकगीतों, लोकोक्तियों, मुहावरों, पहेलियों आदि लोक-साहित्य में मिलता है।
जल संस्कृति की महती उपयोगिता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि भारतीय संस्कृति के पुरातन ग्रंथ वेदों में जल को देवता का स्थान दिया गया, उसी अनुरूप छांदोग्य उपनिषद में विवेचन मिलता है, ‘‘नदियों का जल सागर में मिलता है। वे सागर से सागर को जोड़ती हैं, मेघ वाष्प बनकर आकाश में छाते हैं और बरसात करते हैं…’’(बूंदों की संस्कृति, पृ. 13)। जल चक्र जैसा विवरण वैदिक साहित्य में मिलता है, उसी तरह लोक साहित्य में भी मिलता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में उक्त जल चक्र को एक नुकती दाना में इस प्रकार व्यक्त किया गया है, ‘‘सूरज नीची बिरती आलै पाणी ने आपके तेज सयूँ आसमान में चढ़ा देवै तो वो घमण्ड सयूँ गाजण लाग जावै। वीं को फल यो होवे क वो पाछो ही नीचे आ पड़ै।’’ अर्थात् सूरज के ताप से जल वाष्प बनकर बादल के रूप में इकट्ठा होकर जब वह गरजता है तो वह वर्षा के रूप में पुन: पृथ्वी पर आ जाता है। लोकव्यवहार और लोकसाहित्य में जल चक्र अलग रूपों में भी दृष्टिगत होता है।
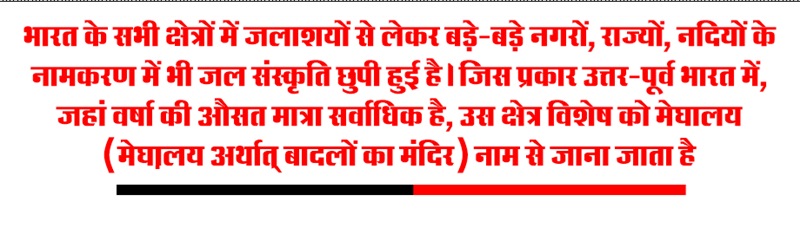 लोकजीवन में वर्षा का महत्व
लोकजीवन में वर्षा का महत्व
वर्षा को कृषि प्रधान समाज ने सदैव देव स्वरूप मानकर उसका स्वागत किया। ग्रामवासी आने वाली वर्षा के स्वागत एवं उसके नितांत अभाव के कारण होने वाले कष्टों की चर्चा बारह महीने करते रहते हंै। लोक जीवन के समस्त विश्वास वर्षा के इर्द-गिर्द ही घूमते हैं। यह लोक-विश्वास न्यून-अधिक भिन्नता के साथ संपूर्ण भारत में देखने-सुनने को मिलता है। स्थानीय पशु-पक्षियों के हाव-भाव, वायु, सूर्य, चंद्रमा एवं बादलों के बदलते हुए रंग-रूप से वर्षा का पूर्वानुमान लगाया जाता था। मौसम ज्ञान से जुड़ी घाघ की कहावतें उत्तर प्रदेश व बिहार में तथा भड्डरी की पंजाब और राजस्थान में आज भी प्रचलित हैं। वर्षा के विशेषज्ञ पशु-पक्षियों, कीट-पतंगों की संवेदनशीलता से भी मौसम का अनुमान लगा लेते थे। तमिलनाडु के तिरुनेलवेल्ली में माना जाता है कि घोंघे यदि विशिष्ट वृक्षों पर चढ़ना शुरू कर दें, तो वर्षा नहीं होगी। कन्याकुमारी में कौए और मुर्गे यदि पंख फैलाकर फुदकना शुरू कर दें तो जोरों की वर्षा होगी। ऐसी ही अनेक कहावतें उत्तर एवं उतर-पश्चिम भारत में भी मिलती हैं, यथा –
चींटी ले अंडा चले चिड़ी नहावे धूर।
ऐसा बोले भड्डरी वर्षा हो भरपूर ।।
भावार्थ- यदि चींटी अपने अंडे लेकर स्थान परिवर्तन करे और यदि चिड़िया चोंच या पंखों से धूल में खेलती दिखें तो मानना चाहिए कि भरपूर वर्षा होने वाली है। इसी प्रकार अनुमान लगाया जाता था कि जब हवा पूरब की हो तो वर्षा अवश्यंभावी है और विपरीत स्थिति में वर्षा नहीं ही होगी। तभी कहा है कि-
पूरब के बादर पश्चिम जाय, पतरी पकावै मोटी खाय,
पकुंवा बादर पूरब के जाय, मोटी पकौव पतरी खाय।।
वर्षा आगमन की सूचना बड़े वैज्ञानिक ढंग से दी जाती है कि ज्येष्ठ मास में जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी ही वर्षा अधिक होगी। स्पष्ट है कि गर्मी का चरम ज्येष्ठ माह में वाष्पीकरण लाकर वर्षा लाता है। इसी प्रकार ज्येष्ठ महीने के नौ दिन मरुस्थल में नौतपा उत्सव के रूप मनाए जाते हैं। यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुरू होते हैं। नौ दिन की यह तपन ओघमौ कहलाती है, जिसके बाद आषाढ़ में बादल आने शुरू हो जाते हैं। इसी खुशी में किसान-चरवाहे स्वागत गीत गाते हैं-
जेठ महीनौ भलां आयौ, दक्खण बाजैबा
उणां कानारै तौ कांकड़ बाजै, वां रे सांईवा
इण बाबत ऐक कहावत ई कैईजै –
जेठ मास जो तपै निरासा, तौ जाणौ बिरखा री आसा
वर्षा के देव इंद्र को प्रसन्न करने के लिए जगह-जगह अनेक हवन-यज्ञ किए जाते हैं। ईस्वी सन् के आरंभकाल में कावेरीपूमपत्तनम् में वर्षा के आगमन के लिए इंद्र-पर्व मनाया जाता था (तमिलनाडु लोक संस्कृति और साहित्य, पृ. 33)। इसी प्रकार के आयोजन मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में भी मनाए जाते हैं। वर्षा से पूर्व यह हवन कोई मिथक नहीं बल्कि वैज्ञानिक है क्योंकि तिल, चावल और जौ के धुंए से बादल बनते हैं। जो पर्जन्य हैं एवं फव्वारे के रूप में अवश्य बरसते भी हैं। पर्जन्य बादलों में जल धीरे-धीरे संचित होता है। हवन के आयोजन से संबंधित जानकारी अभिलेखागारीय स्रोतों से भी मिलती है।
कृषि प्रधान देश का कृषक अच्छी फसल के लिए गीत गाकर वर्षा को रिझाता है। इसी से संबंधित दक्षिण भारत में पझियारों द्वारा गाया जाने वाला वर्षा-स्तोत्र है-
कुडि कुम्मारनुकु सीक्कु संकटम् वरम्
एंकलैक, कोण्डु पोरुत्तुक पेय्यानम्,
नल्ल मड़े पेय्यानम्मन्न पोट्टप पोन्न विलयानम्।
भावार्थ है कि सूखे के कारण होने वाले रोगों से आदमी या मवेशी, किसी को दुख न पहुंचे। हे इंद्र! हमारी रक्षा करो। भारी वर्षा बरसाकर और प्रचुर फसल उगा कर, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दो।

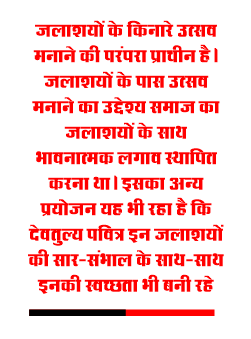 वर्षा के एक बार होने पर जब फिर से कुछ दिन वर्षा नहीं होती थी तो किसान घनी फसलों के सूखने पर चिंतित हो वर्षा को पुकारते हुए इंद्र देव से प्रार्थना करने लगते हैं-
वर्षा के एक बार होने पर जब फिर से कुछ दिन वर्षा नहीं होती थी तो किसान घनी फसलों के सूखने पर चिंतित हो वर्षा को पुकारते हुए इंद्र देव से प्रार्थना करने लगते हैं-
वाकै मरतुप पुंजै, वट्टारक चोलप पुंजै
तंगम् वैलइयम् पुंजै, तरिसक किडक्कुताडि
कट्टै उड़तु पोट्टेन, कदलै पोडप पाठम् पारत्तेन
वन्त मडै पोकुतिल्ल, वरुणने उनातु सेयल
भावार्थ है कि वृक्षों के पास की सूखी जमीन, और उसके पड़ोस की ‘रागी’ भूमि, जो हमेशा घनी फसल देती हैं, आज बिना जोती हुई पड़ी हैं। एक बार हल भी चलाया था। मूंगफली बोने से पहले, मिट्टी की परीक्षा भी करवायी थी। कुछ बूंदाबांदी हुई थी, पर बरखा फिर गायब हो गयी।
इंद्र देवता! यह तुम्हारा कैसा खिलवाड़ है। (तमिलनाडु का लोक संस्कृति और साहित्य, पृ. 35,36)
इसी प्रकार लोक संस्कृति में वर्षा के बारह महीनों के अनुसार भिन्न-भिन्न नाम मिलते हैं। राजस्थानी भाषा में मासानुसार वर्षा के नाम इस प्रकार हैं, यथा- चैत्र-चड़पड़ाट, बैसाख-हलोतियो, ज्येष्ठ-झपटो, आषाढ़-सरवांत, श्रावण-लोर, भादवा-झड़ी, आसोज-मोती, कार्तिक-कटक, मार्गशीर्ष-फांसरड़ो, पौष-पावठ, माघ-मावठ, फाल्गुण-फटकार। इसी प्रकार से जो वर्षा फसल के लिए महत्वपूर्ण होती थी, उसका नामकरण एवं प्रतिमान भी वैसा ही हो जाता था। इसी संदर्भ में उत्तरी कर्नाटक में ‘उत्तराषाढ़ की वर्षा’ नामक कन्नड़ लोककथा प्रसिद्ध है। यह लोककथा आषाढ़ के महिने की वर्षा के इंतजार को व्यक्त करती है कि भला कौन है, जो उत्तराषाढ़ की वर्षा की राह नहीं देखता (कन्नड़ लोककथाएं, पृ. 88)।
विभिन्न सभ्यताओं के उत्थान के केंद्र रहे प्राकृतिक जल स्रोत, विश्व के महत्वपूर्ण नगरों की बसावट के भी आधार रहे हैं। भारत में भौगोलिक विषमताएं हैं, जहां एक ओर नदी- समुंदर के किनारे बसे क्षेत्र हैं, तो दूसरी ओर थार मरुस्थल। इन विषमताओं के होने पर जिन स्थानों पर प्राकृतिक रूप से जलीय स्रोत नहीं थे, वहां कृत्रिम जलाशय निर्मित किए गए। जलाशय निर्माण को पुण्यकार्य बताया गया है। धर्मसूत्रों में भी जोर दिया गया है कि राजा एवं प्रजा को तालाब-कुएं बनवाने चाहिए। इसके फलस्वरूप राज एवं समाज ने अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी अच्छे कार्य की स्मृति, किसी व्यक्ति विशेष की स्मृति या किसी संकल्प के फलस्वरूप मिलकर अथवा निजी तौर पर इनका निर्माण करवाया। जलाशय बनाने के उद्देश्य जलाशयों के किनारे स्थित शिलालेखों में अंकित मिलते हैं। जलाशय निर्मित कराने वालों को समाज मे सम्मानित दृष्टि से देखा जाता था। इससे जुड़ा एक राजस्थानी लोकगीत पनिहारी है- कुण जी खुदाया कुवा बावड़ी…
अर्थात् इस कुएं और बावड़ी को किसने बनवाया और तालाब को किसने बंधाया है? इस गीत में उस जलाशय को निर्मित कराने वाले के साथ उसके घर के सभी सदस्यों का नाम लेकर गीत के बोल बढ़ते जाते हैं। राजस्थानी लोकगीत की तरह ही इसी भाव के साथ जलाशयों का भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न नाम लेते हुए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार के गीत गाये जाते हैं। जलाशयों से पानी भरने को भी भारतीय समाज ने एक उत्सव की भांति समझा। इसी अनुरूप भारत के सभी क्षेत्रों में पणिहारी नामक लोकगीत गाए जाते थे। इसी संदर्भ में गुजरात में ‘एक वनजारी झीलण झीलती ती’ नामक विख्यात पणिहारी लोकगीत है।
लंबी दूरी तय कर जलाशय से पानी लेने आते-जाते समय गाए जाने वाले गीत न केवल सिर और हाथों में लिए मटकों के वजन के साथ रास्ते को नीरस नहीं होने देते थे, उसी प्रकार से ये गीत तत्कालीन समाज में महिलाओं के सुख-दु:ख बांटने के साधन भी थे। देश के प्रत्येक क्षेत्र में जल की व्यवस्था कराने वाले जल योद्धाओं की गाथाएं गाई और सुनाई जाती हैं। इसी से जुड़ी एक लोकगाथा कुल्ह हिमाचल के कांगड़ा तथा चंबा में प्रचलित है जिसमें कुल्ह अर्थात् नहर खुदवाने और उसमें पानी होने के लिए राजपरिवारों द्वारा दिए गए बलिदान की कहानी है।
 हम्पी (कर्नाटक) साम्राज्य में जल प्रबंधन
हम्पी (कर्नाटक) साम्राज्य में जल प्रबंधन
जो यहां डूमणों द्वारा घर-घर जाकर सुनाई जाती है। (सुदर्शन वशिष्ठ, हिमाचली लोककथाएं, पृ. 114) इसी प्रकार की लोकगाथाएं बुंदेलखंड में हरबोलों एवं राजस्थान में भाट व चारणों द्वारा सुनाई जाती रही है। इसी प्रकार से असम में तुई चोंग नदी की लोकगाथा जन-जन में प्रचलित है। (एस.एन. बरकताकी, ट्राइबल फोकटेल्स आफ असम, पृ. 40) जल से जुड़ी ये प्रेरक कहानियां जल से समाज का आत्मीयता भाव स्थापित करने में सक्षम रहती थी।
जलाशयों से निर्बाध जल की प्राप्ति हो सके इसके लिए सदैव से परंपरा चली आ रही है कि क्षेत्र विशेष में लोकप्रिय व्यक्तित्व या अपने इष्टदेव को जलाशयों के किनारे मंदिर में स्थापित किया जाता रहा है। भारत के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक यह परंपरा देखने को मिलती है। जिसका उद्देश्य जलाशय की सार-संभाल तो था ही साथ ही उसे अतिक्रमण से बचाने के लिए भी था। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में विनायक, शिव और विष्णु एवं देवियां, जिसमें गणेश जी के मंदिर जलाशयों के किनारे सर्वाधिक हैं। इसी प्रकार से उत्तर भारत में जम्मू के उधमपुर में बिलावर शुक्रला में सुध महादेव मंदिर की बावली में इस जलीय संरचना में कई देवी-देवताओं के चित्र बने हुए हैं परंतु नाग देवता के चित्र या मूर्ति यहां के जलाशयों में सामान्य रूप से देखने को मिलती है। (सोमनाथ धर, जम्मू एंड कश्मीर, पृ. 140)। जलाशयों की खुदाई से पूर्व नाग देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की जाती है। तालाब की खुदाई से पूर्व प्रियजन की सुरक्षा में गाया जाने वाला तमिल लोकगीत है-
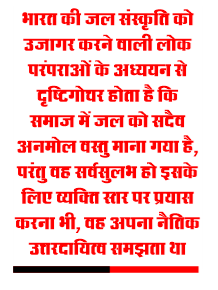 पुट व पुटून नागरे,भूमि इडम कोंडयरे
पुट व पुटून नागरे,भूमि इडम कोंडयरे
मनिप्पिरंबु पोला, वाल अलगु नागरे
सिरु सुलकु पोला, पदमेडुक्कुम नागरे
कुंडु मुतुप पोला, कन्नलागु नागरे
पचारिसि पोला, पल्ललाकु नागरे
पल्लर मकन पल्लन, देवेंद्र कुदुंबन्
कोटटु मन वेट्टि एड तु, कुलतार के पोनन
इरु पुरामुम ओडुक्कि, वाड़ि विडू वै नागरे
अर्थात् हे नागराज, बांबियों में रहने वाले धरती के गर्भ के निवासी तुम्हारी पूंछ बड़ी सुंदर है। मानो बेंत की लपलपाती हुई छड़ी तुम्हारा उभरा हुआ फन जैसे हवा झलने का पंखा तुम्हारी छोटी-छोटी आंखें जैसे आबदार मोती तुम्हारे पैने दांत मानो छड़े हुए चावल के दाने जन्मजात श्रमिक देवेंद्र कुदुंबन कांधे पर कुदाल धरे गया है तालाब पर, या बांध पर खुदाई करने के लिए उसकी रक्षा करना, स्वामी उसे कोई हानि मत पहुंचाना, अपने इस विशाल फण को नीचा ही रखिए और उस गरीब की राह निर्भय कीजिए हे नागस्वामी!
राजस्थान एवं हरियाणा के जलाशयों के किनारे हनुमान जी के थान मुख्यत मिलते हैं। पारंपरिक जल प्रणाली की बात करें तो संपूर्ण देश में एक समान है। जैसे, जम्मू में झरने के इर्द-गिर्द कुएं-बावली मिलती है तो थार मरुस्थल में कच्चे जोहड़ों के इर्द-गिर्द संपूर्ण गांव की जलीय संरचना मिलती है।
पंजाब-हरियाणा के गांव का जीवन जोहड़, तालाबों के आस-पास ही फलता-फूलता रहा है। जोहड़ (छप्पड़-ढाब) गांव के आस-पास ही बनाए जाते थे, ताकि जल के अतिरिक्त छप्पड़ों की मिट्टी का उपयोग किया जा सके। मिट्टी का उपयोग लीपने और कुम्हारी के काम में आता है। गर्मियों में जब छप्पड़ों का पानी उड़ने लगता है तो अन्य स्रोतों से इसे पुन: भर दिया जाता। परंतु अत्यधिक लू के मौसम में जब छप्पड़ फिर खाली होने लगते हैं तो पुन: वर्षा को पुकारने वाले गीत गाए जाते है। छप्पड़ों के किनारे चावलों की देंगे उतरी जाती हैं। छोटे-छोटे बच्चे गलियों में गीत गाते घूमते हैं-
रब्बा-रब्बा मींह बरसा, साडी कोठी दाने पा
कालियां इट्टां,काले रोड, मींह बरसा दे जोरों-जोर
छप्पड़ गांव की धड़कन होते हैं। प्राय: इन छप्पड़ों के पास ही माता के थान होते हैं। जहां बच्चों के चेचक निकलने के बाद माथे टिकाए जाते हैं। छप्पड़ों के चारों ओर घने पेड़ लगाए जाते हैं, जहां पाली अपने पशुओं को खुला छोड़ कुछ न कुछ खेल खेलते रहते। इन छप्पड़ों के आस पास ही नित्य-प्रति के कामों की गहमा-गहमी रहती। लुहार, कुम्हार, सुथार और मोची वगैरह तो जैसे छप्पड़ों का हिस्सा होते। खुशी-गमी की सब रस्में इन छप्पड़ों के किनारे मिट्टी निकाल कर पूरी की जाती, ताकि छप्पड़ और ढाबें और गहरी से गहरी होती जाएं और गांव का जीवन और दीर्घ होता जाए।
 पानी के लिए समाज आया सामने
पानी के लिए समाज आया सामने
जलाशयों के किनारे उत्सव मनाने की परंपरा प्राचीन है। जलाशयों के पास उत्सव मनाने का उद्देश्य समाज का जलाशयों के साथ भावनात्मक लगाव स्थापित करना था। इसका अन्य प्रयोजन यह भी रहा है कि देवतुल्य पवित्र इन जलाशयों की सार-संभाल के साथ-साथ इनकी स्वच्छता भी बनी रहे। प्राकृतिक जलाशयों के अभाव वाले क्षेत्रों में ये उत्सव कृत्रिम रूप से तालाब, बावड़ी, कुएं एवं कुंड के किनारे बनाए जाते थे। उदाहरणार्थ, राजस्थान में कजली तीज का उत्सव जोहरी सागर के किनारे मनाया जाता था, जिसमें ग्रामीणों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता था। इसी प्रकार से बिहार प्रांत में ‘छठ पर्व’ नदी के किनारे सूर्य को अर्घ्य देकर मनाया जाता है। दक्षिण भारत की बात करें तो वहां भी समुद्र की पूजा के साथ नदियों के किनारे बड़ी धूम-धाम से उत्सव मनाए जाते हैं।
इसी संदर्भ में तमिलनाडु में ‘पदिनेट्टम पेरूक्कु’ उत्सव अर्थात् ‘अठारहवीं की बाढ़’, जो तमिल मास की अठारहवीं तिथि (लगभग पहली अगस्त) को कावेरी नदी मुख दोआबों में रहने वाले लोगों द्वारा मनाया जाता है। तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में कावेरी का यह महोत्सव बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। जम्मू-कश्मीर की संस्कृति में नदियों का बहुत महत्व रहा है। कश्मीर में वितस्ता त्रयोदशी का त्योहार तवी नदी के किनारे ‘बाहू का मेला’ नाम से बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। (हेमंत कुकरेती, भारत की लोकसंस्कृति, प्रभात प्रकाशन)। गोवा में भी वर्षा ऋतु के आगमन के फलस्वरूप ‘सांजाव’ एवं ‘चिक्क्ल कालो’ उत्सव मनाए जाते है। ये दोनों उत्सव मानसून आगमन पर हर्षोल्लास की अभिव्यक्ति है। नदी, तालाब एवं कुवे जल से लबालब भर जाएंगे और इससे अच्छी फसल भी होगी।
इसी प्रकार से कांचीपुरम में मनाए जाने वाले ‘नाडवावि’ उत्सव में मद्रास नगर (वर्तमान में चैन्ने) के व्यापारी एवं अन्य बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। ‘नाडवावि’ नाडपवै का ही अपभ्रंश है। वावि का अर्थ कुआं होता है। इसे अप्रैल-मई में आने वाली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस उत्सव के पीछे एक लोककथा भी है कि कोडी कन्निकदानम ताता चारियर ने वरदराज पेरुमल का मंदिर बनवाने के लिए चंदा एकत्रित किया। जिसे मार्ग में डाकुओं ने लूटना चाहा, परंतु महावीर हनुमान जी ने उसकी रक्षा की। इससे अभिभूत होकर उसने आंजनेय (हनुमानजी) का मंदिर बनवाया और विशाल तालाब खुदवाया, परंतु उसके मन में ये भी रहा कि चंदा तो वरदराज पेरूमल के मंदिर के लिए इकट्ठा किया था। अंत में, भक्तों के निर्णय स्वरूप भगवान की वर्षगांठ के दिन अष्यंगारकुलम पहुंचा दिया जाए।
भगवान वरदराज का अविर्भाव यज्ञाग्नि में से हस्तम के ऊपर हुआ था। आज भी इस उत्सव के दौरान उनकी प्रतिमा को ‘नादपवै’ कुएं के भीतर बने हुए मण्डप में ले जाया जाता है। यह कुआं स्थापत्य की भव्यता का अद्वितीय प्रतीक है। उत्सव के समय कुआं पानी से लबालब भरा रहता है। भगवान वरदराज पेरुमाल की मूर्ति को इस मार्ग से सीढ़ियों पर होकर कुएं में ले जाया जाता है। प्रतिमा को कुएं के जल में निमज्जित करके बाहर निकाल लिया जाता है। (तमिलनाडु की लोक संस्कृति और साहित्य, पृ. 138,139)
फसल की सिंचाई के निमित स्थापित कुएं का किसान अपने बच्चे समान ध्यान रखते हैं और यह सब जल संस्कृति में लोक-साहित्य की विभिन्न विधाओं में मिलता है। उदाहरणत: मराठी लोक परंपरा मे ओवी गीत गाया जाता है। इस ओवी गीत में किसान का कुएं के संपूर्ण तंत्र (रहट, बैल इत्यादि) के साथ संबंध स्पष्ट होता है और खेतों की सुचारु सिंचाई हो सके, इसके लिए वह प्रार्थना करता है-
नवस करू गेले हिरीबाई तू सुंदरी।
जतन कर माझे चारी बैल, मोटेकरी।।
हात मी जोडीते, हिरीबाईच्या काठाला।
बाळ माझा लहान, नवा लागलं मोटला।।
किसी क्षेत्र में जब किसी जलाशय की महत्ता या उसकी प्रसिद्धि हो जाती थी तो वह भी जनमानस में लोकोक्ति स्वरूप प्रचलित हो जाती थी। जैसे मैथिली में-
पोखरि रजोखरि आर सब पोखरा,
राजा तं शिवसिंह आर सब छोकरा।
अर्थात् मिथिलांचल में रजोखरि नामक जो जलाशय है वही सही मायनों में पोखरि है शेष सब तो पोखर हैं। (कमलकांत झा, मैथिली लोकोक्ति संचय, पृ. 228)
जल संस्कृति और संस्कार दोनों के पर्याय एक ही जान पड़ते हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता। हमारे 16 संस्कारों में जल की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका अवश्य रहती हैं, क्योंकि जीवन-मृत्यु से जुड़ी समस्त परंपराएं जल से शुरू होकर ‘घड़ा तोड़ने’ की अंतिम क्रिया तक जल से ही बंधी हैं। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में ‘घड़ा तोड़ना’ हमेशा अशुभ माना गया है। इनमें गंगा, कूप-पूजन या जल का पूजन विशेष है।
जलाशयों के निर्माण से लेकर उसकी साफ-सफाई तक की संपूर्ण व्यवस्था बिना किसी थकान के गीत गाते हुए हंसते-खेलते ही हो जाती थी। पुण्य के इस कार्य में राजा से लेकर एक सामान्य व्यक्ति सभी समान रूप से भागीदार होते थे। राजस्थान में यह मिल-जुलकर कार्य करना ल्हास खेलना कहलाता है, तो दक्षिण भारत में कोडग और मध्य प्रदेश में हलमा कहलाता है। दरअसल, हलमा भील समाज के जनजातियों की एक ऐसी लोकपरंपरा है, जिसमें जल अर्थात् पर्यावरण से जुड़े सामजिक कार्यों में निकट के गांवों के हजारों लोग एक साथ श्रमदान करते हैं। इससे कुछ ही घंटों में बड़ी से बड़ी संरचनाएं तैयार हो जाती हैं।
जल संस्कृति का यह रूप समाज को न केवल एक साथ एकत्रित कर सामाजिक एकता की भावना बनाए रखता था, बल्कि जलाशयों एवं इससे जुड़े संपूर्ण ढांचे के प्रति सामाजिक दायित्व भी समझता था। जल संस्कृति का यह रूप बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियों, कविताओं में भी मिलता है, जिनसे बचपन में ही जल के साथ आत्मीय भाव को जागृत किया जाता था और वह बड़ा होकर जल के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझता था। बालक वर्षा से पूर्व गीत गाते हैं-
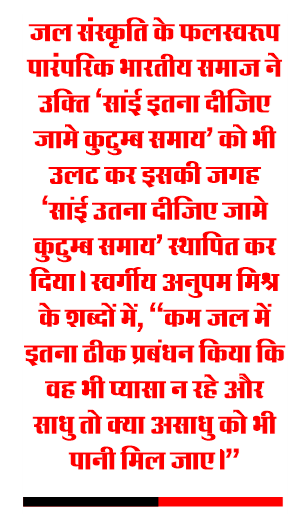 इंदर राजा बेगौ आव, डेडकी नै पाणी पाव
इंदर राजा बेगौ आव, डेडकी नै पाणी पाव
खाडा-नाडा पूर भराव, धोरी मक्की रा कोठा भराव
बच्चे नाचते कूदते गाते हैं-
मेह बाबा आ जा, घी ने रोटी खा जा
जब बारिश शुरू हो जाती है तो मेह में नहाते हुए गाते हैं-
आयौ बाबौ परदेशी, अबै जमानौ कर देसी
आयौ बाबौ परदेसी, खेला-कोठा भर देसी
वर्षा उपरांत फिर से नई पंक्ति गुनगुनाते हैं-
ढ़ाकणी में ढोकलौ, मेह बाबौ मोकलौ
इसी प्रकार से बच्चों को सुनाई जाने वाली एक लोककथा है, जिसमें-एक थी कमेड़ी। वे अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में रोजाना एक बाड़ी तक उड़कर जाती। स्वयं भी पेट भर खाती और बच्चों के लिए चोंच में भरकर ले आती। मगर बाड़ी के माली को यह बात पची नहीं। उसने धोखे से कमेड़ी को अपनी बाड़ी में बंधक बना लिया। कमेड़ी ने राह आते-जाते गड़रियों, रैबारियों, पनिहारिनों से व्यथा कही-
ओ रस्ते जाती पनिहारिन मेरी बहन/बीर
नदिया किनारे मेरे बच्चे री बहन/बीर
आंधी आएगी उड़ जाएंगे री बहन/बीर
मेह आएगा बह जाएँगे री बहन/बीर, कुकडूऊ-कूऊ।
उसने किस-किस से मदद नहीं मांगी पर माली के डर से किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में चूहों ने कमेड़ी का बंधन काट दिया और कमेड़ी अपने बच्चों से मिल गई। इस प्रकार से बाल साहित्य में भी जल संस्कृति को इस प्रकार पिरोया हुआ है।
भारत के सभी क्षेत्रों में जलाशयों से लेकर बड़े-बड़े नगरों, राज्यों, नदियों के नामकरण में भी जल संस्कृति छुपी हुई है। जिस प्रकार उत्तर-पूर्व भारत में जहां वर्षा की औसत मात्रा सर्वाधिक है तो उस क्षेत्र विशेष को मेघालय (मेघ़ालय अर्थात् बादलों का मंदिर) नाम से जाना जाता है। वहीं जिस नदी का जल दूध जैसा स्पष्ट नजर आता है तो वह नदी खिरोदी कहलाती है अर्थात् क्षीर, जो दूध से बनी हुई है। इसी प्रकार जिस नदी का बहाव गो के मूत्र की तरह आढ़े-तिरछे हो, गोमूत्रिका कहलाती है।
जल संस्कृति के फलस्वरूप पारंपरिक भारतीय समाज ने उक्ति ‘सांई इतना दीजिए वामे कुटुम्ब समाय’ को भी उलट कर इसकी जगह ‘सांई उतना दीजिए वामे कुटुम्ब समाय’ स्थापित कर दिया। स्वर्गीय अनुपम मिश्र के शब्दों में, ‘‘कम जल में इतना ठीक प्रबंधन किया कि वह भी प्यासा न रहे और साधु तो क्या असाधु को भी पानी मिल जाए।’’
उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण भारत में जल संस्कृति से संबद्ध विभिन्न परंपराएं प्रचलन में रही हैं। जो एक ओर संकेत करती है कि तत्कालीन समाज जल के संरक्षण के प्रति कितना संवेदनशील था, दूसरी ओर जल के प्रति भावनात्मक संबंध को दर्शाती है। यहां का जनमानस द्वारा वर्षा की तुलना एक व्यक्ति स्वरूप में करते हुए उसे मरुस्थल में बरसने के लिए मनुहार की जाती है। यह केवल राजस्थान में ही नहीं, बल्कि भारत के अन्य राज्यों की लोकोक्तियों व कहावतों में भी देखने को मिलता है। अत: भारत की जल संस्कृति को उजागर करने वाली लोक परंपराओं के अध्ययन से दृष्टिगोचर होता है कि समाज में जल को सदैव अनमोल वस्तु माना गया है, परंतु वह सर्वसुलभ हो इसके लिए व्यक्ति हर स्तर पर प्रयास करना भी अपना नैतिक उत्तरदायित्व समझता था।
(लेखिका जल एवं पर्यावरण मामलों की शोधार्थी और अध्येता हैं)


















टिप्पणियाँ