चुनावी रैली में सूत बराबर फासले से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मौत के मुंह में जाने से बच गए और लगभग इतने ही फासले से अमेरिका गृहयुद्ध से बच गया। पूरी दुनिया के लोग ट्रंप पर गोलीबारी की इस घटना का जायजा लेने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर नजर गड़ाए हुए थे लेकिन रिपब्लिकन और ट्रंप समर्थकों की नजर अमेरिका के बड़े टेलीविजन चैनलों और अखबारों की वेबसाइटों पर थी। रोजाना ‘ट्रंप आए तो प्रलय हो जाएगी’ की भविष्यवाणियां कर रहे इन मीडिया समूहों की वेबसाइटों के शीर्षक सैकड़ों की संख्या में टीवी कैमरों के सामने हुई इस गोलीबारी को देखने के बाद भी यह स्वीकार करने से कन्नी काट रहे थे कि ट्रंप को गोली लगी है।
यह हास्यास्पद था लेकिन विद्रूप यह था कि जो मीडिया समूह यह स्वीकार करने से बच रहे थे कि ट्रंप को गोली लगी है, थोड़ी ही देर बाद वे यह जरूर बता रहे थे कि गोली मारने वाला रिपब्लिकन था। पश्चिमी मीडिया अपने प्रत्यक्ष या परोक्ष हितों के लिए दुनिया में किसी भी घटना को तिल का ताड़ बना देने में माहिर है। लेकिन भारत में कथित असहिणुता, अल्पसंख्यकों के साथ कथित अन्याय या मोदी को तानाशाह कहकर टनों कागज काले करने वाले पश्चिमी मीडिया ने अप्रत्याशित रूप से इस घटना पर चुप्पी साध ली और प्रोपेगेंडा तोप का मुंह सफाई से इजराइल, ईरान और यूक्रेन की तरफ मोड़ दिया।
सवाल ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता के सबसे बड़े पैरोकार पश्चिमी मीडिया ने खबर छिपाने और खबर उछालने की इस कला में इतनी विशेषज्ञता कैसे हासिल कर ली? तो इसका जवाब है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका ने नेतृत्व में मिली जीत को उदारवाद की जीत मान लिया गया। लोकतंत्र, नस्ल, लैंगिक स्वतंत्रता और मुक्त व्यापार जैसी कई चीजों पर एक आम सहमति बनी जो अभी तक लगभग कायम थी। और इस आख्यान को गढ़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई लिबरल सत्ता प्रतिष्ठान के पिछलग्गू बन चुके लिबरल मीडिया ने। वर्चस्व इतना लंबा चला कि आत्ममुग्ध और आत्मसंतुष्ट लिबरल मीडिया ने मान लिया कि यह चिरस्थायी है और इन आम सहमतियों की चौहद्दी के बाहर खड़ा कोई भी तर्क या विचार अतार्किक और अरक्षणीय है।
दुनिया में हर विचारधारा में कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं जो अपनी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि सहनशीलता, अन्य विचारों को आत्मसात करने और खुले विचारों वाले होने का दावा करने वाले उदारवादी विचारधारा के पैरोकार अपने इस दृढ़ विश्वास में काफी आगे हैं कि उदारवाद की श्रेष्ठता स्वत:सिद्ध है और इसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उनका मानना है कि यह तथ्यों व तर्क पर आधारित है जबकि दक्षिणपंथी सिर्फ गलत ही नहीं हैं बल्कि उनकी पूरी विचारधारा अवैध है और यह विचारधारा किसी गंभीर विचार विमर्श के लायक नहीं है। लिहाजा उनसे असहमत लोग नस्लवादी होंगे, रंगभेदी होंगे, महिला विरोधी होंगे और इस नाते तिरस्कार के पात्र हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में हिलेरी क्लिंटन ने जब ट्रंप समर्थकों को ‘धिक्कृतों का झुंड’ कहा था तो यह वही आत्ममुग्धता और श्रेष्ठता बोध था। भारत में इस लिबरल आम सहमति के दायरे से बाहर खड़े लोगों को गोदी मीडिया, भक्त, सांप्रदायिक, संघी, फासिस्ट कहा जाता है और दक्षिणपंथियों के प्रति तिरस्कार को अभिव्यक्ति देने वाले ये शब्द अब मुख्य धारा की लिबरल मीडिया की वर्तनी का मुख्य हिस्सा बन चुके हैं।
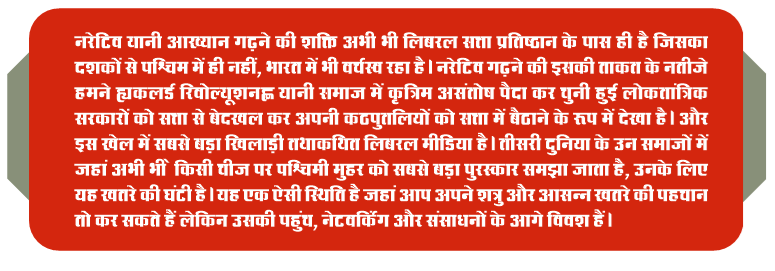
लिबरल मीडिया के लिए यह असहज करने वाली स्थिति है कि कल तक वे सत्य के रखवाले और उसके पालनहार थे, सवाल पूछने पर उनका एकाधिकार था, आज सबसे ज्यादा सवाल उनसे ही पूछे जा रहे हैं। सूचना क्रांति की वजह से खबरों पर मुख्य धारा की मीडिया की मोनोपॉली खत्म हो चुकी है और सोशल मीडिया के जमाने में सेंसरशिप संभव नहीं रह गई है। सोशल मीडिया के कारण अब खबरों को दबाना या उन्हें पूरी तरह अपनी मर्जी से पेश कर पाना संभव नहीं रहा। लिहाजा लिबरल मीडिया अब सोशल मीडिया के सवालों को कांस्पिरेसी थ्योरी या दक्षिणपंथी ट्रोल बताकर इस चुनौती से मुंह चुराने की कोशिश में है। लेफ्ट लिबरल तबके में एक आम सहमति अब तक कायम है कि अपने मिजाज की जो खबरें वे परोसते हैं, वे व्यापक हित में है और जो नहीं परोसते वह किसी लिबरल बायस की वजह से नहीं बल्कि सौहार्द और समरसता जैसे महान उद्देश्यों से प्रेरित है।
हालांकि ज्यादातर लोग इससे सहमत नहीं हैं। अक्तूबर 2016 में ही भाषाविदों, पत्रकारों और लेखकों की एक जूरी ने ‘लुजेनप्रेस’ यानी झूठा प्रेस को साल का सबसे प्रचलित शब्द घोषित किया था। इसकी जड़ें जर्मनी के शहर कोलोन में 31 दिसंबर, 2015 की मध्यरात्रि को हुई घटना में हैं। कोलोन में नववर्ष के जश्न के मौके पर बड़े पैमाने पर जर्मन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुईं, जिसे जर्मन मीडिया ने बेशर्मी के साथ दबाने की कोशिश की। सभी उत्पीड़क मुस्लिम थे जो हाल ही में पीड़ित शरणार्थी के रूप में जर्मनी में दाखिल हुए थे। लेकिन जर्मन मीडिया को लगा कि इस घटना के बारे में छापा गया तो जनता में अरब मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ नाराजगी पनपेगी जो उनकी राय में जर्मन उदारवादी मूल्यों के विपरीत होगा। जनाक्रोश के बाद जर्मन अखबारों ने जब मुंह खोला तो उन्होंने लगभग मोटे तौर पर एक सुर में कहा कि यह घटना विदेशियों के एकीकरण में जर्मन समाज की नाकामी का प्रतीक है। यानी दोष बलात्कारियों की भीड़ का नहीं, जर्मन समाज का है। लिबरल मीडिया के लिए हर अपराध की जवाबदेही मुख्यधारा के समाज यानी बहुसंख्यक वर्ग की है।
यह सिर्फ एक घटना नहीं है। आए दिन की घटनाएं और उन्हें पेश करने के तरीके से स्पष्ट है कि लिबरल खबरों के चुनाव और उन्हें पेश करने में पूरी तरह चयनात्मक है, इसके मानदंड दोहरे हैं। धर्म, लिंग, नस्ल, अल्पसंख्यक के नाम पर कुछ समुदायों की करतूतों पर पूरी तरह लीपापोती की जाती है तो कुछ को भरपूर उछाला जाता है। दिल्ली की सीमा से सटे दादरी एवं कथित रूप से चर्चों पर हमले की घटनाओं की तुलना पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ की घटना से करें तो लिबरल मीडिया के इस दोहरे चाल चरित्र और चेहरे के बारे में कोई संशय नहीं बचता। दादरी में अखलाक की हत्या एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनी और ‘असहिष्णुता’ के खिलाफ अवार्ड वापसी आंदोलन चला।
महीनों तक यह घटना अखबारों के पहले पन्ने और संपादकीय पन्नों पर बनी रही। उधर, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मार्च, 2015 को कुछ अपराधी चर्च की 71 वर्षीय नन से सामूहिक बलात्कार के बाद दस लाख रुपए लूट ले गए। इसे बड़े पैमाने पर बढ़ती असहिष्णुता के नतीजे के तौर पर प्रचारित किया गया। एक मोदी निंदा विशेषज्ञ और अल्पपसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिला पत्रकार ने एक प्रतिष्ठित वेबसाइट पर सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लिया। बिना किसी जांच पड़ताल के और बेबुनियादी आरोप लगा दिए गए। जांच के बाद जो गिरफ्तारियां हुईं, उसमें ये सारे अपराधी बांग्लादेश से आए निकले और वे उसी समुदाय के थे जिन्हें भारत में अल्पसंख्यक कहा जाता है। अपराधियों का धर्म पता चलते ही अचानक यह मुद्दा रहस्यमय तरीके से मीडिया से गायब हो गया।
उधर, दिसंबर 2016 में कोलकाता से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर हावड़ा के धूलागढ़ में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को मीडिया में कहीं भी जगह नहीं मिली, जबकि पीड़ित मीडियाकर्मियों को हिंसा के वीडियो भेजकर कार्रवाई की गुहार लगाते रहे। तमाम फोटो और वीडियो के रूप में दस्तावेजी सबूत हाथ में होने के बावजूद कोलकाता की लिबरल मीडिया को लगा कि इस घटना की रिपोर्टिंग गैरजिम्मेदाराना होगी क्योंकि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। घटना के कई दिन बाद ‘जी न्यूज’ के तत्कालीन मुख्य संपादक सुधीर चौधरी ने एक कार्यक्रम में इस पर चर्चा की। लेकिन इससे नाराज होकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चौधरी और जी न्यूज की रिपोर्टर और कैमरामैन के खिलाफ दंगे भड़काने की कोशिश सहित कई गैरजमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी। हिंसा के कई दिन बाद रिपोर्टर जब धूलागढ़ पहुंचे तो नाराज पीड़ितों की भीड़ ने मीडियाकर्मियों पर ही हमला कर दिया।
यह विश्वसनीयता खत्म हो जाने का नतीजा है। ब्रिटेन में हाल ही में हुए दंगों में प्रदर्शनकारी ‘किड्स डाइंग, मीडिया लाइंग’ जैसी तख्तियां लिखे देखे गए। लेकिन इन आवाजों की जगह सिर्फ सोशल मीडिया में है। ब्रिटिश लिबरल मीडिया फिलहाल हिंसा के कारणों की पड़ताल के बजाय धुर दक्षिणपंथ के उभार के खतरों की चर्चा में व्यस्त है। लिबरल मीडिया के कंधे पर बहुत बोझ है। उदारवादी सत्ता प्रतिष्ठान का हिस्सा होने के नाते उन्हें अपनी पसंद के मुद्दे उठाने हैं, असहज करने वाली चीजों की अनदेखी करना है, उन पर निशाना साधना और फिर उन पर समाज में विद्वेष फैलाने या सत्ता समर्थक होने का आरोप लगा कर उनकी विश्वसनीयता पर हमला करना है। सदैव सत्ता प्रतिष्ठान का पिछलग्गू रहे लिबरल मीडिया का यह चाल, चरित्र और चेहरा है। बस सोशल मीडिया और सूचना के वैकल्पिक माध्यमों ने इस चेहरे को बेनकाब कर दिया है। लेकिन लिबरल मीडिया की विश्वसनीयता के इस खात्मे के खतरे गंभीर होने वाले हैं क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत चाहे जितनी हो, यह मुख्यधारा का मीडिया नहीं बन सकता और इसकी भूमिका वैकल्पिक मीडिया तक ही सीमित रहेगी। जरूरत है एक निरपेक्ष मीडिया की जहां राष्ट्र, संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी चिंताओं को भी जगह मिले। लेकिन इनकी बात करने वालों को सांप्रदायिक, भक्त, संघी, फासिस्ट और विभाजनकारी ही कहा जाएगा।
नरेटिव यानी आख्यान गढ़ने की शक्ति अभी भी लिबरल सत्ता प्रतिष्ठान के पास ही है जिसका दशकों से पश्चिम में ही नहीं, भारत में भी वर्चस्व रहा है। नरेटिव गढ़ने की इसकी ताकत के नतीजे हमने ‘कलर्ड रिवोल्यूशन’ यानी समाज में कृत्रिम असंतोष पैदा कर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को सत्ता से बेदखल कर अपनी कठपुतलियों को सत्ता में बैठाने के रूप में देखा है। और इस खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी तथाकथित लिबरल मीडिया है। तीसरी दुनिया के उन समाजों में जहां अभी भी किसी चीज पर पश्चिमी मुहर को सबसे बड़ा पुरस्कार समझा जाता है, उनके लिए यह खतरे की घंटी है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप अपने शत्रु और आसन्न खतरे की पहचान तो कर सकते हैं लेकिन उसकी पहुंच, नेटवर्किंग और संसाधनों के आगे विवश हैं। दादरी की घटना और चर्चों पर कथित हमलों के आलोक में छिड़ी असहिष्णुता पर बहस और अवार्ड वापसी सर्कस से मचे होहल्ले के नतीजे में दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की पराजय इसका सबूत है।
(लेखक मीडिया रणनीतिकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं)

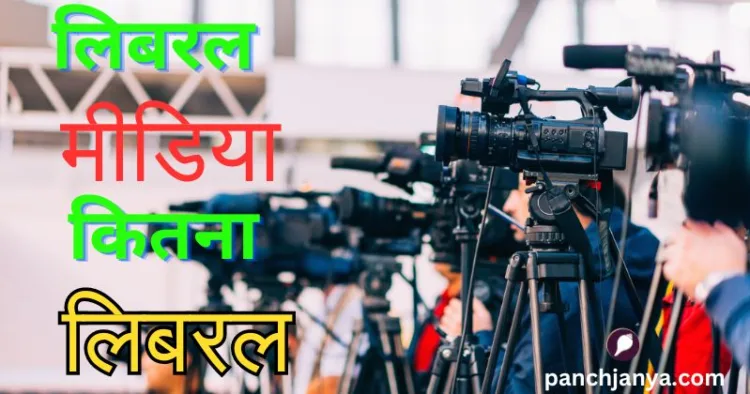















टिप्पणियाँ