युवा वर्ग 12वीं के बाद भविष्य के स्वर्णिम सपने संजोये उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दाखिला लेता है। इस समय वे जीवन के उच्चतम उर्जा स्तर पर होते हैं। उन्हें सही परामर्श और उचित मार्गदर्शन से ज्ञानार्जन के प्रति उनकी रुचि बढ़ाई जा सकती है।

कुलपति केंद्रीय विश्विद्यालय, बठिंडा
देश का युवा वर्ग 12वीं के बाद भविष्य के स्वर्णिम सपने संजोये उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दाखिला लेता है। इस समय वे जीवन के उच्चतम उर्जा स्तर पर होते हैं। उन्हें सही परामर्श और उचित मार्गदर्शन से ज्ञानार्जन के प्रति उनकी रुचि बढ़ाई जा सकती है। साथ ही, समग्र शिक्षा उपलब्ध करा कर उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। यह ध्यान रखना होगा कि जब ये रोजगार के योग्य होंगे, तब उन्हें ऐसे कार्य-स्थलों का सामना करना होगा, जहां निष्पादित होने वाले कार्यों की न तो अभी कल्पना की जा सकती है और न ही उनके संपादन हेतु जिन कौशलों एवं तकनीकियों की आवश्यकता होगी, उनके बारे में सोचा जा सकता है। इसके इतर आज के युवा शिक्षा-4.0 के युग में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह परिणाम आधारित है।
शिक्षा 4.0 का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक क्रांति 4.0 को बढ़ावा देने के लिए कौशल एवं वैश्विक क्षमतावान युवा तैयार करना भी है। इन परिस्थितियों में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के युवाओं को शिक्षित करने की दशा एवं दिशा क्या हो, यह चिंतन का विषय है। बहुत हद तक इसका जवाब राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में निहित है। शिक्षा नीति की मुख्य चिंता वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों के सापेक्ष 21वीं सदी के अधिगमकर्ताओं में खास कौशलों एवं अभ्यासों का निर्माण करना है। यह शिक्षा को ऐसी सामाजिक-सांस्कृतिक परियोजना के रूप में प्रस्तावित करती है, जिसमें अधिगमकर्ता देशज ज्ञान से जुड़े होने के साथ बोध की आधुनिक आलोचनात्मक तार्किकता से भी युक्त हो। इसमें विषय-वस्तु सिखाने की बजाय सीखने की कला एवं बुनियादी कौशलों को प्राथमिकता दी गई है। सीखने की यही प्रक्रिया अधिगमकर्ता को उन संभावनाओं से युक्त करेगी, जहां वह उद्यमशीलता, रोजगारकर्ता एवं कौशल के स्वायत्त व आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी का निर्माण कर सकें।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पांचवीं कक्षा तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही अध्ययन करवाया जाएगा।
- माध्यमिक चरण पर कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी, इसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाएगा। यह चरण 3 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इस चरण में बच्चों के लिए खास कौशल विकास पाठ्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे।
- उच्चतर माध्यमिक चरण में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी , इसमें 14 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। यह चरण 4 वर्ष में पूरा होगा।
बदलावों और चुनौतियों का दौर
21वीं सदी न केवल ज्ञान की प्रकृति, स्वरूप और नवाचारों, बल्कि ज्ञान-आर्थिकी एवं सामाजिक सरोकारों के संदर्भ में भी बदलावों और चुनौतियों से गुजर रही है। वैश्विक स्तर पर ज्ञान-संरचना और तकनीकी में सम-सामायिक बदलाव ज्ञान की अवधारणात्मक ज्ञानमीमांसा को विषय-वस्तु के सापेक्ष ही नहीं, पद्धतिमूलक संदर्भ में भी पुनर्व्याख्यायित कर रहे हैं। वर्तमान में ‘बिग डाटा एनालिटिक्स’, ‘मशीन लर्निंग’, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’, ‘इंटरनेट आफ थिंग्स’, ‘वर्चुअल रियलिटी’, ‘अगमेंटेड रियलिटी’ आदि बदलते समय की अधिगम वैचारिकी को गढ़ रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों में रचनात्मकता एवं नवाचार कौशल से संबद्ध ज्ञान ही साधन एवं साध्य की अपरिहार्य भूमिका में हों। साधन-साध्य की यह युति ही वैश्विक संदर्भ में विकराल होती समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थियों को इन्हें परिभाषित करने के निमित्त सक्षम बनाएगी। सवाल यह है कि क्या हम महाविद्यालयीय एवं विश्वविद्यालयीय विद्यार्थियों को वैश्विक ‘ज्ञान के डिजिटलीकरण’ के साथ-साथ भारतीय ज्ञान-संरचनाओं को संदर्भित करने योग्य बना रहे हैं? क्या हम उनको भविष्य की चुनौतियों का सामना करने हेतु सशक्त बनाने के लिए उनकी ऊर्जा और क्षमता का उचित ढंग से प्रयोग करने में उन्हें सक्षम बना पा रहे हैं? ज्ञान-संरचनाओं में हो रहे व्यापक डिजिटलीकरण एवं कौशल विकास के उदीयमान प्रारूपों ने शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के समक्ष समान रूप से विषय ज्ञान के साथ कौशल एवं गुणवत्ता के निर्धारण में निश्चित रूप से विचलन एवं चुनौती पेश की है।

पाठ्यक्रम संरचना एवं अधिगम प्रणाली
स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के बीच पाठ्यक्रम संरचना, विषयवस्तु, अधिगम तथा मूल्यांकन प्रणाली में तारतम्यता स्थापित करने के साथ इन सभी क्षेत्रों में सुधार भी अत्यावश्यक है। साथ ही, मूल पाठ्यक्रमों के इतर वैकल्पिक, अंतर्विषयक, कौशल एवं उद्यमिता आधारित, मूल्य-वर्धित, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का समुचित अनुपात में समावेश और सीखने के प्रतिफलों का पूर्व निर्धारण भी बहुत जरूरी है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिफलों का पाठ्यक्रम सामग्री के साथ सामंजस्य बनाना चाहिए। इन सभी में अधिगम प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सभी स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में केवल लिखवाया जाता
है, जिससे विद्यार्थियों में चिंतनशीलता व तार्किकता का विकास नहीं हो पाता।
शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन कक्षाओं को सीखने के सक्रिय स्थलों में कैसे परिवर्तित किया जाए। एक कारगर उपाय यह हो सकता है कि प्रत्येक सेमेस्टर में एक अवधि पत्र हो, जिसमें उस सेमेस्टर के संबंधित विषयों में प्रमुख शोध, प्रगति, सामाजिक घटनाएं, महामारी, फसलों की बीमारी, प्रकृति में मुख्य बदलाव, प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाओं आदि विषयों पर विद्यार्थियों को विमर्श एवं स्थिति-पत्रक बनाने में दक्ष किया जाए। वर्तमान अधिगम का स्वरूप त्रुटिपूर्ण है। यह अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को न तो उत्साहित करने में समर्थ है, न ही उनके लिए रुचिकर है। यह विश्व स्तरीय उच्चतम दक्षता और विचारपूर्ण कौशल की बजाय प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन में यांत्रिक प्रदर्शन एवं अंकीय श्रेष्ठता को महत्व देता है। साथ ही, अंकीय परीक्षाओं का वर्तमान प्रारूप अधिगमकर्ता की वास्तविक बौद्धिक क्षमता के समग्र आकलन में भी अक्षम है। आज ज्ञान और बोध के स्तर पर बहुआयामी शिक्षा की आवश्यकता है। मूल-पाठ्यक्रमों के इतर, पारंपरिक एवं आधुनिक ज्ञान के बीच सामंजस्य, तार्किक, नवाचारधर्मी एवं वैज्ञानिक प्रणाली से युक्त विद्यार्थी ही अपने समय की चुनौतियों से पार पा सकता है।
क्या सीखें से जरूरी ‘कैसे सीखें’
व्यक्तिगत, प्रायोगिक एवं मिश्रित अधिगम, विविधतापूर्ण अधिगम अवसरों का अनुप्रयोग जैसे- कार्यात्मक एवं अनुभवयुक्त अधिगम के साथ समूह चर्चा, वाद-विवाद, तर्क, पर्यटन, इंटर्नशिप, सामुदायिक परियोजनाओं एवं कार्यशालाओं आदि में सहभागिता द्वारा ही अधिगम एवं मूल्यांकन की व्यवस्था को परिवर्तित कर आनंददायक बनाया जा सकता है। इसके लिए कक्षाओं से बाहर उपलब्ध ज्ञान-समुदायों, समूहों एवं संस्थाओं से संलग्नता अपरिहार्य है। ऐसा करके एक अधिगमकर्ता सूचना एवं तकनीकी के सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग (डिजिटल तकनीकी के उपयोग द्वारा उच्च शिक्षा में मूल्यों का सृजन), अधिगम को कौशल एवं उद्यमिता के साथ एकीकृत करने (परिवर्तन, नवाचार तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए), वैश्विक दक्षता विकसित करने (छात्रों में न्यायोचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और अवसर उत्पन्न करना) तथा ज्ञान-समाज में अस्तित्व बनाए रखने हेतु ‘क्या सीखें’ की अपेक्षा ‘कैसे सीखें’ की प्रवृत्ति को विकसित करने से दक्षता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए विद्याथी प्राचीन शिक्षा प्रणाली से सूत्र प्राप्त कर सकते हैं।
काक चेष्टा बको ध्यानं, स्वान निद्रा तथैव च।
अल्पहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी पञ्च लक्षणं।।
उक्त श्लोक में विद्यार्थियों के पांच लक्षण बताए गए हैं। कौवे की तरह सीखना (यानी तब तक प्रयास करना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए), बगुले की तरह काम पर ध्यान केंद्रित करना, कुत्ते की भांति सतर्कता के साथ सोना, संतुलित आहार लेना और समग्र शिक्षा के लिए सभी घरेलू सुख-सुविधाओं का त्याग करना। इसके अलावा, वैदिक परंपरा में प्रश्न पूछने, सत्यापन करने, तर्क सहित विचार रखने और गहराई से सोचने आदि को अधिगम होने की स्थिति के रूप में स्वीकृति प्राप्त थी। सीखने की अवधारणा भारतीय ज्ञानमीमांसा में क्या, क्यों, कैसे सीखा जाए के साथ जो अधिगम योग्य नहीं है, उनको वर्गीकृत करने की संज्ञानात्मक व्यूहरचना से निर्मित होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को इसी आलोक में समझा जा सकता है। यह ‘लर्निंग टू लर्न’ की अनिवार्यता के साथ ‘अन-लर्न और री-लर्न’ की नैसर्गिक महत्ता सदैव अधिगम-पारिस्थितिकी का निर्माण करती है।
…इसलिए विश्व गुरु बना भारत
गुरुकुल परंपरा की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत विश्व गुरु बना। गुरुकुल शिक्षा के आवासीय केंद्र थे, जो सार्वजनिक दान से चलते थे। इसलिए उन्हें पढ़ाए जाने वाले विषयों को तय करने, पाठ्यक्रम बनाने, अधिगम एवं मूल्यांकन प्रणाली को तय करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। गुरुकुल में शिक्षक और विद्यार्थी संयमपूर्ण जीवन-शैली के माध्यम से जीवनपर्यंत नैतिकता के आदर्श स्थापित करते थे। गुरुकुलों में 16 विषय और 64 कौशल आधारित पाठ्यक्रम सिखाए जाते थे। वर्तमान शिक्षण प्रणाली की तरह परीक्षा नहीं होती थी, वरन निरंतर मूल्यांकन पद्धति द्वारा सीखने के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता था। गुरुकुलों की मान्यता थी कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। वस्तुत: गुरु सूत्रधार और मार्गदर्शक होते थे। वे शिष्यों के मस्तिष्क को प्रशिक्षित नहीं करते थे, अपितु उन्हें यह दर्शाते थे कि उनके सीखने के अधिगमजन्य साधनों को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार, गुरुकुल आत्मविश्वास, आत्म-अनुशासन, चरित्र-निर्माण, सामाजिक जागरूकता, व्यक्तित्व विकास, बौद्धिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक उन्नति, तार्किक ज्ञान और संस्कृति के संरक्षण जैसी अन्यान्य विशेषताओं को विकसित करने में सफल रहे, जो गुणवत्तापरक शिक्षा के आवश्यक घटक हैं।
प्राचीन भारतीय संदर्भ में भी ऐसे अनेक ‘मेटा-नैरेटिव’ मौजूद हैं। आद्य जगतगुरु शंकराचार्य का मत है कि सीखने की प्रक्रिया तीन चरणों-‘श्रवण’, ‘मनन’ एवं ‘निधिध्यासन’ में पूरी होती है। श्रवण ज्ञानार्जन की अवस्था है, मनन मतलब जो सुना उसका विश्लेषण और उसे आत्मसात करना, जबकि निधिध्यासन का अर्थ है सत्य की समझ और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में इसका अनुप्रयोग करना, जो बोध का चरण होता है। बल्लभाचार्य के अनुसार, एक दक्ष विद्यार्थी में तीन गुण होने चाहिए। इसमें जिज्ञासा पहला और सबसे महत्पूर्ण गुण है। अधिगम प्रक्रिया को केवल सफलता का सोपान नहीं मानना चाहिए, बल्कि यह जिज्ञासु में अतंर्निहित, सतत और स्थायी इच्छा होनी चाहिए। निष्ठा दूसरा गुण है, जिसका मतलब है विद्यार्थी को खुद को शिक्षक से बेहतर या कमतर नहीं आंकना चाहिए। उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि शिक्षक उससे अधिक ज्ञानवान है तथा उसे विनम्रतापूर्वक ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव उत्सुक रहना चाहिए। तीसरा गुण है श्रवणदार, जिसका तात्पर्य है कि विद्यार्थी को चौकस, समयनिष्ठ, जिज्ञासु होना चाहिए और दिए गए कार्यों को निश्चित समयावधि में पूर्ण करना चाहिए तथा व्याख्यान आदि में सहभागी होना चाहिए।
प्राचीन काल में भारतीय ग्रामीण कौशल अद्वितीय था। प्रत्येक ग्रामीण समुदाय किसी न किसी प्रकार के कौशल से संपन्न था, जिसका उपयोग आजीविका हेतु किया जाता था। यानी प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह की सार्थक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न था और ग्रामीण उत्पादकता को समृद्ध कर रहा था। लेकिन इस तरह के कौशल निरंतर कम होते जा रहे हैं, जिस पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनौपचारिक ग्रामीण कौशल केंद्रों में मौजूद कौशल को बढ़ावा दिया सकता है। यह ऐसे ग्रामीण कौशल केंद्रों में प्रशिक्षित युवाओं को सरकारी-निजी संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों में रोजगार या लघु पैमाने पर स्टार्टअप और उद्यमशीलता के प्रयास शुरू करने में सक्षम बनाएगा। साथ ही, युवाओं को प्रकृति संरक्षण हेतु संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। भारत जैसे बड़े देश में, सरकार के साथ निजी कंपनियों को भी युवाओं के कौशल विकास हेतु कार्य करना चाहिए। सामान्य शिक्षा सफल ज्ञान आधारित करियर के लिए उत्कृष्ट आधार होते हुए भी स्नातकों को आवश्यक कार्य कौशल से लैस करने में विफल है। ‘जीवनपर्यंत सीखना’, अधिगम की यह अनुभाविक प्रक्रिया ही भारतीय ज्ञान संस्कृति की मूल प्रविधि रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 अधिगम के इस समुच्चय के सांस्कृतिक अधिष्ठान की पुनर्स्थापक सिद्ध हो सकती है।
(लेखक- केंद्रीय विश्विद्यालय, बठिंडा, कुलपति हैं)







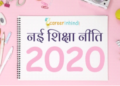










टिप्पणियाँ