हरियाणा के लगभग 60 प्रतिशत गांवों में भू-जल गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। कम बरसात ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। राज्य के 45 प्रतिशत भाग में भूमिगत जल खारा है, जो न पीने लायक है, न सिंचाई के लिए उपयुक्त। जल संकट को देखते हुए राज्य सरकार धान की सीधी बिजाई, सिंचाई की आधुनिक तकनीक व फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही
हरियाणा को भारत के ‘ब्रेड बास्केट’ के तौर पर जाना जाता है। प्रदेश में मुख्यत: चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, तिलहन, बाजरा, चना और जौ का उत्पादन होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत से जो बासमती चावल का निर्यात होता है, उसमें हरियाणा की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन गिरते भू-जल स्तर ने राज्य के चावल उत्पादकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं।
दरअसल, हरित क्रांति के बाद हरियाणा सिंचाई क्षेत्र में भू-जल के प्रमुख उपयोगकर्ता के रूप में उभरा है। भू-जल से सिंचाई के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव तो आया ही, खाद्य सुरक्षा और विशेष रूप से राज्य की आजीविका वृद्धि में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि राज्य के सकल मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 2021-22 में बढ़कर 16.9 प्रतिशत हो गई, जो 2015-16 में 3.2 प्रतिशत थी। प्रगतिशील अत्याधुनिक नीतियों को अपना कर कृषि क्षेत्र (प्राथमिक क्षेत्र) ने अपनी हिस्सेदारी लगभग 19.5 प्रतिशत कर ली है। यही नहीं, देश के सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा के कृषि क्षेत्र का योगदान 14.1 प्रतिशत है। लेकिन यह उपलब्धि भू-जल के अंधाधुंध दोहन से हासिल हुई है। हरियाणा में साल-दर-साल भू-जल स्तर खतरनाक दर से गिर रहा है। खासतौर से दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के जिले इससे अधिक प्रभावित हैं। यही नहीं, भूमिगत पानी की गुणवत्ता भी खराब हो गई है।
गिरता जल स्तर
सूबे के भू-जल स्तर में 1974 से 2019 तक औसत गिरावट लगभग 10.65 मीटर दर्ज की गई है। भू-जल स्तर की गहराई आमतौर पर दक्षिणी भागों में उच्च और उत्तर-पूर्व पहाड़ी क्षेत्र में कम होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कृषि सिंचाई में भूमिगत जल के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण 1995 से 2020 तक राज्य के भू-जल में औसतन 9.47 मीटर की गिरावट आई है। कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में धान की बुआई से जलस्तर तेजी से गिरा है। वहीं, खेती में रासायनिक उर्वरकों, एक साल में अधिक फसलें उपजाने, कम उपजाऊ मिट्टी, परंपरागत सिंचाई प्रणाली और शहरीकरण के कारण रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों में भू-जल स्तर और इसकी गुणवत्ता में गिरावट आई है। आलम यह है कि लगातार पांच दशक से हो रहे दोहन के कारण कुछ जिलों में भू-जल स्तर 80 फीट नीचे चला गया है, जो कृषि के लिए एक गंभीर संकट बन कर उभर रहा है
लंबे समय तक फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। भिवानी जिले में पानी में खारापन (1,692-2,560 मिलीग्राम/लीटर), क्षारीयता (442-1,232 मिलीग्राम/लीटर), बाइकार्बोनेट (554-672 मिलीग्राम/लीटर) भी मान्य सीमा से अधिक पाया गया है। इसी तरह, झज्जर जिले में भू-जल तो खारा है ही, यह बहुत अधिक दूषित भी है, जिससे लोगों को बीमारियां हो रही हैं और इसके कारण उन पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा के 141 खंडों में से 85 में भू-जल का अत्यधिक दोहन हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि पुनर्भरण की मात्रा के मुकाबले इन क्षेत्रों ने 100 प्रतिशत भू-जल का दोहन किया है। यानी भू-जल पुनर्भरण सालाना 100 लीटर है, तो निकासी 200 लीटर से अधिक हो रही है। इसी तरह ‘गंभीर’ श्रेणी के 12 अन्य खंडों में भू-जल दोहन की गति 90 से 100 प्रतिशत है, जबकि 14 खंड, जहां भू-जल दोहन 70 से 90 प्रतिशत के बीच है, को ‘अर्ध-महत्वपूर्ण’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केवल 30 प्रखंडों को सुरक्षित घोषित किया गया है।
आलम यह है कि सूबे के लगभग 60 प्रतिशत गांवों में भू-जल स्तर को ‘तनाव ग्रस्त’ या ‘संभावित तनावग्रस्त’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि इसके कारण लगभग 2 करोड़ लोगों के जीवन और आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है।
पानी में घुलता जहर
कई जिलों में भू-जल भी प्रदूषित हो गया है, जबकि खारा पानी न तो पीने योग्य है और न ही सिंचाई के लिए उपयुक्त। हरियाणा में मोटे तौर पर भू-जल समस्या के दो आयाम हैं- पहला, निम्न गुणवत्ता वाले जलभृतों के साथ दक्षिणी भागों में बढ़ता भू-जल स्तर, जिसके कारण द्वितीयक लवणीकरण और जलभराव होता है। इससे राज्य का लगभग 10 प्रतिशत क्षेत्र जलभराव की स्थिति में है। दूसरी ओर, मीठे पानी वाले जलभृत क्षेत्रों में भू-जल के अत्यधिक पंपिंग के कारण जल स्तर में गिरावट। खासकर जिन जिलों में धान और गन्ने की खेती अधिक होती है, वहां भू-जल स्तर की स्थिति अत्यन्त चिंताजनक है। हालांकि राज्य के कई जिलों में जल स्तर की गहराई में औसत वृद्धि हुई है। 1974 से 2014 के बीच गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में जल स्तर की गहराई लगभग दोगुनी हो गई है।
2004 के अनुमानों की तुलना में 2009 में सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भू-जल उपयोग में सालाना लगभग 31.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 2004 से 2017 तक सालाना शुद्ध भू-जल उपलब्धता और भू-जल निकासी में 311 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य में औद्योगिक अपशिष्ट के बिना उपचार निपटान के कारण भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है। खासकर अंबाला, पानीपत और भिवानी में पीने के पानी में फ्लोराइड के अंश मिले हैं। लंबे समय तक फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। भिवानी जिले में पानी में खारापन (1,692-2,560 मिलीग्राम/लीटर), क्षारीयता (442-1,232 मिलीग्राम/लीटर), बाइकार्बोनेट (554-672 मिलीग्राम/लीटर) भी मान्य सीमा से अधिक पाया गया है। इसी तरह, झज्जर जिले में भू-जल तो खारा है ही, यह बहुत अधिक दूषित भी है, जिससे लोगों को बीमारियां हो रही हैं और इसके कारण उन पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
45 प्रतिशत पानी खारा
राज्य के 45 प्रतिशत हिस्से का भू-जल खारा है। इससे सिंचाई भी नहीं हो सकती। राज्य में सतही जल संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इसका 60 प्रतिशत से अधिक प्रयोग सिंचाई में किया जाता है। जल उपलब्धता के हिसाब से हरियाणा की गिनती ऐसे राज्य के रूप में होती है, जहां सतही और भूमिगत जल की कमी है। राज्य को नौ भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया गया है, जहां दो प्रमुख नदियों- घग्गर और यमुना से सिंचाई की जाती है। हरियाणा में कुल पानी की आवश्यकता 20 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) है। राज्य को यमुना और भाखड़ा से लगभग 2.3 एमएएफ पानी मिलता है, जबकि 12 एमएएफ पानी 8.48 लाख नलकूपों से निकाला जाता है। कुल मिलाकर हरियाणा सालाना 5.7 एमएएफ पानी की कमी का सामना कर रहा है। सूबे का अधिकांश हिस्सा जलोढ़ क्षेत्र में आता है। भू-जल विशेषज्ञों के अनुसार, जल संकट से निपटने में राज्य की संसाधन इकाइयों की जैव-भौतिक विशेषताओं, उपयोगकर्ताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, भू-राजनीतिक परिस्थितियों और भौगोलिक क्षेत्र की पारिस्थितिक चिंताओं में संलग्न जटिलता और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाती है।
कम वर्षा बनी समस्या
हरियाणा में हर साल औसत 354.5 मिमी. बारिश होती है। 2018 में मानसून के सामान्य होने के कारण 415.2 मिमी वर्षा हुई। लेकिन 2017 में 25 प्रतिशत कम बारिश हुई। हालांकि 2019 में देश में मानसून बीते 25 साल के मुकाबले अच्छा रहा और जून-सितंबर के दौरान राज्य में 42 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई। कुल मिलाकर बीते 10 वर्षों में से 6 वर्ष (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017) में मानसून्न खराब रहा, जिसके कारण राज्य में पानी की स्थिति और गंभीर हो गई है। ऊपर से पानी की जरूरतों और धान-गेहूं, कपास-गेहूं, गन्ना-गेहूं की खेती के कारण भूमिगत जल का बड़े पैमाने पर लगातार दोहन हो रहा है, जिसके कारण जल स्तर तेजी से गिर रहा है।
न्यूनतम और आश्वस्त समर्थन मूल्य के कारण इन फसलों की बढ़ी हुई लोकप्रियता और सुनिश्चित बाजार के कारण किसान इन्हीं फसल चक्रों पर ध्यान देते हैं। शुरुआत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चावल और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूरी था, लेकिन अब यह फसल विविधीकरण के मार्ग में बाधा बन रहा है। गेहूं और धान की खेती का रकबा बढ़ने से अब नुकसान हो रहा है। अमूमन एक किलो चावल के उत्पादन में लगभग 2,500-5,000 लीटर पानी खर्च होता है। 1966 में हरियाणा जब अलग राज्य बना था, उस समय सूबे में करीब 1.96 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की खेती होती थी। बीते साल यह बढ़कर 14.70 लाख हेक्टेयर हो गई। इसे देखते हुए राज्य में कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा-जल संचयन की तत्काल आवश्यकता है।
सरकारी योजनाओं से बचेगा पानी
राज्य सरकार 79 प्रतिशत गांवों में तेजी से हो रहे भू-जल दोहन के बीच हर गांव में जल स्तर का नक्शा तैयार करेगी। साथ ही, गिरते भू-जल को रोकने के लिए सूक्ष्म सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली और तालाब खोदने के लिए 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार पुराने व टूटे हुए खालों का पुनर्निर्माण व चौड़ीकरण का काम भी युद्ध स्तर पर कर रही है। सूक्ष्म सिंचाई एवं नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण खरीफ और रबी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। इसमें विभाग कुशल एग्रोनोमिस्ट किसानों को बिजाई से लेकर भंडारा तक सभी नवीनतम कृषि गतिविधियों की जानकारी देते हैं।
सरकार साथ ही, पानी की बचत के लिए धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहन दे रही है। इससे लगभग 25-30 प्रतिशत पानी की बचत होती है। साथ ही, राज्य सरकार धान की सीधी बिजाई के लिए प्रति एकड़ 4,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देती है, जो पहले 5,000 रुपये थी। लेकिन शर्त यह थी कि किसान ढाई एकड़ में ही सीधी बिजाई कर प्रोत्साहन राशि का लाभ ले सकता था। अब इस शर्त को खत्म कर दिया गया है। इस बार राज्य सरकार ने एक लाख एकड़ में धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य रखा है। धान का कटोरा कहलाने वाले करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल सहित 12 जिलों को यह लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकायों/टैंकों के नवीनीकरण, पुन: उपयोग आदि पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा के सभी जिलों में पुनर्भरण संरचित, वाटरशेड विकास और गहन वनरोपण के माध्यम से जन भागीदारी और व्यापक अभियान के माध्यम से ‘वर्षा जहां और जब भी गिरती हो वही संरक्षित करो’ अभियान चलाया जा रहा है।
इसके अलावा, हरियाणा राज्य उप मृदा, जल संरक्षण अधिनियम-2009 बनाया गया है, जिसके तहत धान की नर्सरी की बुआई 15 मई से पहले और 15 जून से पहले धान की रोपाई प्रतिबंधित है। इस कानून के कारण खासतौर से धान वाले क्षेत्रों में भू-जल का दोहन रोकने में काफी सफलता मिली है। नई नीति के तहत किसान 20 मई के बाद धान की सीधी बिजाई और पारंपरिक तरीके से धान की रोपाई 15 जून के बाद कर सकते हैं। भावी पीढ़ी के लिए पानी बचाने हेतु राज्य सरकार ने ‘मेरा पानी, मेरी विरासत’ कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें धान की जगह मक्का, अरहर, काला चना, ग्वार, कपास, बाजरा जैसी कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। यही नहीं, संसाधन-संरक्षण प्रौद्योगिकियों जैसे कम जुताई, लेजर भूमि समतलन, अवशेष प्रतिधारण के साथ नो-टिलिंग, भूरा परिपक्वता, पत्ती रंग चार्ट के रूप में पोषक तत्व प्रबंधन उपकरण, एसपीएडी, ग्रीन सीकर के तहत गेहूं में ड्रिप सिंचाई के लिए किसानों को प्रेरित जा रहा है।

कृषि की अन्य संबद्ध गतिविधियों जैसे बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी, सिंचाई के विकास की दिशा में हरियाणा अग्रणी राज्य के तौर पर उभर रहा है। सरकार कृषि क्षेत्र में विविधीकरण को बढ़ावा तो दे ही रही है, अनुसंधान में सुधार के साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कृषि क्षेत्र में उभरते अवसरों का दोहन करने के लिए विकास प्रणाली और बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है।
जल प्रबंधन नीति
जल संरक्षण के लिए बांधों को मजबूत कर जल उपयोग दक्षता में सुधार करना होगा। भूमि समतलीकरण, खेतों की नालियों की सफाई, ढलान, मिट्टी की भौतिक स्थिति और जल निकासी, फसल की जरूरत के आधार पर सिंचाई से जल प्रबंधन को नया आयाम दिया जा सकता है। उद्योगों और सीवेज के पानी का पुनर्चक्रण कर इसका उपयोग सिंचाई में किया जा सकता है। साथ ही, वन रोपन में भी इसका प्रयोग हो सकता है। विश्व बैंक की सहायता से केंद्र सरकार ने राज्य में अटल भूजल योजना शुरू की है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य लक्षित क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने, परिस्थिति आधारित प्रबंधन और वित्तीय विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुसार भूजल प्रबंधन की स्थिति में सुधार करना है।
यह एक ग्राम पंचायत में सालाना कितना पानी उपलब्ध है, सालाना कितनी खपत है और शुद्ध शेष क्या है, इसकी स्पष्ट तस्वीर देगा। इसी तरह, जल शक्ति अभियान के तहत देश भर में जल संरक्षण आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके तहत जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकायों/टैंकों के नवीनीकरण, पुन: उपयोग आदि पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा के सभी जिलों में पुनर्भरण संरचित, वाटरशेड विकास और गहन वनरोपण के माध्यम से जन भागीदारी और व्यापक अभियान के माध्यम से ‘वर्षा जहां और जब भी गिरती हो वही संरक्षित करो’ अभियान चलाया जा रहा है।
(लेखक सूक्ष्म सिंचाई एवं नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पंचकूला के उप-निदेशक हैं।)









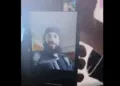


टिप्पणियाँ