अभी कुछ दिन पहले ही ‘देहरादून साहित्य महोत्सव’ संपन्न हुआ। इस तीन दिवसीय महोत्सव में अनेक विद्वानों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों ने अपने विचार रखे। महोत्सव के दूसरे दिन पाञ्चजन्य के संपादक हितेश शंकर और ‘ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इंडिया’ पुस्तक के लेखक सबरीश पी.ए. के बीच ‘भारत में विज्ञान का इतिहास’ पर चर्चा हुई। उस चर्चा के कुछ प्रमुख अंश यहां प्रस्तुत हैं—
गुरुकुल, पाठशाला जैसी भारतीय शिक्षा प्रणाली को इस्लामी आक्रमणकारियों और यूरोपीय/ब्रिटिश औपनिवेशिक संस्थाओं ने अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए नष्ट कर दिया। इस बारे में आपका क्या कहना है?
जब मैंने भारतीय विज्ञान के इतिहास को खंगालना शुरू किया तो देखा कि प्राचीनकाल से ही भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण था। इस्लामी आक्रमण और यूरोपीय उपनिवेशवाद जब चरम पर था, उस समय भी विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजों का सिलसिला जारी था। जब हम वैज्ञानिक खोज की बात करते हैं तो उसमें उस राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की बात भी शामिल रहती है जिसने प्राचीन और मध्यकालीन भारत में लोगों के लिए विज्ञान की बेहतर समझ का वातावरण तैयार किया था। आम लोगों में विज्ञान विषय की गहरी समझ निश्चित रूप से हमारी अनूठी शिक्षा प्रणाली ने ही विकसित की होगी जो वैदिक काल से भारत की विरासत का हिस्सा थी। यह ज्ञान परंपरा गुरुकुलों, आश्रमों, मठों के साथ- साथ तक्षशिला (गांधार ), बिहार के नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और तेल्हारा, शारदापीठ मंदिर विश्वविद्यालय (कश्मीर), वल्लभी (गुजरात), पुष्पगिरि (ओडिशा), सोमपुर, बिक्रमपुर और बंगाल में जगदला, मुरैना (मध्य प्रदेश), केथलूर साला (कीलाडी, तमिलनाडु) जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के माध्यम से आगे बढ़ती रही। ये उन शिक्षण संस्थानों में से हैं, जिन्हें बर्बरता से तबाह कर दिया गया।
धर्मपाल जी की एक पुस्तक है, ‘द ब्यूटीफुल ट्री’, जो अंग्रेजों की साजिश को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करती है कि उन्होंने व्यापक सर्वेक्षणों के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली की जानकारी इकट्ठी की और एक खास रणनीति के तहत नष्ट कर दिया। धर्मपाल जी ने शोध के लिए लंदन के ब्रिटिश अभिलेखागार में मौजूद सामग्री का अध्ययन किया जिससे यह पता चला कि अंग्रेज सर्वेक्षक और अधिकारी पूरे भारत में स्कूल स्तर पर प्रचलित 1750 के दशक में मौजूद असाधारण और बहु-विषयक स्वदेशी शिक्षा प्रणाली की उत्कृष्ट परंपरा से भली-भांति परिचित थे। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी, अवध, पंजाब, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर हर गांव के स्कूल स्थानीय व्यापारियों और संस्थाओं की सहायता से सुचारु तरीके से चलते थे, क्योंकि यह सर्वमान्य था कि स्थानीय चुनौतियों का समाधान ऐसे स्थानीय शिक्षा केंद्रों में उत्पन्न ज्ञान से ही हो सका है। अंग्रेजों को शासन करना था, इसलिए उन्होंने अन्यायपूर्ण करों और व्यापार नीतियों को थोप कर भारत की स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर अपनी विदेशी प्रणाली लागू कर दी जहां उनके अपने पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने लगे। इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीय जनता के दिमाग में यह बात भर दी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मूलत: यूरोपीय ज्ञान है और पूर्वी सभ्यताओं में मौजूद वैज्ञानिक विचार सारहीन और निरर्थक हैं।
मैकाले ने 2 फरवरी, 1835 को कहा, ‘वर्तमान में हमें एक ऐसा वर्ग बनाने की पूरी कोशिश करनी है जो हमारे और उन लाखों लोगों के बीच दुभाषिया का काम करे, जिन पर हम शासन कर रहे हैं। ये बस रक्त और रंग से भारतीय हों, लेकिन उनकी पसंद, आचार-विचार और बौद्धिकता में अंग्रेजी बसी हो। हम इस देश की स्थानीय बोलियों को परिष्कृत करने का काम उसी वर्ग पर छोड़ सकते हैं, जो उन बोलियों में मौजूद विज्ञान के मूल शब्दों को पश्चिमी नामों में बदलने का काम करें।’

प्राचीनकाल से ही भारत में गणित और खगोल विज्ञान संयुक्त रूप में विकसित हुए, दोनों में क्या समान है?
कोई भी ज्ञान प्रणाली चाहे वह वैज्ञानिक हो या सामाजिक प्रकृति की, समाज के सामने मौजूद चुनौती के समाधान के लिए विकसित होती है। कृषि और व्यापार के लिए मानसून के आगमन और महत्वपूर्ण मौसमों के आकलन के लिए खगोल विज्ञान की आवश्यकता थी, तो सटीक खगोलीय गणना के लिए गणित महत्वपूर्ण था। ‘ए ब्रीफ हिस्ट्री आॅफ साइंस इन इंडिया’ पुस्तक में भारतीय ज्ञान प्रणाली की बहु-विषयक प्रकृति के बारे में बताया गया है जो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित ज्ञान को समृद्ध करती रही है।
पुस्तक के आवरण पृष्ठ और अध्यायों में शल्यक्रिया, सुश्रुत, चरक और संबंधित ग्रंथों जैसे ‘सुश्रुत संहिता’ और ‘चरक संहिता’ की बार-बार चर्चा हुई है। आपने कावसजी नाम के एक पारसी सैनिक के बारे में भी जिक्र किया है जिसकी नाक टीपू सुल्तान ने 1793 में काट दी थी और कुमार नाम के पुणे के एक शल्यचिकित्सक ने उसकी चेहरे पर नई नाक लगा दी थी। भारत में पश्चिमी और यूरोपीय राष्ट्रों से पहले शल्य चिकित्सा का ज्ञान कैसे था?
आवरण पृष्ठ की वह तस्वीर लंदन की ‘जेंटलमैन्स मैगजीन’ से ली गई है, जिसमें 1794 में ‘ए सिंगुलर आॅपरेशन’ शीर्षक से कावसजी की तस्वीर को दर्शाया गया था, जिनकी वह शल्यक्रिया की गई थी। कावसजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत एक पारसी सिपाही थे, जिन्हें 1792 के एंग्लो मैसूर युद्ध में कैद कर लिया गया था। नाक की सफल शल्यक्रिया के बारे में मद्रास मेडिकल बोर्ड के मुख्य सर्जन कोली लियोन लुकान ने पहली बार 1793 में मद्रास गजट और बाद में ‘जेंटलमैन्स मैगजीन’ में रिपोर्ट की थी। इसके 20 साल बाद जोसेफ कॉन्सटेंटाइन कारपियु ने 1814 में इंग्लैंड में कावसजी की सर्जरी तकनीक, जो सुश्रुत संहिता से प्रेरित थी, पर आधारित नाक की पहली सर्जरी की। बाद में जर्मनी और यूएसए में वॉन ग्रेफ और जोनाथन मेसन वारेन ने क्रमश: 1816 और 1834 में पहली बार भारतीय तकनीक आधारित राइनोप्लास्टी की। इतिहासकार सर विलियम हंटर ने अपनी किताब, ‘सम एस्पेक्ट्स आॅफ हिंदू मेडिकल ट्रीटमेंट’ में कहा है, ‘सदियों पहले आधुनिक गया के पास नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय में हिंदू शल्यचिकित्सकों ने सफलतापूर्वक राइनोप्लास्टी और शल्य चिकित्सा के अन्य कौशल का प्रदर्शन किया था। प्राचीन हिंदू चिकित्सा ग्रंथों में शल्य चिकित्सा की ऐसी शाखा का वर्णन है जो विकृत कान और नाक को शल्यक्रिया से ठीक करने में सक्षम थी जिसे आज यूरोप के आधुनिक शहरों के नामचीन अस्पतालों में किया जा रहा है।’
आपकी पुस्तक में विजयनगर, मराठा, मैसूर साम्राज्यों में विकसित रॉकेटों का उल्लेख है जिसे बाद में अंग्रेजों ने ‘कांग्रेव रॉकेट्स’ के रूप में अपनाया था। क्या यह सच है कि भारत को रॉकेटों के बारे में जानकारी थी और इसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान किलों की रक्षा के लिए किया जाता था?
हां, भारत के पास रॉकेट बनाने की तकनीक थी। ‘आकाशभैरव कल्प’ जैसे भारतीय ग्रंथ में रॉकेट का उल्लेख है जिसे बाना, अग्निशास्त्र, अग्नि नलिका आदि कहा जाता था। 1563 में मुगलों के खिलाफ तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर की सेना ने रॉकेट इस्तेमाल किए थे। एक आक्रामक प्रक्षेपण हथियार के जरिए युद्ध में हावी होने के लिए मराठों और मुगलों ने रॉकेट का क्रमिक विकास किया। युद्ध में हाथियों और घोड़ों को डराने और दुश्मन की ताकत को कमजोर करने और विशेष रूप से किलों की रक्षा के लिए रॉकेट काफी प्रभावी थे। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना ने अफगान सेना के खिलाफ रॉकेट को एक शक्तिशाली हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जेम्स फोर्ब्स मराठों द्वारा 1775 में इस्तेमाल किए गए युद्ध रॉकेटों का वर्णन करता है जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा रखी थी। इसमें आठ से दस इंच लंबी और दो इंच व्यास की एक लोहे की ट्यूब होती थी जिसमें विस्फोटक से भरी बेलनाकार वस्तु को लोहे की छड़ या दोधारी तलवार या चार फीट से अधिक लंबी बांस की बेंत से बांधा जाता था। लोहे की नली के अंदर ज्वलनशील सामग्री भरी जाती और ऊपर सामने लोहे का नुकीला सिरा होता था जिसके कारण रॉकेट फायरिंग पर बड़ी तेज गति से प्रहार करता था और दुश्मनों को भयभीत कर देता था। मराठों ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों पर 940 मीटर से अधिक की मारक क्षमता वाले रॉकेट दागे थे। टीपू सुल्तान ने 1792 और 1799 में अंग्रेजों के खिलाफ श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में रॉकेटों को युद्धक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। फ्रांसीसी रॉकेट अंग्रेजी रॉकेट के सामने कमजोर पड़ गए थे, जबकि मैसूर रॉकेट अंग्रेजी सेना के लिए गंभीर चुनौती बन गए थे। विलियम कांग्रेव जूनियर ने मैसूर रॉकेटों का अध्ययन किया और कुछ बदलावों के साथ रॉकेट के एक नए स्वरूप, कांग्रेव रॉकेट, को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट और युद्ध सचिव के सामने प्रस्तुत किया। 1805 में लॉर्ड कैस्टर रेघ ने युद्ध में इसे इस्तेमाल करने का आदेश दिया। 1806 में अंग्रेजों ने जमीन और जल, दोनों ही युद्ध क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया। इसने 1806 में बोलोग्ने में नेपोलियन के साथ युद्ध में, 1807 में कोपेनहेगन पर और 1814 में वाटरलू की निर्णायक लड़ाई में अहम भूमिका निभाई।
आपने अपनी पुस्तक में एक विवादास्पद बात कही है कि ताजमहल हिंदू मंदिर की वास्तुकला पर आधारित है और इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने जयपुर के राजा जय सिंह से खरीदा था। क्या आप यह कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर स्थापत्य शैली की एक इमारत को एक मकबरा बना दिया गया?
ताजमहल का निर्माण भारत के पारंपरिक भवन सिद्धांतों, मेट्रोलॉजी और माप इकाइयों (अंगुलम) के आधार पर देशी भारतीय वास्तुकारों, शिल्पकारों, कारीगरों ने दिन-रात कड़ी मेहनत करके ग्रिड पैटर्न डिजाइन पर किया जो हड़प्पा सभ्यता के समय से प्रचलन में है। इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में भी किया गया है। दुर्भाग्य से, ताजमहल के बारे में वास्तविक और तथ्यात्मक जानकारी का भारी अभाव है और ठीक विपरीत इसके निर्माण संबंधी सामग्री, मूल निर्माणकर्ता और इतिहास के बारे में मनगढ़ंत दावे, नकली और जाली पांडुलिपियां ही ज्यादा प्रचारित हैं और लोग उसे ही सच मान कर बैठे हैं। ताजमहल के निर्माण में उपयोग की गई इंजीनियरिंग सामग्री में संगमरमर, र्इंटें, पत्थर, मिट्टी, मोर्टार, प्लास्टर, लकड़ी, धातु और कीमती पत्थर शामिल हैं। ताजमहल की दीवारों पर की गई पच्चीकारी मोजेक डिजाइन का एक रूप है। संगमरमर की दीवारों पर सुंदर पत्थरों की नक्काशी की गई है। मुगल बादशाह शाहजहां के महत्वपूर्ण अदालती दस्तावेज, बादशाहनामा से पता चलता है कि उसने 1632 में अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल, जिसकी मृत्यु 1631 में बुरहानपुर में हो चुकी थी, का मकबरा बनाने के लिए जयपुर के राजा जय सिंह के महल का अधिग्रहण किया था, जिसे आज हम आगरा का ताजमहल कहते हैं। राजा जय सिंह को यह महल अपने दादा राजा मान सिंह से पैतृक संपत्ति के रूप में विरासत में मिला था, जो मूलत: मंदिर वास्तुकला पर आधारित था। शाहजहां ने राजा जय सिंह से महल खरीद कर 1631 से 1653 ई. के बीच इसके मूल रूप को बदलकर इस्लामी स्वरूप देते हुए मकबरा बना दिया। इसकी मीनारें, नक्काशी और पच्चीकारी आदि बाद में बनीं।
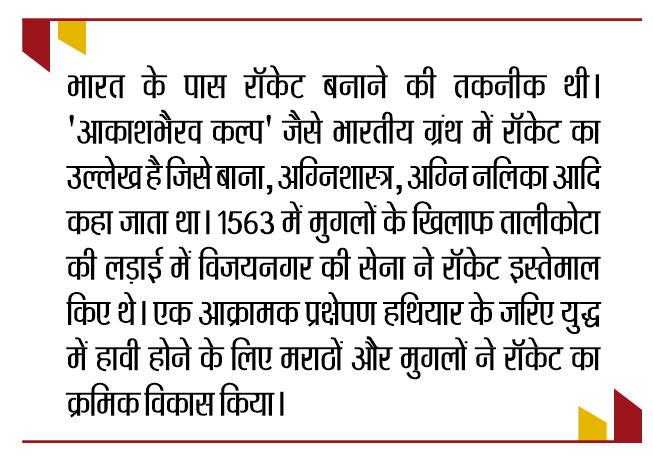
दिलचस्प बात है कि ताजमहल के उत्तरी द्वार के दरवाजे की लकड़ी के नमूने की कार्बन -14 डेटिंग वर्ष 1359 ईस्वी को दर्शाती है, यानी करीब 89 वर्ष का अंतर है। उस हिसाब से यह 1270 और 1448 ईस्वी के बीच के कालखंड में बना होगा। ताजमहल की स्थापत्य विशिष्टताएं कई ऐसे प्रतीकों को दर्शाती हैं जो शिव मंदिरों से मिलते हैं, पर इसकी पुष्टि इस भव्य मध्ययुगीन स्मारक के पुरातात्विक पुन: परीक्षण से ही संभव है। मेरी दलीलें मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि यह सब इंडियन इंस्टीट्यूट आॅफ साइंस की ‘करेंट साइंस’ जर्नल और आईएनएसए द्वारा प्रकाशित ‘इंडियन जर्नल फॉर द हिस्ट्री ऑफ साइंस’ के प्रकाशित शोध पत्रों में बताया गया है।
अब बात आत्मनिर्भर भारत और भारतीय विज्ञान प्रणाली की। हम कैसे आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं?
हमें अपनी भारतीय ज्ञान—परंपरा के कोश को आत्मसात करने की जरूरत है। हमें अपने पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति के बीच के संबंधों पर मंथन करना होगा और इस उद्देश्य को ‘भारतीय पुनर्जागरण’ जैसे व्यापक लक्ष्य का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले तो हमें स्वदेशी विज्ञान समेत अपने पारंपरिक ज्ञान कोश के उत्कृष्ट योगदान को स्वीकार और सम्मान करना होगा। साथ ही ज्ञान सृजन के वैकल्पिक तरीकों और मानकों यानी अनुसंधान पद्धति को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारतीय दर्शन बहुआयामी और विभिन्न धार्मिक विचारों पर आधारित होने के कारण सत्य तक पहुंचने की राह को व्यापक शोध क्षेत्र उपलब्ध करा सुगम बनाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि शोधार्थी और वैज्ञानिक सांख्य और न्याय दर्शन आधारित शोध पद्धतियों को अपनाना शुरू करें।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान—परंपरा, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कितनी महत्वपूर्ण है?
भारत का इतिहास और उसकी गौरवशाली विरासत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की उपलब्धियों की बात किए बिना अधूरी है। अत: यह पुस्तक उस अंतर को पाटने की कोशिश करती है और इसे ऐसे ढंग से तैयार किया गया है कि यह किसी भी सामान्य पाठक से लेकर शिक्षाविदों और शोधार्थियों, सबके लिए उपयोगी है। इसमें विभिन्न अवधारणाओं, तथ्यों और आंकड़ों, दार्शनिक व्याख्या से लेकर विभिन्न आयामों का ध्यान रखा गया है।


















टिप्पणियाँ