वह बुढ़िया पार्टी सोई हुई थी। उसके भाग्यविधाता भी नींद में थे, लेकिन सपने में अरब की क्रांति आती है। जब बीच-बीच में आंखें खुलतीं तो सपने की उसी क्रांति का अक्स सामने आ खड़ा होता। शाहीन बाग में वैसा ही कुछ दिखा था, लेकिन जब आंखें खुली तो वैसा कुछ नहीं था। सपना पता चलने पर फिर चादर तान ली। लेकिन उनींदी अवस्था में भी वह चलती रही और संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई।
एक तरफ जहां चाइनीज वायरस से दुनिया हिली, वहीं कुछ लोगों के लिए यह सत्ता-संसाधन हासिल करने का खेल बना। कांग्रेस लंबे समय से सो रही थी। कोरोना आने पर वह अचानक जागती है। सोनिया आर्इं तो उन्होंने कहा कि मीडिया के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। राहुल आए तो उन्होंने कहा कि ये अब आपके खाने के चावल से सैनेटाइजर बनाएंगे। ये धूर्तता वाली, लोगों को उकसाने वाली बात तो है ही, अपूर्ण भी है। इसके बाद एक ट्विटर ट्रेंड चला #WHO_With_Rahul … 14 जनवरी को डब्ल्यूएचओ का जो ट्वीट था, वह लोगों को गुमराह करने वाला था कि यह वायरस इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता। राहुल गांधी ने जब कहा कि तुम्हारे खाने के चावल से ये लोग अमीरों के हाथ धोने के लिए सैनेटाइजर बनाएंगे, तो यह भी धूर्ततापूर्ण था क्योंकि भारत में खाद्यान से गोदाम भरे हुए हैं। साल-डेढ़ साल का अनाज हमारे पास है। और फिर बचत होती क्यों है? गाढ़े समय में काम आने के लिए।
ख्वाबों की उसी रूमानी क्रांति को हकीकत में बदलने वाले एक और आयाम की बात। भारत में वायरस का संक्रमण बहुत हद तक काबू में हो जाता अगर जमात के मरकज से ये नहीं फैलता। मगर कथित ‘सेकुलर’ का सबसे बड़ा दांव यह है कि एक जमात की गलती होने के बावजूद ‘इस्लामाफोब’ ठहरा देना। अब जब उन्होंने यह शब्द गढ़ ही दिया है तो देखना होगा कि यह सोच उन्होंने पाई कहां से। कहीं ये उनका ‘काफिरोफोबिया’ तो नहीं! ये लोग अपने मत-मजहब, अपनी राय, अपने राजनैतिक रुझान को ठीक मानते हैं और इससे इतर बाकी सब लोगों ‘काफिर’ हैं। जो इस्लामोफोबिया के नाम से समाज में जहर घोल रहे हैं, वे चाहते हैं कि मजहब कट्टरपंथियों के हाथों में बंधक बना रहे।
जो सत्ता में नहीं होता वह आक्रोश को अपने हित में भुनाना चाहता है। इसीलिए जब दूसरे राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार होता है तो कांग्रेस को दिखता है। लेकिन यह सब उसके राज्य में होने पर वह आंखें मूंद लेती है। अखलाक की हत्या उसे दिखती है, लेकिन रूपेश पांडेय की हत्या और लावण्या का दर्द पर वह मौन हो जाती है। आक्रोश को रोकने के लिए यदि प्रशासनिक सख्ती होती है तो इसे दोगुने वेग से भड़काया जा सकता है। लोग किन परिस्थितियों में हिंसाचार पर उतर सकते हैं, राजनीतिक दल बखूबी जानते हैं। कोरोना त्रासदी से ठीक पहले दिल्ली दंगों में हम सबने यह देखा है। लाशों पर राजनीति करने वाले, आक्रोश पर राजनीति करने वाले हमेशा ताक में रहते हैं।
प्रशासनिक अमले पर हमला, टोंक जैसी घटना में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाना, डॉक्टरों से दुर्व्यवहार और क्वारंटाइन केंद्र की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करना, ये सब दरअसल चालें हैं। ये चालें हैं आक्रोश को अराजकता में बदलने और उस आक्रोश को सीधे-सीधे लोगों की परेशानी से जोड़ने की। यानी लोगों को भड़काना, उन्हें राज्य या देश के खिलाफ खड़ा करना, हिंसाचार पर उतारू करना और फिर बताना कि यह मजलूम और पीड़ितों की आवाज है, जिसे दबाया जा रहा है। इस राजनीति की तुरंत काट करना जरूरी है, वरना भारत एक संकट से गुजरते हुए दूसरे बड़े संकट में धंस सकता है।

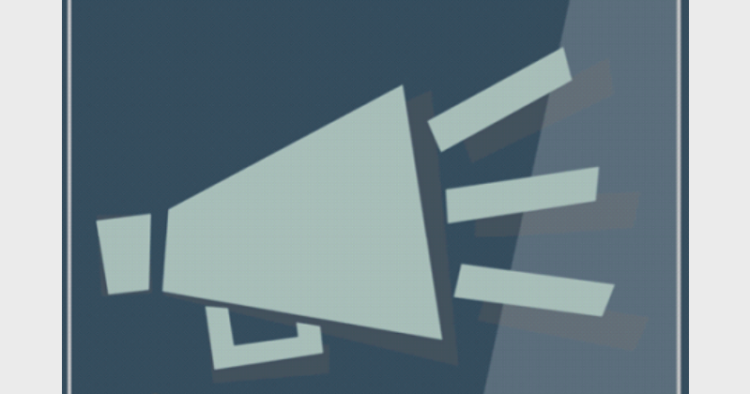









टिप्पणियाँ