कचरे से संवार रहीं जीवन

असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास बोसागांव की रूपज्योति सैकिया गोगोई प्लास्टिक कचरे का बेहतरीन प्रयोग कर दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही हैं। रूपज्योति राष्ट्रीय उद्यान के आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को लेकर चिंतित थीं। वे चाहती थीं कि जंगल साफ-सुथरा रहे और जानवरों को इससे कोई नुकसान न हो। उनका कहना है कि प्लास्टिक को जलाने से वायु प्रदूषण भी होता है। इसलिए 48 वर्षीया रूपज्योति ने पहले प्लास्टिक से सामान बनाने की प्रक्रिया सीखी। इसके बाद 2004 में पॉलीथिन और प्लास्टिक की बोतलों से धागा, हैंडबैग, पायदान, चटाई व अन्य सजावटी सामान बनाने लगीं। इससे राष्ट्रीय उद्यान के आसपास से कचरा तो साफ हुआ ही, दूसरी महिलाओं को काम भी मिला। इसके बाद वे गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण भी देने लगीं। वे अब तक 35 से अधिक गांवों के लोगों को रोजगार व करीब 2500 महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। उनके साथ जुड़ी महिलाएं अच्छी-खासी कमाई कर रही हैं। इसके अलावा, रूपज्योति ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए 2012 में काजीरंगा हाट भी शुरू किया। आजकल वे डिजिटल माध्यम से अपने उत्पादों को देश-दुनिया में आॅनलाइन बेच रही हैं।
दो बहनों ने खड़ा किया ब्रांड

पश्चिम बंगाल की तान्या बिस्वास और सुजाता बिस्वास सगी बहनें हैं। दोनों इंजीनियरिंग व एमबीए की पढ़ाई के बाद अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रही थीं, पर उनके मन में कुछ अलग करने की इच्छा थी। लिहाजा नौकरी छोड़ 2016 में कंपनी बनाई व साड़ियों का कारोबार शुरू किया। इसके लिए उन्होंने बाकायदा शोध किया। हालांकि महिलाओं में साड़ियों का चलन कम हो रहा था। इस क्षेत्र में पहले से ही बड़े ब्रांड थे, पर उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया व सभी उम्र की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए आकर्षक साड़ियां बनाने लगीं। शुरू में दो बुनकरों को साथ जोड़ा और सूती साड़ी को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड सुता नाम से एक एप बनाया। चूंकि पैसे नहीं थे, इसलिए खुद ही मॉडल बनीं और सोशल मीडिया के जरिये प्रचार की बागडोर भी संभाली। महज तीन लाख रु. से शुरू किया गया उनका कारोबार 13 करोड़ रुपये के पार चला गया है। आज उनके पास 1500 से अधिक बुनकर हैं। कंपनी की दो हथकरघा इकाइयां भी हैं। ब्रांड सुता के जरिये वे सामान्य साड़ी को डिजाइनर साड़ी में बदल कर सूती साड़ियों की शौकीन महिलाओं तक पहुंचाती हैं। साथ ही, बंगाल के बुनकरों की स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही हैं और उनके द्वारा निर्मित साड़ियों को प्रोत्साहन देती हैं।
पहले परिवार संभाला, फिर दूसरों का सहारा बनीं

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के रानापार गांव की गीतारानी के पति दिनेश यादव महाराष्ट्र में फर्नीचर की दुकान पर काम करते थे। लेकिन कोरोना की पहली लहर में उनकी नौकरी छूट गई। परिवार आर्थिक मुसीबत में फंस गया तो गीतारानी ने मोर्चा संभाला। वे गांव के एक महिला स्वयंसहायता समूह से जुड़ गईं और लॉकडाउन के दौरान मास्क बनाए और उन्हें ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को उपलब्ध कराया। इसके बाद उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म की सिलाई का काम मिला, जिससे उनकी और समूह से जुड़ी महिलाओं को अच्छी कमाई हुई। इसी दौरान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के खंड प्रबंधक से पता चला कि राज्य सरकार बाहर से लौटने वाले श्रमिकों को समूह के जरिये स्वरोजगार उपलब्ध करा रही है। गीतारानी ने अधिकारियों से संपर्क कर बैंक से दो लाख रुपये का कर्ज लिया और बरही गांव के बाजार में चंदा एसएचजी इंटरप्राइजेज नाम से पति की फर्नीचर की दुकान खुलवा दी। अभी उनके पति न केवल इलाके के प्रतिष्ठित फर्नीचर की दुकान के मालिक हैं, बल्कि अन्य समूहों को अपने उत्पाद भी बेच रहे हैं। उन्होंने दुकान पर दो लोगों को रोजगार भी दिया है। गीतारानी की आर्थिक स्थिति सुधरी तो वे संकट काल में गांव के लोगों की मदद करने लगीं। उन्होंने गरीब महिलाओं को निशुल्क मास्क और साबुन बांटे। इससे समूह से जुड़ी दूसरी महिलाओं का भी उत्साह बढ़ा। आज गीतारानी गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे रही हैं। वे कहती हैं कि घर का खर्च चलाने और पति को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम रंग लाई। अब उनके पति को काम के लिए दिल्ली-मुंबई नहीं जाना पड़ेगा।
एक फ्रॉक ने बना दिया कारोबारी

लखनऊ की 35 वर्षीया तरिषी जैन आर्किटेक्ट हैं और पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करती थीं। करीब 5 साल पहले उन्होंने घर से हैंडमेड किड्स वियर का काम शुरू किया। आज वे छोटे बच्चों के लिए हाथ से बुने स्वेटर और फैन्सी पोशाकों की ‘अजूबा’ नाम से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित देशभर में आॅनलाइन मार्केटिंग कर रही हैं। उन्होंने 250 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं। पिछले साल उनकी कंपनी का करोबार 2 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। दरअसल, 2014 में तरिषी गर्भवती हुर्इं तो पति के पास अमदाबाद आ गर्इं। 2015 में एक बच्ची को जन्म दिया तो सास ने उसके लिए एक फ्रॉक बनाई। बकौल तरिषी, फ्रॉक अलग हटकर और बहुत सुंदर थी। उन्होंने फ्रॉक में बेटी की फोटो व्हाट्सएप पर लगाई तो दोस्तों ने अपने बच्चों के लिए इसी तरह की फ्रॉक की फरमाइश कर दी। तब तक उनके दिमाग में व्यापार का कोई विचार नहीं था। फ्रॉक बनाने के लिए उन्होंने सास से सिलाई सीखी और कुछ फ्रॉक बनाकर दोस्तों को उपहार स्वरूप दे दीं। लेकिन दोस्तों के परिचित और रिश्तेदार भी उसी तरह की पोशाक की मांग करने लगे। कुछ लोगों ने तो पैसे भी पहले दे दिए। तब जाकर तरिषी ने इस काम को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। लेकिन अकेले यह सब संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका की मदद ली। इस तरह, उन्होंने पहली खेप का आॅर्डर पूरा किया। बाद में उन्होंने सिलाई-बुनाई में पारंगत तीन अन्य महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। आज वे पति के साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं।
जोखिम आया रास

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की 26 वर्षीया प्राची भाटिया ने करीब चार साल पहले घर सजाने वाले रचनात्मक उत्पाद बेचने के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया था। 2017 में प्रोडक्ट डिजाइनिंग में स्नातक प्राची ने इन उत्पादों की डिजाइनिंग और देशभर में मार्केटिंग की हैं। 2020 में उनकी कंपनी का सालाना कारोबार 14 लाख रुपये पहुंच गया। प्राची शुरू से ही आत्मनिर्भर बनना चाहती थीं, इसलिए पढ़ाई के दौरान ही एक कंपनी में काम शुरू कर दिया था। पहली ही नौकरी के दौरान वे स्टार्टअप शुरू होना चाहती थीं, लेकिन उनकी और घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे कोई जोखिम ले सकें। लिहाजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2018 में वे दूसरी कंपनी में काम करने लगीं। हालांकि वेतन अच्छा था, लेकिन वहां उनके साथ लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था। हालांकि काफी हद तक उन पर घर की जिम्मेदारी थी, इसके बावजूद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और एक लाख रुपये से अपना स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने 5-6 उत्पादों के डिजाइन बनाकर स्थानीय निर्माताओं से उसे तैयार कराया। इनमें अधिकतर रसोई में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद थे। सभी बिल्कुल अलग, रचनात्मक और कम दाम के थे। उत्पाद तैयार होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी मार्केटिंग शुरू की। धीरे-धीरे उनके उत्पादों की मांग बढ़ती गई। वर्तमान में प्राची अपने 70 उत्पादों की देशभर में आपूर्ति कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने पांच बड़ी कूरियर कंपनियों के साथ समझौता किया है, जो उनके उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। उन्होंने पांच लोगों को नौकरी पर रखा है और कुछ प्रशिक्षुओं को भी अवसर दे रही हैं।
नए अंदाज में परंपरागत आभूषण

हंसिका जेठियानी और स्टीवन झांगियानी ने दिसंबर 2020 में ‘फंकी महारानी’ नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया। सिंगापुर में रहने वाले स्टीवन वैसे परंपरागत भारतीय आभूषणों को नए रूप में तैयार कर बेचते हैं, जिन्हें भुला दिया गया। एक दिन स्टीवन की निगाह अपनी पत्नी सपना झांगियानी के मांग टीका पर पड़ी, जिसे उन्होंने एक विवाह में पहना था। इसके बाद से वह ऐसे ही रखा हुआ था। यह देखकर स्टीवन के मन में विचार आया कि क्यों न मांग टीके को नए अंदाज में प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद उन्होंने अपने काम की शुरुआत की और इसमें मुंबई में रहने वाली अपनी चचेरी बहन हंसिका जेठानी को साझीदार बनाया। हंसिका लंदन स्थित यूनिवर्सिटी आॅफ आर्ट्स से स्नातक हैं। इस काम को ठीक से अंजाम देने के लिए उन्होंने फ्रीलांसर ज्वेलरी डिजाइनर के साथ कुछ समय तक काम किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर सूरत के कुछ कारीगरों को अपने साथ लिया और मांगटीका, झुमका व पायल को कई रूपों में बाजार में उतारा। इनमें अधिकतर रिसाइकिल किए गए पीतल से बने हुए हैं। हंसिका बताती हैं कि करीब आठ महीने में उन्होंने 52 मांगटीके बेचे मुंबई और गोवा के कुछ पॉपअप स्टोर में ऐसे उत्पादों की काफी मांग है। खासतौर से गोवा का नाइट मार्केट ऐसे गहनों के लिए सबसे अच्छी जगह है। स्टीवन कहते हैं कि हालांकि वे भारत में नहीं पले-बढ़े, लेकिन यहां की संस्कृति के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा है। उनकी कंपनी के 80 प्रतिशत उत्पाद गुजरात के स्थानीय कारीगर रिसाइकिल पीतल से दस्तकारी कर तैयार करते हैं। वे कहते हैं कि उनका उद्देश्य धातु के कचरे को कम करना और पर्यावरण की रक्षा करना है।
विदेश की नौकरी छोड़ बनाई पहचान

राजस्थान की अंकिता कुमावत आईआईएम कोलकाता से पढ़ाई कर अमेरिका में अच्छी नौकरी कर रही थीं। लेकिन 5 साल जर्मनी और अमेरिका में रहने के बाद पिता के बुलाने पर 2014 में सब कुछ छोड़कर अजमेर लौट आर्इं। यहां गांव में पिता के साथ खेती और डेयरी फार्मिंग का काम शुरू किया। वे जैविक खेती और खाद्य प्रसंस्करण के काम से सालाना करीब एक करोड़ रुपये का कारोबार कर रही हैं। उनके पास 50 गायें हैं और वे 24 से अधिक उत्पाद बनाती हैं। साथ ही, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 100 लोगों को रोजगार भी दिया है। दरअसल, जब अंकिता की नौकरी लगी तो पिता ने नौकरी छोड़ दी और परिवार के लिए खेती करने लगे और गाय भी रख ली। धीरे-धीरे जब गायों की संख्या बढ़ी तो उन्होंने आसपास के लोगों को दूध बेचना शुरू किया। जब अंकिता वापस आर्इं तो उन्होंने नई तकनीक पर जोर दिया। साथ ही, सौर ऊर्जा से सिंचाई की बूंद-बूंद तकनीक अपनाई और खेती का दायरा बढ़ाने के साथ गायों की संख्या भी बढ़ाई। खुद कई संस्थानों से प्रशिक्षण भी लिया। इसके बाद उन्होंने प्रसंस्करण इकाई भी लगा ली। चाहे दुग्ध उत्पाद हों या सब्जियां, अंकिता अपने हर उत्पाद की शुद्धता का पूरा ध्यान रखती हैं। वे घी, मिठाइयां, शहद, नमकीन, ड्राई फ्रूट, मसाले, दाल जैसे उत्पाद तैयार करती हैं। काम बढ़ा तो मंडियों पर निर्भरता मुनासिब नहीं लगी, इसलिए उन्होंने अपने उत्पाद को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और आॅनलाइन मंचों का सहारा लिया। फिर ‘मातृत्व’ नाम से अपनी वेबसाइट बनाई और देशभर में अपने उत्पादों की आपूर्ति करने लगीं। इससे उनका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा।
बांस की चाय ने दिलाई फॉर्ब्स सूची में जगह
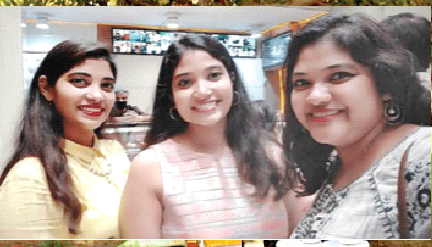
दिल्ली की तीन बहनों तरुश्री, अक्षया और ध्वनि का ‘शिल्पकारमैन’ नाम से स्टार्टअप है, जिसे उन्होंने 2017 में शुरू किया था। तरु क्लिनिकल साइकोलॉजी में परास्नातक, अक्षया बिजनेस इन इकोनॉमिक्स और ध्वनि ने फिल्म निर्माण की पढ़ाई की है। शुरुआत में तरु बांस से बने रोजमर्रा से लेकर रसोई तक में प्रयुक्त होने वाले हस्तशिल्प उत्पाद का कारोबार करती थीं। बाद में दोनों बहनें भी उनके साथ जुड़ गर्इं। अपने उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने देश-विदेश में कई प्रदर्शनियों में भी हिस्सा लिया। फिर विभिन्न आॅनलाइन मंचों के जरिये उत्पादों की बिक्री करने लगीं। 2019 में पढ़ाई पूरी कर छोटी बहन ध्वनि जब साथ जुड़ीं तो उन्होंने बांस की पत्तियों से बनी चाय का व्यापार शुरू करने का सुझाव दिया। काफी शोध के बाद पता चला कि विदेशों में बांस की पत्तियों का प्रयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है। इसमें प्रोटीन, सिलिका, जिंक सहित कई पोषक तत्व होते हैं। 2020 में इन्होंने विभिन्न प्रकार के बांस की पत्तियों का प्रसंस्करण कर चाय बनाना शुरू किया। इन्होंने अपने साथ पूर्वोत्तर के राज्यों के स्थानीय कलाकारों को अपने साथ जोड़ा, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। आज उनके साथ 500 से अधिक कारीगर जुड़े हुए हैं और इनके उत्पादों की मांग भारत ही नहीं, विदेशों में भी है। 2020 में इनका कारोबार सालाना 7 लाख रुपये था, जिसे 2021 में इन्होंने 25 लाख रुपये करने का लक्ष्य रखा था। 2021 में फोर्ब्स पत्रिका ने अपनी सूची में उनका नाम शामिल किया था। उनके उत्पादों में फर्नीचर, लैपटॉप स्टैंड, कलम, ब्रश के अलावा रसोई में प्रयुक्त होने वाले सभी उत्पाद शामिल हैं।
मशरूम ने 20,000 वनवासियों को बनाया आत्मनिर्भर

बिहार के बांका जिले के झिरवा गांव की विनीता एक सामान्य गृहिणी हैं, जिन्हें सिलाई-कढ़ाई से लेकर अन्य हुनर भी आते हैं। लेकिन उनके लिए इतना ही काफी नहीं था। वे कुछ अलग करना चाहती थीं, इसलिए शादी के चार साल बाद 2012 में अपने घर से 300 किलोमीटर दूर डॉ. राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर से मशरूम की खेती का प्रशिक्षण लिया। तमाम परेशानियों के बावजूद वे रोज ट्रेन से पूसा जाती थीं। प्रशिक्षण के बाद महज पांच बैग से मशरूम की खेती करने वाली विनीता की पहचान आज राज्य में ‘किसान दीदी’ की बन गई है। यही नहीं, उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उनकी लगन को देख कृषि विश्वविद्यालय ने उन्हें दूसरे लोगों को भी प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद भी रातभर ट्रेन की यात्रा कर वे पूसा जातीं रहीं और करीब 400 लोगों को प्रशिक्षण दिया। अब तक वे करीब 20,000 से अधिक वनवासियों को प्रशिक्षण दे चुकी है और पूरे इलाके को मशरूम का केंद्र बना दिया है। खुद विनीता मशरूम की खेती कर हर माह कम से कम 50,000 रुपये कमा लेती हैं। बिहार सरकार की ओर से उन्हें 15 लाख रुपए का अनुदान मिला, जिससे उन्होंने तमाम उपकरण खरीदे और अपने घर पर ही प्रयोगशाला बनाई। विनीता अब पूरे जिले में मशरूम और इसके लिए खाद खुद तैयार करती हैं और किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ खाद-बीज भी उपलब्ध कराती हैं। अपनी मेहनत और लगन से सूबे की महिलाओं में नई उर्जा का संचार करने वाली विनीता बताती हैं कि झिरवा में रोजाना 50 किलो से लेकर 2 क्विंटल तक मशरूम उत्पादन होता है। इससे लोगों को लाखों रुपये की कमाई होती है और उनका गांव भी आत्मनिर्भर हो गया है।
ई-कचरे के विरुद्ध नागालैंड की दो महिलाओं का ‘युद्ध’

(दाएं से दूसरी)
नागालैंड के दीमापुर की दो महिलाएं सोवेते.के. लेट्रो और बेंदांगवाला वॉलिंग ई-कचरे के विरुद्ध ‘युद्ध’ लड़ रही हैं। उन्होंने 2018 में ई-सर्किल नाम से नागालैंड का पहला ई-कचरा संग्रह केंद्र स्थापित किया। 27 वर्षीया लेट्रो बचपन से ही यह सोच कर ई-कचरा इकट्ठा करती थीं कि भविष्य में इनका फिर से उपयोग किया जा सकता है। दोनों ने पंजाब विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। लेट्रो ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, जबकि वॉलिंग सोशल वर्क में परास्नातक हैं। पढ़ाई के दौरान चंडीगढ़ में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर शोध करते हुए उन्हें इसे पेशा बनाने की प्रेरणा मिली। इसके बाद दोनों ने एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ शिलांग में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप की, जो नगरपालिका के ठोस कचरे का निपटान करती है। इंटर्नशिप पूरा करने के बाद दोनों ने कचरा प्रबंधन पर शोध किया और खासतौर से ई-कचरे पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर ई-कचरा उपलब्ध हैं, जिनका निपटान आसान नहीं है। पूरे नागालैंड में 30 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ उन्होंने दीमापुर के कई स्कूलों, दुकानों और कार्यालयों में ई-कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था की है। साथ ही, ई-कचरे से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। शुरुआत में दोनों घर-घर, कार्यालयों, स्कूलों और संस्थानों में जातीं और उनसे ई-कचरा मांगती थीं। बदले में थोड़े पैसे और ई-कचरा दान प्रमाण-पत्र देती थीं। 2018 में ई-सर्किल ने 20 टन कचरा कोलकाता भेजा। आज उनकी कंपनी देश के 14 राज्यों और 18 शहरों में सक्रिय है। दीमापुर के अलावा, पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य त्रिपुरा में अगरतला और शिलांग, मेघालय में भी उनके साझीदार हैं।

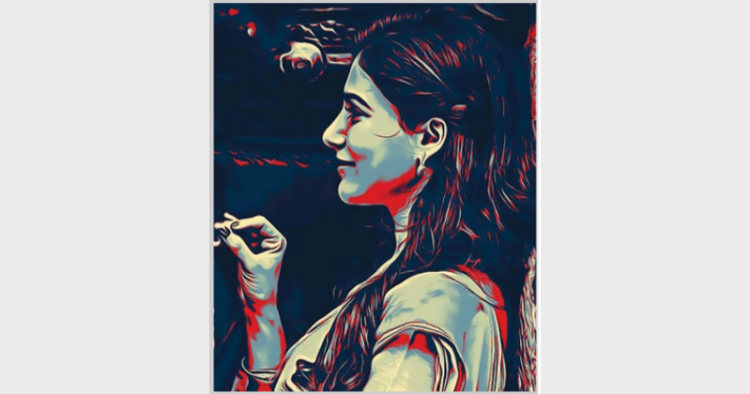








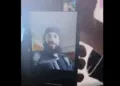

टिप्पणियाँ