ज्ञान की अपनी एक यात्रा होती है। जब कोई ज्ञान-विशेष व्यवहार की कसौटी पर बार-बार कसने पर एक ही परिणाम दे तो वह सूत्रबद्ध हो जाता है। आज जितने तरह के विज्ञान हमारे अध्ययन का हिस्सा हैं, सब में ऐसे ही व्यवहार-सिद्ध प्रमेय और सूत्र हैं। आम बोलचाल में हम इन्हें लीक भी कह सकते हैं। गिनती के लोग होते हैं जो लीक बनाते हैं, बाकी उसपर चलते हैं। श्रीपद ए. दाभोलकर को उन चंद लोगों में गिना जा सकता है, जिन्होंने लीक बनाई। पूरी तार्किकता और वैज्ञानिकता के साथ। आज दाभोलकर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जीवन के विभिन्न आयामों के लिए ज्ञान को सूत्रबद्ध करने के उनके कुछ प्रयासों का संकलन ‘प्लेंटी फॉर आॅल’ नाम की पुस्तक हमारे बीच है।
आज के कोरोना काल में हम जानते हैं कि गांवों ने हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरह रसातल में जाने से बचाया। उसके बाद ही देश की नीतियों में गांवों को और मजबूती के साथ अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाने की कोशिश हो रही है। दाभोलकर ने न केवल दशकों पहले वैश्विक, खास तौर पर भारत में गरीबी को दूर करने में गांवों को एक अभिन्न कड़ी के रूप में देखा बल्कि इसके लिए प्रयोग आधारित सूत्र भी सुझाए। बाद में अपने कुछ अनुभवों को 1998 में पुस्तक के रूप में संकलित भी किया।
अंग्रेजी में लिखी इस पुस्तक की प्रस्तावना ऋग्वेद के इस श्लोक से शुरू होती है-‘विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् अनातुरम्’। अर्थात् जिस तरह विश्व अपने आप में परिपूर्ण है, गांव भी उतने ही समर्थ-सक्षम और सर्व-संपन्न बनें। अगर यह हुआ तो पूरी दुनिया गरीबी से मुक्त हो जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि इसकी मशाल किसके हाथ में होगी? दाभोलकर कहते हैं कि यह तो स्थानीय लोगों के ही हाथ में होगी और यह मशाल पारंपरिक ज्ञान की लौ से प्रज्जवलित होगी। लेकिन वैश्विक समस्याओं के समाधान में इस स्थानीय ज्ञान, किसी सुदूर क्षेत्र में अपनी धुन में लगे किसी व्यक्ति के प्रयोगों की भी भूमिका है, यह पुस्तक इस बात को स्थापित करती है।
आजादी के बाद का दौर था। दाभोलकर विभिन्न संस्थागत गतिविधियों, शिक्षण और प्रशिक्षण से ग्रामीण जीवन में बदलाव करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए कई प्रयास किए लेकिन उन्हें जल्दी ही इस बात का अहसास हो गया कि व्यवस्था में स्थापित निर्धारित पाठ्यक्रम किसी भी रचनात्मकता और मौलिकता को हतोत्साहित करने वाले थे। इसी बीच सांस्थानिक शैक्षणिक कार्यक्रमों के जरिये ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने के लिए भारत सरकार की ओर से खोले गए 14 ग्रामीण संस्थान अपने उद्देश्यों को पाने में विफल हो चुके थे और स्थिति ऐसी थी कि शिक्षा पर कोठारी आयोग की रिपोर्ट में ग्रामीण विश्वविद्यालय के विचार को भुला दिया जा चुका था। ज्ञान को जन-जन तक पहुंचाने में सांस्थानिक शिक्षण की कमियों ने दाभोलकर को प्रेरित किया कि वे शिक्षण-प्रशिक्षण की गैर-सांस्थानिक शृंखला विकसित करें।
दाभोलकर को बचपन से ही पेड़-पौधों, फसलों-वनस्पतियों के साथ प्रयोग करना अच्छा लगता था इसलिए उनका खेती-किसानी का जो भी अनुभव था, वह प्रयोग सिद्ध था। उनके अनौपचारिक शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्र आसपास के क्षेत्रों में नए तौर-तरीकों का ज्ञान फैलाने की प्रयोगशाला बन गए। उनके प्रयोगों का लाभ जन-जन को मिले, इसके लिए दाभोलकर ने हमेशा खुद को बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में रहते हुए अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता व्यक्ति मानकर प्रयोग किए। उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि अगर खेती को ऐसा बनाना है जिससे किसान का पेट भर सके, उसकी जरूरतें पूरी हो सके तो इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों को लाना होगा और इसके लिए जरूरी था कि भारत जैसे विकासशील देश में विज्ञान की नई सामाजिकता विकसित हो। इसमें उनके ‘प्रयोग परिवार’ की अवधारणा काफी सफल रही। दाभोलकर ने पुस्तक में लिखा है कि कैसे ‘किर्लोस्कर’ पत्रिका में नियमित रूप से उनके प्रयोग प्रकाशित होने लगे जो खेती-किसानी, मुर्गी पालन, पशुपालन जैसी ग्रामीण जीवन की विभिन्न गतिविधियों से जुड़े थे। कुछ ही समय में उनके पास देशभर से लोगों की चिट्ठियां आने लगीं। कई लोग कहते कि उनके प्रयोग को आजमाया और परिणाम वैसे ही आए तो कई ने लिखा कि आप जो उपाय बता रहे हैं, वह तो हम पहले से ही करते रहे हैं। अब दाभोलकर अपने प्रयोगों के अतिरिक्त एक जगह के लोगों के अनुभव सिद्ध सूत्रों को दूसरे इलाके के लोगों को भेजने लगे। व्यवहार-सिद्ध ज्ञान के परस्पर आदान-प्रदान की इस पूरी शृंखला को दाभोलकर ‘प्रयोग परिवार’ कहते हैं।
उन्होंने पुस्तक में ऐसे विभिन्न उदाहरण दिए हैं जिनमें चंद किसानों या उत्पादकों के प्रयोग से निकली विधि ने एक बड़े समुदाय के लिए सफलता के दरवाजे खोले। जैसे महाराष्ट्र के सांगली जिले में अंगूर उत्पादकों के समूह ‘वैज्ञानिक द्राक्षाकुल’की बात। वर्ष 1974 में यह महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले 20 पढ़े-लिखे लोगो का एक समूह था। यह समूह अंगूर की खेती के विभिन्न चरणों में नई तकनीकों को आजमाता और व्यवहार-सिद्ध परिणामों को सूत्रबद्ध करता। आठ साल में ही यह समूह देश में अंगूर उत्पादन की जानकारी के मामले में अग्रणी हो गया, यहां तक कि विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से भी उत्कृष्ट।
वैसे ही पपीता और मुर्गीपालन का संबंध आंखें खोलने वाला है। जो लोग मुर्गीपालन के क्षेत्र में हैं, वे जानते हैं कि चूजों से लेकर मुर्गे तक के लिए दाने का इंतजाम करने में कितना खर्च करना पड़ता है। दाभोलकर ने अनुसंधान और प्रयोग से पाया कि एक मुर्गे के लिए रोजाना 120 ग्राम पपीते पर्याप्त है। पपीता का एक पेड़ साल भर में इतने फल दे देता है जिससे चार मुर्गियों के खाने का इंतजाम हो सके और जो अंडे दे सकें। पपीते की जगह जिमीकंद का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे यहां बरसात के दिनों में जिमीकंद तैयार होता है और इसे बड़ी आसानी से सालभर रखा जा सकता है। इसमें वसा, कैल्शियम, फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में होते हैं। हां, इसमें प्रोटीन की कमी को हरी पत्तियों, पक्षियों के मल, मछलियों के दाने वगैरह से पूरा किया जा सकता है। पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अक्सर ज्यादा दूध देने वाली गायों का खास ध्यान रखना पड़ता है। पशुपालकों में यह बात आम है कि अगर रोजाना दूध की मात्रा में 1-2 लीटर की वृद्धि करनी है तो इसके लिए बिटीरेट, ऐसीटेट समेत कुछ अन्य एसेन्शियल आॅयल की गोलियां देनी पड़ती हैं। दाभोलकर जी ने इसपर अध्ययन किया और अपने प्रयोग परिवार के जरिये प्रयोग भी कराए। तब पता चला कि जो काम ये गोलियां करती हैं, वही काम कद्दू कर देता है। इससे भी गाय का दूध बढ़ जाता है। फिर भला ऊपर से गोलियां क्यों देनीं?
पुस्तक में इस तरह के उदाहरण भरे पड़े हैं। उनकी पूरी दृष्टि अपने आप में शानदार है क्योंकि इसमें ज्ञान-कोश को समृद्ध करने के क्रम में बड़ा ही खुलापन है। यह दृष्टि वैज्ञानिकता और प्रयोग आधारित वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए दुनिया को नितांत स्थानीयता की भावना के साथ छोटी-छोटी भौगोलिक इकाइयों में विकसित करने का लक्ष्य रखती है। उनके तौर-तरीकों में प्रकृति को समझते हुए उसके साथ सामंजस्य बैठाने की
उत्कंठा है।
यह पुस्तक ऐसे चंद विषयों पर केंद्र्रित है जिनमें कृषि महत्वपूर्ण है लेकिन व्यापक दृष्टि से यह अपने आप में एक दर्शन है जो स्थानीयता को केंद्र्र में रखते हुए प्रकृति और विकास की प्रकृति में सामंजस्य की बात करती है। सही अर्थोें में यह
पुस्तक एक दर्शन है। स्थानीयता को केंद्र में रखकर वैश्विक संपन्नता के सूत्र टटोलती इस पुस्तक की प्रासंगिकता आज चीनी कोरोना वायरस के वैश्विक आतंक के दौर में बेहतर समझी जा सकती है।
अरविंद

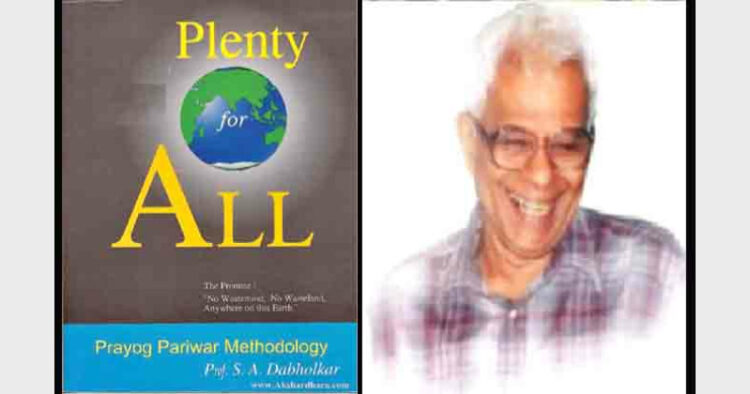










टिप्पणियाँ