भागय्या
अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र, सामाजिक, राजनीतिक शास्त्र तथा धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों का गहन ज्ञान रखने वाले पूज्य बाबासाहेब उच्च कोटि के राष्ट्रभक्त थे।
संविधान निर्माता
संविधान निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। संविधान सभा के ज्येष्ठ सम्मानीय सदस्य श्री टी.टी. कृष्णामाचारी कहते हैं, ‘संविधान निर्माण समिति में सात सदस्यों की नियुक्ति हुई। एक सज्जन ने त्यागपत्र दे दिया, उनके स्थान पर दूसरे सदस्य नियुक्त हुए और एक सदस्य का देहांत हो गया। एक सदस्य भर्ती नहीं हुआ और एक सदस्य अमरीका में थे। एक राज्य के प्रशासन कार्य में लगे थे और दो लोग दिल्ली के बाहर रहते थे तथा अस्वस्थता के कारण बैठकों में नहीं आ सकते थे। इसलिए अंतत: सारा काम आंबेडकर जी को ही करना पड़ा। स्वास्थ्य बहुत ठीक न होने पर भी वे लगन से पूरी शक्ति लगाकर संविधान का काम करते थे। इसलिए हम सब उनको धन्यवाद देते हैं।’ वहीं बाबू राजेंद्र प्रसाद कहते हैं- ‘राष्ट्रजीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तथा जनता के अधिकार और कर्तव्यों को भी ध्यान में रखकर उन्होंने इस महान कार्य को पूरा किया था।’
प्रखर राष्ट्रभक्ति का हृदय
1946 में 9 दिसंबर को संविधान सभा का काम प्रारंभ हुआ। 11 दिसंबर को डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्यों को सभा के सामने रखा- नेहरू जी के वक्तव्य में तीसरे परिच्छेद में-स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश इंडिया के साथ मिलने वाले शेष सभी राज संस्थानों के बारे में बोलते हुए कहा गया-
‘उक्त शासित प्रदेशों को, चाहे उनकी वर्तमान सीमाओं में अथवा संविधान सभा और उसके बाद में संविधान के कानून के अनुसार निर्धारित सीमाओं में, स्वायत्त इकाई की स्थिति प्राप्त होगी और बनी रहेगी, जिसमें उनकी शेष शक्तियां भी होंगी, और वे सरकार तथा प्रशासन की सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेंगे, सिवाय ऐसी शक्तियों और कार्यों के, जो संघ में निहित हैं या संघ के लिए निर्धारित हैं, या संघ में चली आ रही हैं या अंतरनिहित हैं’
सभा में तनाव का वातावरण था। सारे देश को स्वतंत्र भारत में एक राष्ट्र के नाते आगे बढ़ना है। परंतु ब्रिटिश इंडिया के बाहर सभी रजवाड़ों को retain the status of autonomous प्रावधान देने का विरोध था। ऐसे में बाबू राजेंद्र प्रसाद को अचानक बाबासाहेब से बात करने के लिए बुलाया गया।
बाबासाहेब संविधान सभा के सदस्य के नाते, कांग्रेस विरोध के कारण मुंबई से हार गए थे, इसलिए वे बंगाल से चुनकर आए थे।
सभा का गठन और संचालन का सारा काम कांग्रेस के हाथों में था। अन्य रियासतों से भी कांग्रेस का संबंध ठीक नहीं था। जब बाबासाहेब का वक्तव्य शुरू हुआ तो सारे सदस्य अत्यंत श्रद्धा से सुन रहे थे। वक्तव्य ऐतिहासिक था- वर्षों बाद स्वतंत्रता पाने वाले देश के लिए यह भाषण राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि से और देश की एकता बनाए रखने के लिए था।
श्री एऩ वी. गाडगिल जो प्रत्यक्ष सुन रहे थे, इस वक्तव्य के बारे में बताते हैं- उनका वक्तव्य एक श्रेष्ठ राष्ट्रभक्त का था- एकात्मबोध का था, भेदभाव लेशमात्र नहीं था। प्रखरता थी, शब्द उनके हृदयातरंग से आ रहे थे इसलिए सभी हर्ष से उनका स्वागत कर रहे थे।
बाबासाहेब ने अपने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वक्तव्य में कहा –
श्रीमान, इस महान देश की भावी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचना के विकास और उसकी परम उन्नति को लेकर मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं है। मुझे पता है कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से विभाजित हैं। हम झगड़ालुओं के शिविरों का एक झुंड हैं और मैं यह स्वीकार करने की हद तक जा सकता हूं कि मैं शायद ऐसे एक शिविर के नेताओं में से हूं । लेकिन इस सब के बावजूद, मैं पूर्ण आश्वस्त हूं कि समय और परिस्थितियां मिलने के बाद, दुनिया में कोई ताकत देश को एक बनने से नहीं रोकेगी। हमारी सभी जातियों और आस्थाओं के बावजूद, मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि हम किसी न किसी रूप में एकजुट लोगों की तरह होंगे।
बाबासाहेब की विद्वता
वे सदस्यों से पूछते हैं कि परिच्छेद में बताए अनुसार प्रस्ताव पारित करने का अधिकार सभा को हो सकता है, परंतु देश की समग्रता के लिए यह ठीक है क्या? यह भाषण बाबासाहेब के अंत:करण को दर्शाता है। उनके इस भाषण से मातृभूमि के प्रति अत्यंत भक्तिभाव और देश की हजारों वर्षों की परंपरा के प्रति विश्वास और श्रद्धा उजागर होती है।
निष्पक्ष और उदार हृदय
संविधान सभा के काम का सिंहावलोकन करते हुए वे कहते हैं, ‘संविधान की प्रारूप समिति में सब व्यवस्थित चलने का श्रेय कांग्रेस को है। कांग्रेस के अनुशासन के कारण ही मैंने प्रारूप निर्माण किया। कांग्रेस के अनुशासन के कारण ही प्रारूप समिति, संविधान समिति में प्रत्येक धारा व प्रत्येक संशोधन के भविष्य की विश्वासपूर्ण जानकारी के आधार पर संविधान के मार्गदर्शक का काम कर सकी।’
साम्यवादी व समाजवादी संविधान का ज्यादातर विरोध करते थे। साम्यवादी दल को श्रमिक वर्ग की तानाशाही पर आधारित संविधान चाहिए था। समाजवादी लोग दो कारणों से विरोध करते थे। पहला कारण यह कि यदि वे अधिकार (सत्ता) में आते हैं तो मुआवजा न देते हुए निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण अथवा सामाजिकीकरण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा यह कि संविधान में मूलभूत अधिकार निरंकुश व अमर्यादित होने चाहिए। यानी यदि उनका दल सत्ता में नहीं आता है तो उन्हें केवल आलोचना करने की नहीं, बल्कि राजसत्ता उलटने की स्वतंत्रता चाहिए।
वे कहते हैं कि राष्ट्र के उपयोग के लिए स्थापित संस्थाओं और उन्हें चलाने के लिए जनता के विश्वास से नियुक्त लोग प्रामाणिक होंगे, ऐसा मानकर चला जाता है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को राष्टÑहित में जो भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी, इसके लिए प्रावधान रखा गया है।
केंद्र और राज्यों के संबंध तथा अधिकारों के बारे में वे बताते हैं- आपातकाल में सत्ता के दावों से संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। कोई संदेह नहीं कि शेष निष्ठा राज्यों पर न होकर केंद्र पर होनी चाहिए, क्योंकि संयुक्त अधिकार के लिए अंतिम रूप से संपूर्ण देश के सामूहिक हितसंबंध के लिए काम करने वाला केंद्र ही होता है। आपातकाल में राज्य सरकार को हटाने का अधिकार केवल केंद्र को ही होता है। संपूर्ण देश की सुरक्षा और अखंडता तथा एकता के लिए यह आवश्यक है।
ऐतिहासिक दूरदर्शिता
भारत के भविष्य को लेकर उनके मन में बहुत चिंता थी। इस चिंता का कारण उनकी मातृभूमि पर निष्ठा ही थी। संविधान सभा में दिए अपने अंतिम भाषण में वे कहते हैं-
‘26 जनवरी, 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट हो जाएगा। (जयघोष) उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा। वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा कि उसे पुन: खो देगा? इस संबंध में मेरे मन में पहला विचार यह आता है। ऐसा नहीं है कि भारत कभी स्वतंत्र राष्ट्र नहीं रहा है। मुद्दा यह है कि पहले जो स्वतंत्रता थी, उसे उसने गंवाया। क्या वह उसे फिर से गंवा देगा? कारण- वह (उसने) अपनी जनता में से कुछ की अप्रामाणिकता व विश्वासघात के कारण स्वतंत्रता गंवाई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तब दाहिर के सेनापति ने कासिम के दलाल से रिश्वत ली और अपने राजा की तरफ से लड़ने से इनकार कर दिया। मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए व पृथ्वीराज से लड़ने का निमंत्रण देने वाला सोलंकी राजा जयचंद था। जब शिवाजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय बाकी मराठा सरदार और राजपूत मुगल बादशाह की तरफ से लड़ रहे थे। जब ब्रिटिशों ने सिख राजकर्ताओं को नष्ट करने का प्रयास किया, तब सेनापति गुलाब सिंह चुप बैठा रहा।
1857 में भारत के बड़े भाग में ब्रिटिशों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की गई। उस समय सिख प्रेक्षक बने रहे। क्या इतिहास की पुनरावृत्ति होगी? यही विचार मुझे व्यग्र करता है। इस व्यग्रता को तीव्र करने वाला कारण यह है कि जाति व संप्रदाय के अपने पुराने शत्रुओं के साथ अब परस्पर विरोधी व विभिन्न राजनीतिक प्रणाली वाले अनेक राजनीतिक दलों का सामना करना पड़ेगा। भारत के लोग राष्टÑ को अपने राजनीतिक संप्रदाय से श्रेष्ठ मानेंगे अथवा अपने राजनीतिक संप्रदाय को राष्ट्र से श्रेष्ठ मानेंगे? यदि दलों ने अपनी राजनीतिक प्रणाली को राष्टÑ से श्रेष्ठ माना तो स्वतंत्रता फिर खतरे में पड़ सकती है। इससे अपने देश की रक्षा करनी है।
समता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा हो सकती है। इसमें समता और स्वतंत्रता दोनों की रक्षा के लिए बंधुता अत्यंत आधारभूत है। आज बंधुता के आधार पर ही संपूर्ण समाज को संगठित किया जा सकता है और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है।
लोकशिक्षक बाबासाहेब
उच्च शिक्षा के पहले चरण में इंग्लैंड से भारत आने पर बाबासाहेब ने बंबई के सिडे हॅम महाविद्यालय में दो साल अर्थशास्त्र का अध्यापन किया। बाद में एक निजी संस्था में प्रोफेसर आॅफ मर्केन्टाईल के पद पर कार्य किया। सन् 1928 में वे शासकीय विधि महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए। आगे चलकर इसी महाविद्यालय में सन् 1935 में प्राचार्य पद पर उनकी नियुक्ति हुई। इस पूरी अवधि में उन्होंने एक सव्यसाची, विद्यार्थी प्रिय, प्राध्यापक और अनुशासनप्रिय प्रशासक के रूप में ख्याति प्राप्त की। अध्यापन, विषय का गहरा ज्ञान, चौतरफा वाचन और अत्यंत व्यामिश्र जीवनानुभव से उनका अध्यापन प्रभावी और वजनदार था। उनकी अध्यापन शैली में संवाद कुशलता, भाषा की शान और गहरा ज्ञान था। अंग्रेजी भाषा पर उनका अनूठा प्रभुत्व था। उन्हें विद्यार्थियों को विषय, क्रमिक पुस्तक पढ़ाने का जैसे एहसास था, वैसे ही उनका चरित्र निर्माण करना है, साथ-साथ मार्गदर्शन करना है, इसका भी ज्ञान था। महाविद्यालय के प्राचार्य के नाते, बंबई विश्वविद्यालय के कामकाज पर उन्होंने अमिट छाप छोड़ी थी।
अध्यापन लौकिक पेशा था और उसके साथ-साथ वे व्यावहारिक कुशलता सिखाने का, लोकशिक्षक का काम भी करते थे। सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं की उन्हें गहरी समझ थी। ‘मूकनायक’, ‘बहिष्कृत भारत’, ‘जनता’ आदि नियतकालिकों (पीरियाडिकल्स) से उन्होंने इन समस्याओं की कठोर चिकित्सा की और उनके बारे में दिग्दर्शन भी किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समाज समता संघ आदि संस्थाओं से उन्होंने समाज परिवर्तन को गति दी। दलित और अस्पृश्य समाज की अनेक परिषदों में उन्होंने अपने प्रभावी भाषणों के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन किया। सन् 1927 में महाड में हुई परिषद और चवदार तालाब सत्याग्रह के समय उनके भाषण विशेष रूप से मशहूर हुए। उन्होंने दलित मुक्ति आंदोलन की नींव डाली। बंबई, दिल्ली, बीबीसी लंदन और वायस आॅफ अमरीका आदि रेडियो केन्द्रों से उन्होंने विचार करने को बाध्य करने वाले प्रभावी भाषण दिए। अनेक शासकीय समितियों और मंचों से विचार व्यक्त किए। प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर शासकीय यंत्रणाओं में जिम्मेदारी के पद को विभूषित करते हुए किया हुआ कार्य और व्यक्त किए विचार, व्यापक अर्थ से लोकशिक्षा ही है। उनमें जो कालनिरपेक्षता और चिरनूतनता है, वह दर्शनीय तो है ही पर सच्चे अर्थों में समाजमन पर किए गए जादू जैसी है। लोक शिक्षक के रूप में बाबासाहेब का किया हुआ काम चिरस्मरणीय है।
पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी की स्थापना करके उन्होंने दलित समाज के विद्यार्थियों के लिए बंबई और औरंगाबाद में उच्च शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना की। ये महाविद्यालय उपेक्षित समाज के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान के मुक्तद्वार थे। संस्था संचालन करते हुए उन्होंने दूरदर्शिता, तत्वनिष्ठा और पारदर्शी व्यवहार पर बल दिया। इन संस्थाओं में आर्थिक अनुशासन और सच्चाई पर जोर दिया गया। सार्वजनिक पैसे का भलीभांति हिसाब रखकर, उसे समय-समय पर जनता को दिखाना और इसे पवित्र कर्तव्य समझना उनकी संस्था व्यवहार के बारे में संकल्पना थी।
उन्होंने दलित विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, उत्तम ग्रंथालय और प्रयोगशाला आदि सुविधाओं की भी व्यवस्था की। शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति करते समय उन्होंने जाति को नहीं, बल्कि योग्यता को महत्व दिया। उनका आग्रह था कि मेरे विद्यार्थियों को गुणी अध्यापकों से सर्वोत्तम ज्ञान मिलना चाहिए। बाबासाहेब के समय इन शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत रहे प्राध्यापकों की और प्राचार्यों की नामावली देखी जाए तो वे कितने उच्च स्तर के नामवर थे, इसका उदाहरण मिलता है। वे समाज को तत्वनिष्ठ व्यवहार और उत्कृष्ट विचार देकर रुके नहीं। आदर्श शिक्षा केन्द्र कैसा होना चाहिए, उसका एक आदर्श उन्होंने समाज के सामने रखा।
महाविद्यालय के प्राध्यापकों को संबोधित करते हुए वे कहते हैं, ‘अध्ययन और अध्यापन के काम में प्राध्यापक इतने जुट जाएं कि अपने घर की ओर देखने के लिए भी उनको वक्त न मिले। अध्ययन और अध्यापन के साथ अनुसंधान भी आ जाता है। उनका केवल विद्वान होना ही अपेक्षित नहीं, वे बहुश्रुत भी हों, उनमें विषय को रंजक बनाने की कला और उत्साह हो। इनमें से कुछ गुण तो आपमें होंगे ही, पर कुछ अध्ययन और अनुभवों के द्वारा साध्य करने होंगे।’
अध्यापकों को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि ‘प्रत्येक पीढ़ी एक स्वतंत्र राष्टÑ है, ऐसा हम मानें। हर पीढ़ी को बहुमत से स्वयं को बंधित करने का हक है। दूसरे देश पर बंधन लादने का अधिकार जैसे उन्हें नहीं, वैसे ही अपने पीछे आने वाली पीढ़ी पर बंधन डालने का भी उन्हें हक नहीं है।’ इन विचारों से बाबासाहेब ने सच्चे लोकतंत्र का सार हमारे सामने रखा है।
पाठशाला और शिक्षा संस्था
डॉ. आंबेडकर कहते हैं कि पाठशाला एक पवित्र संस्था है। वहां छात्रों के मन सुसंस्कृत होते हैं। इसीलिए पाठशाला का कारोबार अनुशासन से चलना चाहिए। अन्य जगहों पर अंधाधुंध कारोबार से सार्वजनिक पैसे की हानि होगी, परंतु शिक्षा के कारोबार में अगर अंधाधुंध गड़बड़ी हो जाए तो नई पीढ़ी का नुकसान होगा। इस भेद और धोखे को कोई भी, कभी भी न भूले। ‘बहिष्कृत भारत’ के एक लेख में वे कहते हैं, ‘पाठशाला के छात्रों के मन को समाजहित के लिए मोड़ देना चाहिए। पाठशाला उत्तम नागरिक बनाने का कारखाना है। अर्थात् इस कारखाने में फोरमैन जितना कुशल, उतना अच्छा माल कारखाने में तैयार होगा।’ अध्यापकों और संस्था चालकों के लिए कारोबार का बाबासाहेब का दिशादर्शन है यह।
बाबासाहेब ने शिक्षा क्षेत्र की आदर्श संस्था का श्रीगणेश पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी की स्थापना करके किया। शिक्षा संस्था के संचालन की जो नियमावली बाबासाहेब ने तैयार की, उससे शिक्षा संस्था के आदर्श कारोबार और व्यवहार के बारे में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। वे शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक-प्राध्यापकों की नियुक्ति करते समय जाति-पांति का नहीं, उच्च योग्यता का आग्रह करते हैं। वे कहते हैं कि मेरी शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के छात्रों के प्रवेश को सर्वाधिक प्रधानता है, परन्तु उन्हें पढ़ाने वाला अध्यापक वर्ग केवल उच्च योग्यता वाला ही हो, भले ही वह किसी भी जाति का क्यों न हो। उनका मानना था कि राजनीतिक दलों को भी शिक्षा कार्य करना चाहिए और उसके लिए शिक्षा संस्थाओं का जाल तैयार करना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने शे़ का. फेडरेशन के घोषणा पत्र में इस विषय का स्पष्ट उल्लेख करने वाली धारा को समाविष्ट किया।
बाबासाहेब सहशिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने कहा है कि स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी में एक साथ शिक्षा प्राप्त हो। वे कहते हैं कि स्त्रियों के साथ रहकर भी जो पुरुष अपना मन काबू में रखते हैं और पुरुषों के संग में रहकर भी जो स्त्रियां अपना पांव न फिसले, इस बारे में सजग रहती हैं, उन्हें नीतिमान कहना चाहिए। बाबासाहेब का स्पष्ट मत था कि संस्था चालकों को सहशिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए।
छात्रों का दायित्व
बाबासाहेब स्वयं अनेक वर्षों तक प्राध्यापक रहे थे, अत: छात्रगण से उनका गाढ़ा परिचय था। शिक्षा से छात्रों का आत्मविश्वास जागना चाहिए, इस विचार को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं-आत्मविश्वास जैसी दूसरी दैवी शक्ति नहीं, हमें अपना आत्मविश्वास कभी गंवाना नहीं चाहिए। बाबासाहेब मूल्य शिक्षा पर बल देते हुए कहते थे कि विद्या, विनय, शील और कड़ा अनुशासन – सब कुछ छात्रों को आत्मसात करना चाहिए। विद्या के साथ शील चाहिए, क्योंकि शील के बिना विद्या व्यर्थ है। वे कहते थे कि शिक्षा से छात्रों की सामाजिक संवेदनाएं भी सजग होनी चाहिए। छात्रों को राजनीति में दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर वे अध्ययन छोड़कर राजनीति को अपनाने लगेंगे, तो जीवनभर उनकी हानि होगी।
उपाधि की सीमाएं स्पष्ट करते हुए बाबासाहेब कहते हैं कि केवल उपाधि धारण करके कुछ भी साध्य नहीं होगा, क्योंकि विश्वविद्यालयों की उपाधियों और बुद्धिमत्ता में अन्योन्य संबंध होता हो, ऐसा नहीं है। परीक्षा में सफल होना और उपाधि पाना अलग है और सुशिक्षित और ज्ञानी होना अलग है। अर्थात् उनकी छात्रों से यह अपेक्षा थी कि छात्रों का भारवेत्ता होने से ज्ञानवेत्ता होना ज्यादा जरूरी है।
छात्रों की कमियों को सही ढंग से जानते हुए बाबासाहेब कहते हैं कि विषय की जड़ तक पहुंचकर सम्यक् ज्ञान का मार्मिक आकलन करके उसकी भलीभांति रचना करने की योग्यता, सर्वसाधारण ज्ञान की बुनियादी अवस्था, युक्तिवाद, निर्दोष मत प्रदर्शन, प्रश्नों के तर्क की कसौटी पर उत्तर खोजना, मन के विचारों को सुस्पष्टता से रखना – आदि बातें छात्रों में आजकल कम मात्रा में दिखाई देती हैं।
सिद्धार्थ महाविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए बाबासाहेब कहते हैं -‘शिक्षा से आपके मन, दृष्टि, विचारशक्ति, समस्या सुलझाने की ताकत आदि का विकास होना चाहिए। आज हमारा देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं के बारे में इस शक्ति के माध्यम से अपना अभिमत बनाने में उस शक्ति का, दृष्टि का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, राजनीतिज्ञों को इन समस्याओं को सुलझाने में आपके इस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। आपकी सहकारिता से वे उत्तर खोजे जाने चाहिए। अगर वे कहीं गलती कर रहे हैं तो निडरता से, स्पष्टता से उन्हें बताने का साहस शिक्षा से प्राप्त होना चाहिए।’ इतनी बड़ी अपेक्षा वे छात्रों से रखते थे।
अध्यापकों की योग्यता
स्वयं एक उत्कृष्ट अध्यापक रहे बाबासाहेब की अध्यापक वर्ग से क्या अपेक्षाएं थीं। उनका कहना था कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और अध्यापक उसका मुख्य आधार है। इसीलिए शिक्षा और योग्यता उनकी ज्ञानपिपासा, विद्याव्यासंग, आत्मीयता और ध्येयासक्त जीवनदृष्टि इन बातों पर निर्भर है। बाबासाहेब ने अपनी ज्ञानसाधना में वाचन-मनन, चिंतन और अध्ययन के त्रिसूत्र को अपनाया था। इसी वजह से वे स्वयं एक उत्कृष्ट अध्यापक और व्यापक अर्थ में समाजशिक्षक बन पाए। इस संदर्भ में उनकी भूमिका पहले करनी बाद में कथनी थी।
अध्यापक को बहुश्रुत होना आवश्यक है। उसे अपने विचारों का विन्यास अच्छी तरह करना जरूरी है, अपने और दूसरों के विचार जांचना जरूरी है, तभी वे छात्रों को अध्ययन करने तथा विचार करने के लिए प्रवृत्त कर सकेंगे। वह तेज बुद्धि का और चयनशीलवृत्ति का हो। उसमें चिकित्सकवृत्ति तथा मर्मज्ञता हो। उनकी दृष्टि में अध्यापक वर्ग राष्टÑ का सारथी है, क्योंकि उनके हाथों में शिक्षा की बागडोर होती है। अत: पाठशालाओं में सम्बुद्धि वाले, उदात्त विचारों से भरपूर और विशाल हृदय के अध्यापक होना जरूरी है।
शिक्षा नीति
डा़ॅ आंबेडकर ने अपनी शिक्षा विषयक नीति क्रमबद्ध रूप से ग्रंथित नहीं की। इस संदर्भ में उनके रखे विचार अन्य स्थानों पर अलग-अलग माध्यमों द्वारा व्यक्त हुए हैं। उनकी संपादित पत्रिकाएं, स्थापित की हुई सामाजिक और शिक्षा संस्थाओं के ध्येय और नीतियों से उनके विचारों का पता चलता है। उनके अन्यान्य शासकीय समितियों, आयोगों के सामने दिए गए साक्ष्य, प्रस्तुत किए गए पत्र-प्रपत्र इनके माध्यम से भी शिक्षा नीति का चिंतन सामने आता है। विविध परिषदों में, सम्मेलनों में, महाविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में दिए भाषणों के द्वारा भी विचार प्रस्तुत हुए हैं। वैधानिक क्षेत्र अर्थात् बंबई विद्यापीठ सीनेट, शिक्षण संस्थाओं में उनके भाषणों में भी विचार प्रस्तुत हुए। बंबई विधिमंडल, महाराज्यपाल की मंत्रिपरिषद, संविधान सभा, लोकसभा आदि में हुई चर्चाओं में उन्होंने शिक्षा नीति के अनेक मुद्दों पर विशद विचार व्यक्त किए हैं। उनके विस्तृत चिंतन में शिक्षा क्षेत्र की सामाजिक विषमताएं, उस पर उपाय, साक्षरता प्रसार और विकास की आवश्यकता, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और संशोधन, व्यवसाय प्रशिक्षण, तंत्र शिक्षा जैसे विषय विविध स्तरों के संदर्भ में दिखाई देते हैं। उनके व्यापक चिंतन में से कुछ विशेष मुद्दों पर विचार इस प्रकार हैं :
एकसूत्रीय राष्ट्रीय नीति
केन्द्रीय सत्ता की परिकल्पित एकसूत्रीय राष्ट्रीय नीति से ही सार्वजनिक शिक्षा की समस्या – यह खंड-खंड करके सुलझने वाला प्रश्न नहीं है, बल्कि यह प्रश्न एकसूत्री नीति से ही सुलझ सकता है, क्योंकि शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रदीर्घ प्रक्रिया है। शिक्षा क्षेत्र को सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर व्यक्ति की सत्ता धोखादायक है। शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं को न सौंपें। वे कहते हैं, शिक्षा गटर साफ करने जैसी बातों से भिन्न है, यहां कारोबार उपयुक्त नहीं।
शिक्षा अन्न के समान
साक्षरता प्रसार और विकास तथा सार्वत्रिक शिक्षा के उद्देश्य पर बल देते हुए बाबासाहेब कहते हैं कि एक बार बच्चे ने प्राथमिक शाला में प्रवेश ले लिया, तो वह साक्षर हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक उसमें जीवनभर साक्षर रहने की क्षमता विकसित नहीं होती, तब तक वह प्राथमिक शाला या साक्षरता वर्ग न छोड़े। उनकी दृष्टि में शिक्षा अन्न के समान है, उसकी आवश्यकता जीवनभर होती है। उनको दृढ़ मत था कि इस संदर्भ में पूरी जिम्मेदारी शासन को ही उठानी होगी।
सामाजिक विषमता
शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त सामाजिक विषमता के बारे में बाबासाहेब का मत अत्यंत स्पष्ट है। सन् 1927 में बंबई विधिमंडल में दिए भाषण में उन्होंने इस संदर्भ में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर जो विषमता है, उसकी सांख्यिकी प्रस्तुत की। उस पर आधारित निष्कर्ष थे- समूचे हिन्दू समाज में निरक्षरता का परिमाण 82़.5 प्रतिशत है, उसमें भी पिछड़े समाज में वह 98 प्रतिशत जैसा भयंकर है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर पिछड़े वर्ग की अवस्था अत्यंत दयनीय है। शैक्षिक विषमता की जड़ सही मायने में सामाजिक और आर्थिक विषमता में है।
उपाय
इस परिस्थितियों के उपाय बताते हुए वे कहते हैं कि असमान बर्ताव तत्व को स्वीकार करके कुछ वर्गों को विशेष सहूलियतें देने की आवश्यकता है। जो निम्नस्तरीय हैं, उन्हें विशेष दर्जा और सहूलियत देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे कहते हैं, केवल छात्रवृत्ति देने से पिछड़े वर्ग की समस्या नहीं सुलझ पाएगी। छात्रावास, अभ्यासगृह, बालवाड़ी, संस्कार केन्द्र आदि से उनके लिए उचित, प्रेरणादायी सामाजिक वायुमंडल का निर्माण करना आवश्यक है। आगे चलकर भारतीय संविधान में शामिल हुए आरक्षण नीति के बीज उनके इस भाषण में मिलते हैं।
समाज परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा से समाज परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। बाबासाहेब कहते हैं कि परिवर्तन की इस प्रक्रिया को गति देने के लिए समाज मानस में परिवर्तनवादी विचार दृढ़ होना आवश्यक है। व्यापक एवं सार्वत्रिक शिक्षा द्वारा ये विचार समाज में दृढ़ बन सकते हैं। शिक्षा का सामाजिक आशय कभी भी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। शिक्षा की संकल्पना के अंतर्गत ‘पढ़ो और पढ़ाओ’ की प्रक्रिया अभिप्रेरित होती है। उसी से समाज की प्रगति संभव होती है। बाबासाहेब कहते हैं कि शिक्षा के बिना किसी भी समाज में संवेदनशीलता, प्रतीति या सजगता निर्मित नहीं होगी तथा बिना जागृति के समाज की उन्नति भी नहीं होती। शिक्षा का आशय खासकर ऐहिक होना चाहिए। उनकी व्यावहारिक अपेक्षा थी कि समाज में जो विषमताएं हैं, वे शिक्षा के माध्यम से दूर हों। वे एक आदर्शवादी विचार सामने रखते हैं कि शिक्षा किसी के व्यक्तित्व में निहित सुप्त शक्तियों को मुक्त करती है और मनुष्य को पशुता से मनुष्यत्व की ओर ले जाती है। बाबासाहेब यह कहने से भी नहीं चूकते थे कि शिक्षा का हेतु व्यक्ति का सामजिकीकरण और नैतिकीकरण करना है क्योंकि सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद शिक्षा ही है।
बाबासाहेब की ज्ञान की संकल्पना बड़ी ही व्यापक और आदर्श है। वे कहते हैं कि विद्या, प्रज्ञा, करुणा, शील और मित्रता इन पंचतत्वों के अनुसार हरएक को अपना चरित्र निर्माण करना चाहिए। वे कहते हैं कि विद्या के साथ शील भी चाहिए, शील के बिना विद्या व्यर्थ है। विद्या तलवार के समान है इसीलिए जो उसे धारण करे, उस पर उसकी महत्ता अवलंबित है। बुद्धि और चतुराई को सदाचार अर्थात् शील का साथ मिलना चाहिए। बगैर शील के अगर शिक्षित लोग निर्मित होने लगेंगे, तो उनकी शिक्षा से राष्ट्र और समाज का नाश होगा। मनुष्य का निर्माण करे, वह शिक्षा। ज्ञान और प्रज्ञा का सुचारु मेल माने शिक्षा। व्यक्ति को स्वत्व की प्रतीति कराना शिक्षा का कार्य है।
ज्ञान का अर्थ है प्रकाश। गौतम बुद्ध की दी हुई शिक्षा की यह परिभाषा बाबासाहेब को भाती है। यह प्रकाश सामाजिक, आर्थिक, राजकीय क्रांति का आधार बनना चाहिए। प्रकाश शब्द का विश्लेषण वे इस प्रकार करते हैं- शिक्षा का संदर्भ सामाजिक होना चाहिए, शिक्षा शोषणमुक्ति का महामार्ग है, अत: समाज में जो पीड़ित, उपेक्षित, शोषित घटक हैं उनकी दैन्यावस्था मिटाने वाला अचूक उपाय है शिक्षा । उनकी दृष्टि से समाज में जो पददलित हैं, उनकी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का आंदोलन है शिक्षा। वे समाज के निम्नस्तर को उच्चस्तर तक उठाने के लिए शिक्षा और शिक्षा में आरक्षण के दोहरे उपायों के कठोर क्रियान्वयन की जरूरत मानते हैं। समताधिष्ठित, मूल्याधिष्ठित और नीतिमान समाज- यह सफल लोकतंत्र की पूर्वशर्त है और यह संस्कार केवल शिक्षा के माध्यम से ही हम पा सकते हैं। उनका यह प्रतिपादन चिंतनीय है।
समाज में निरक्षरता के परिमाण के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए बाबासाहेब कहते हैं कि इसी निरक्षरता ने जनता को मानसिक दृष्टि से गुलाम, आर्थिक दृष्टि से दरिद्र, सांस्कृतिक दृष्टि से लूला-लंगड़ा और सामजिक दृष्टि से पिछड़ा बना दिया। इसी वजह से समाज विदेशी आक्रमकों के विरुद्ध संघर्ष करने की ताकत खो बैठा है। उनके इस अभिप्राय का भावार्थ समझने की आवश्यकता है। बाबासाहेब ने शिक्षा और शिक्षाशास्त्र की केवल तात्विक चर्चा नहीं की है। उनका शिक्षा संबंधी ध्येय यह है कि औपचारिक शिक्षा को नैतिकता का साथ मिलना चाहिए।
बंबई विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि पाने के बाद सन् 1913 में वे उच्च शिक्षा हेतु अमरीका गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अनेक चर्चा सत्रों में उन्होंने शोध निबंध भी प्रस्तुत किए। बाद में इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल आॅफ इकोनॉमिक्स तथा ग्रेज इन नामक विश्वमान्य संस्थाओं में अध्ययन किया। वहां उन्होंने एमएससी, डीएसी, एलएलडी, बार एट लॉ ये उपाधियां सम्मान सहित प्राप्त कीं। सन् 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि सम्मान के साथ प्रदान की। हर उपाधि के लिए उन्होंने ज्ञानसाधना कर स्वतंत्र संशोधन ग्रंथ लिखे और वे ग्रंथ विश्वविख्यात हुए। इनमें प्रमुख रूप से सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय विषयों के ग्रंथों का समावेश है। विदेश से वापस आने पर देश के सामने जो अनेक समस्याएं थीं, उनपर अध्ययन करके उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। उनका अध्ययन और लेखन निर्बाध गति से सदा चलता रहा। सडसठ साल की उम्र में उनकी जीवनयात्रा समाप्त हुई। उससे कुछ दिन पूर्व उन्होंने ‘बुद्ध और धम्म’ नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखकर पूरा किया था। उनका समग्र साहित्य 22 खंडों में 15,000 पृष्ठों में ग्रंथित हुआ है। बाबासाहेब के इस योगदान का परामर्श लेना एक स्वतंत्र अध्ययन का विषय है।
बाबासाहेब ने वैचारिक विश्व में जो परिवर्तन किया, उसका प्रमुख आधार रहा उनका अखंड ग्रंथ पठन। वे विदेशी विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों में प्याला भर दूध और ब्रेड के दो चार टुकड़े खाकर 18-18 घंटे अध्ययन करने वाले विद्यार्थी थे। पेट काटकर उन्होंने 35,000 ग्रंथ खरीदे। और तो और, हर ग्रंथ बारीकी से पढ़ा हुआ और हाशिये में टिप्पणी किया हुआ था। ग्रंथ तो मानो उनके प्राण ही थे। पं़ मदनमोहन मालवीय जी ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए इन ग्रंथों की मांग की थी। वे उन ग्रंथों के लिए मुंहमांगा दाम देने के लिए तैयार थे। उसे बड़ी नम्रता से अस्वीकार करते हुए बाबासाहेब ने कहा, ‘आप तो मानो मेरे प्राण ही मांग रहे हैं।’
शिक्षा विषयक चिंतन
शिक्षा लो, संगठित हो और संघर्ष करो- बाबासाहेब ने प्रगति का यह मूलमंत्र समाज को दिया। इस मूलमंत्र में शिक्षा का प्रथम स्थान है। परंतु उनका शिक्षा विषयक चिंतन, सुसंगठित रूप में, प्रबंध रूप में उपलब्ध नहीं बल्कि अन्यान्य रचनाओं में बिखरा पड़ा है। सम्मेलनों और परिषदों में किए हुए भाषण, पत्रवांग्मय, पत्रिकाओं में छपे लेख, शिक्षा संस्थाओं को दी भेंट, प्रांतिक या केन्द्रीय विधिमंडलों में तथा विश्वविद्यालयों में किये भाषण, अन्यान्य वर्गों के सामने दिए हुए साक्ष्य आदि में ये विचार व्यक्त हुए हैं। अपने समग्र चिंतन में शिक्षा का तत्वज्ञान, ध्येयवाद, शिक्षा का सामाजिक आशय, पाठ्यक्रम का स्वरूप और ध्येय, विद्यार्थियों का दायित्व, अध्यापकों की पात्रता, पाठशाला तथा महाविद्यालयों की जिम्मेदारी, शिक्षा क्षेत्र में रखे गए आरक्षण और उनकी मीमांसा जैसे शिक्षा विषयक अलग-अलग पहलुओं पर उन्होंने भाष्य किया है। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालयों का कारोबार, साक्षरता प्रसार, सार्वत्रिक शिक्षा की अनिवार्यता आदि बातों की भी उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने सैद्धांतिक रचना के साथ व्यावहारिकता को भी महत्व दिया। हम अब उनकी इसी विचारसंपन्नता का संक्षिप्त लेखा- जोखा लेंगे।
बाबासाहेब का मत था कि शिक्षा और समाज का एक अटूट रिश्ता होता है क्योंकि शिक्षा ही समाज के सांस्कृतिक उन्नयन का आधार होती है। वे कहते हैं कि समाज द्वारा अपना स्तर अधिक से अधिक ऊंचा उठाने के लिए सामूहिक प










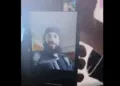

टिप्पणियाँ