|
अदालतों पर मुकदमों का इतना बोझ है कि वर्षों तक लोगों को न्याय नहीं मिलता। इस समय देश में 2.2 इंसाफ की आस करोड़ मुकदमे लंबित हैं। लोग न्याय की आस में जी रहे हैं। उन्हें जीते जी इंसाफ मिलेगा, इसकी उम्मीद कम है
राजेश गोगना
चडीगढ़ में रहने वाले आशीष कुमार ने अपने भाई विनोद को आखिरी बार 1994 के मई मास की दोपहरी में देखा था जब कुछ पुलिस वाले उसे उठा ले गए और फिर उसका कुछ भी पता नहीं चला। मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने जांच की और पाया कि विनोद की मौत के लिए सैनी नाम के आला अफसर जिम्मेदार थे और हत्या का मुकदमा 1994 में ही दायर कर दिया गया।
विनोद की मां अमर कौर उस समय 72 वर्ष की थीं और सोचती थीं कि जल्दी ही उन्हें इंसाफ मिलेगा और दोषियों को सजा। अमर कौर आज 94 वर्ष की हैं। न ढंग से बोल पाती हैं, न सुन पाती हैं, और न कोई बात समझ सकती हैं, पर उन्हें यह अनुभव हुआ है कि हत्यारा यदि अमीर और रसूखवाला हो तो भारत की न्यायिक व्यवस्था उसके सामने घुटने टेक देती है।
अमर कौर को 22 वर्ष बाद भी न्याय नहीं मिला है। आयु अधिक होने की वजह से अब वे ठीक से चल भी नहीं पातीं इसलिए तारीखों में स्ट्रेचर पर ही अदालत पहुंचती हैं। वे सोचती हैं कि उनके मरने से पहले उन्हें इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन भारतीय न्यायालयों में मुकदमों के अंबार को देखें तो इसकी संभावना धुंधली नजर आती है।
अमर कौर की तरह भारत के लाखों लोग विभिन्न जिला अदालतों में लंबित अपने 2.2 मुकदमों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से लगभग 60 लाख मुकदमे पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों में 45 लाख से अधिक और सर्वोच्च न्यायालय में 60,000 से अधिक मुकदमे लंबित हैं और इनकी संख्या खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के पास एक दिन में 100 से अधिक मुकदमे होते हैं और उन्हें निस्तारित करने के लिए कुल 300 मिनट। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक मुकदमे पर औसतन तीन मिनट से अधिक का समय नहीं दे पाते। जिला न्यायालयों में तो यह स्थिति और भी खराब है। अदालतों के कमरों के बाहर भीड़ का आलम यह है कि मुकदमे से जुड़े लोगों का अदालत के कमरों में दाखिल होना भी दुष्कर हो जाता है। यह भीड़ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भी देखी जा सकती है।
मुकदमों का फैसला न्यायाधीशों के बिना नहीं हो सकता। भारत में 10 लाख लोगों पर केवल 13 न्यायाधीश उपलब्ध हैं। यह विकसित देशों के औसत से काफी कम है, जहां 10 लाख की आबादी पर 50 से अधिक न्यायाधीश हैं। न्यायालय की कार्य व्यवस्था ऐसी हो गई है कि वकील मुकदमों में तारीख पर तारीख मांगते हैं और न्यायाधीश अपने उस दिन का काम निबटाने के लिए तारीख दे देते हैं। तारीखों का यह क्रम देश को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाता है। किसी भी न्यायालय को चलाने का औसतन खर्चा 15 से 20 लाख रुपए प्रतिमाह आता है। देश में लाखों अदालतें हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि न्याय व्यवस्था पर देश कितना खर्च करता है और जनता का यह पैसा व्यर्थ हो रहा है। विडंबना यह भी है कि भारत सरकार न्याय मंत्रालय को अपने कुल बजट का केवल 0.2 प्रतिशत ही देती है। दुनिया के सबसे पिछड़े देशों के मुकाबले भी यह राशि बहुत कम है। भारत की जेलों की स्थिति तो और भी खराब है। जेलों में उनकी क्षमता से 3-4 गुना ज्यादा कैदी रह रहे हैं। यह भी चिंता और चिंतन की बात है कि जेलें सुधार की प्रयोगशाला की बजाय अपराध की पाठशाला बनती जा रही हैं। एक अनुमान के अनुसार जेलों में रहने वाले 80-90 प्रतिशत कैदी गरीबी रेखा से नीचे के हैं। इन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिलता और न्याय मिलने की उम्मीद भी नहीं है।
छुट्टियां अधिक
भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जिस पर न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, में 16 मई से 2 जुलाई तक 43 दिन की गर्मी की छुट्टी होती है। 2013 से पहले यह छुट्टी 70 दिन की होती थी। लगभग 43 दिनों की धार्मिक तथा सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं। इसमें रविवार तथा अन्य छुट्टियां शामिल नहीं हैं। आज भी सर्वोच्च न्यायालय साल में लगभग 103 दिन बंद रहता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री लोढ़ा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय 365 दिन में केवल 193 दिन, उच्च न्यायालय 210 दिन तथा जिला न्यायालय केवल 245 दिन ही काम करते हैं।
विधि आयोग ने अपनी रपट में सुझाव दिया था कि अदालतों की छुट्टियों में 10-15 प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए और काम की अवधि में डेढ़ घंटे की वृद्धि होनी चाहिए।
श्री लोढ़ा ने राय दी थी कि भारत के न्यायालय पूरे वर्ष काम करें तथा न्यायाधीश अपनी इच्छा-अनुसार छुट्टियां तय करें, लेकिन इस राय को वकीलों तथा न्यायाधीशों ने भी नकार दिया, क्योंकि इनके लिए अपनी छुट्टियां मरती हुई न्यायिक व्यवस्था से ज्यादा जरूरी थीं।
न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता
भारत में मुकदमों को निस्तारण करने के लिए अंग्रेजों द्वारा सुझाया गया एडवर्सियल सिस्टम (अपने मुकदमे में खुद पेश होना) काम करता है। इसमें आरोप लगाने वाले पक्ष को ही आरोप सिद्ध करना पड़ता है और कोई भी चूक होने से मुकदमा खारिज हो जाता है। इस व्यवस्था में न्यायाधीश का काम बहुत ही सीमित होता है। न्यायाधीश स्वयं से जांच नहीं करा सकता। जबकि विकसित देशों में न्यायाधीश मुकदमे के निस्तारण की हर प्रक्रिया में भूमिका निभाता है और वह निश्चित करता है कि दोषी को सजा मिले। भारत में मुकदमों में झूठ बोलने की बड़ी बीमारी है। लोग साफ तौर पर झूठ बोलते हैं, पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और न्यायाधीश इस प्रक्रिया को शुरू करने से बचते हैं। जिस न्यायिक व्यवस्था में झूठ बोलने वाला दंडित नहीं होगा, उस व्यवस्था में किसी को न्याय नहीं मिल सकता। भारत का कानून अपराध सिद्ध होने पर ही किसी अपराधी पर कार्रवाई करता है। बहुत से अपराधी शक के आधार पर छूट भी जाते हैं। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। इस कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। भारत के फौजदारी मुकदमों में संभावना के आधार पर सजा का सिद्धांत लागू होना चाहिए।
-न्यायमूर्ति मूलचंद गर्ग, पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
आम आदमी से दूर न्यायिक व्यवस्था
भारत में आम आदमी की पहुंच न्यायिक व्यवस्था तक तो है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह न्याय आम आदमी को उपलब्ध नहीं हो पाता। 1980 से पहले व्यवस्था में खुलापन नहीं था। सब कुछ छुपा होने के कारण आम आदमी तक न्याय नहीं पहुंचता था। 1980 के बाद न्याय व्यवस्था में खुलापन तो आया, पर यह बहुत ज्यादा महंगी हो गई। आम आदमी को न्याय व्यवस्था तक आने का अधिकार तो है किंतु वह उपलब्ध नहीं है। न्याय व्यवस्था में न्याय की उपलब्धहीनता की स्थिति बहुत ही विकट है। व्यक्ति को जब न्याय नहीं मिलता तो न्याय व्यवस्था से ही उसका विश्वास उठ जाता है। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था एक गंभीर खतरे में आ जाती है। लाखों लोग पढ़ाई-लिखाई कर वकील बन रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी गरीब आदमी के लिए उपलब्ध नहीं है। सबके सब कारपोरेट वकील बनना चाहते हैं तथा गरीबों के लिए पूरी तरह संवेदनहीन हैं। संवेदनहीन वकीलों की इस फौज का गरीब आदमी को क्या फायदा।
-संजय जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता, भारत सरकार
मुकदमों का पहाड़
सन् 1987 में विधि आयोग ने बताया था कि एक लाख की आबादी पर 10.5 न्यायाधीश थे। अब यह संख्या 13-14 है। यूके में यह दर 50.9, कनाडा में 75.2, अमेरिका में 107 प्रतिशत है। विधि आयोग की एक रपट के अनुसार भारत में 10 लाख की आबादी पर 107 न्यायाधीशों की आवश्यकता है। 31 दिसम्बर, 2015 तक उच्च न्यायालयों में 38.76 लाख मुकदमे और जिला न्यायालयों में 2.18 करोड़ मुकदमे लंबित थे। इनमें 1.46 करोड़ फौजदारी और 72 लाख दीवानी हैं।
पैमाना अलग
भारत में लंबित मुकदमों की संख्या को लेकर बहुत असमंजस है। ऐसे मुकदमों की परिभाषा को लेकर भी काफी विवाद है। विधि आयोग की 245 रपटों में बताया गया है कि भारत का हर उच्च न्यायालय अपने हिसाब से लंबित मुकदमों की संख्या तय करता है। संख्या तय करने का एक पैमाना न होने से संख्या को बहुत बढ़ा कर या बहुत घटा कर प्रस्तुत किया जाता है। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, मुम्बई, कर्नाटक और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में वादकालीन अनुरोध पत्रों को लंबित मुकदमों की श्रेणी में नहीं गिना जाता, जबकि दूसरे उच्च न्यायालयों में इन पत्रों को गिना जाता है।
पंजाब, हरियाणा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में लंबित तथा निस्तारित मुकदमों को निर्धारित तथा गिनती करने का तरीका हर जिले में अलग-अलग है। कर्नाटक उच्च न्यायालय यातायात और पुलिस चालान को लंबित एवं निस्तारित मुकदमों की श्रेणी में नहीं रखता। बाकी सभी ऐसा नहीं करते। अदालतें इस मामले में ठीक रपट भी नहीं देती हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी एक रपट में न्याय आयोग को सूचित किया था कि 2010 में दिल्ली में माइनस 40,054 चेक संबंधी मुकदमे दर्ज हुए तथा 1,11,517 मुकदमों का निस्तारण हुआ। यह आंकड़ा बहुत अजीब और भ्रमित करने वाला था।
न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधीशों की भारी कमी है। सरकारें धन के अभाव का हवाला देकर स्थिति को और विकट बना दे रही हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर उठा ताजा विवाद भी संकेत कर रहा है कि न्यायिक व्यवस्था धीमी मौत की ओर बढ़ रही है। आज न्याय व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उसकी किडनी, हृदय, लीवर सब खराब हो गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर भी न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं। अप्रैल, 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के छह तथा उच्च न्यायालयों में 432 पद खाली पड़े थे। जिला न्यायालयों में भी न्यायाधीशों के 4,432 पद खाली पड़े थे, जो कि कुल स्वीकृत संख्या का 25 प्रतिशत है। यह बात भी गौर करने वाली है कि यदि खाली पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर भी दी जाए तो वे लोग काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत में निचली अदालतों में न्यायाधीशों के 20,502 पद स्वीकृत हैं और केवल 16,513 कमरे उपलब्ध हैं। 3,989 कमरे उपलब्ध ही नहीं हैं। न्यायिक व्यवस्था का इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है?
कालबाह्य कानूनों के कारण भी न्याय मिलने में देरी होती है और लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ जाती है। सरकार ने ऐसे 1,700 कानूनों को चिन्हित किया है तथा उन्हें निरस्त करने की प्रक्रिया पूरी होने को ही है। मुकदमों के जल्दी निस्तारण के लिए दुनियाभर में प्रयत्न हो रहे हैं। निस्तारण की समय सीमा को लेकर कई कानून भी बनाए गए हैं। भारत के सीपीसी, सीआरपीपीसी तथा अन्य कानूनों में जवाब दाखिल करने, गवाही समाप्त करने आदि के लिए तो सीमा निश्चित की गई है, पर किसी भी मुकदमे के निस्तारण की समय सीमा कानूनी तौर पर निर्धारित नहीं की गई है। अमेरिका में 1974 में यूएस स्पीडी ट्राइल एक्ट 1974 किया गया, जिसमें किसी भी मुकदमे के समाप्त होने की कानूनी सीमा भी तय कर दी गई है। भारत में ऐसे कानूनों की सख्त जरूरत है। लेकिन साधनों के अभाव में शायद ऐसा कानून भारत में कभी बन ही नहीं पाएगा। पता नहीं, समाज ने न्यायिक व्यवस्था को मारा है या न्यायिक व्यवस्था समाज को मार रही है? सच कुछ भी हो, हम सब इसके साथ मर रहे हैं। रोज-रोज मरती और जीती यह न्यायिक व्यवस्था अपनी लाश की मजार बनने के लिए अभिशप्त है।
(लेखक सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता और ह्यूमन राइट्स डिफेंस इंटरनेशनल के महामंत्री हैं)











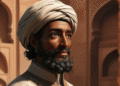
टिप्पणियाँ