|
गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। साहित्य, संस्कृति और कला की दृष्टि से समृद्धि भरे इस युग में शासक और प्रजा अपने-अपने दायित्व एवं कर्तव्य के प्रति समर्पित थे।
'जिये कांधार' नामक ऐतिहासिक उपन्यास लेखक डॉ. गणेश प्रसाद बरनवाल ने गुप्तकाल की भावभूमि पर ही रचा है। इस उपन्यास में मुख्य रूप से शक आक्रमणकारियों को पराजित करने वाले गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त और उनके पुत्र समुद्रगुप्त नायक रूप में चित्रित हैं। लगभग छह दशक तक शासन करने वाले ये पिता-पुत्र हूणों से उत्तर पश्चिमी सीमांत कांधार को बचाते हुए दिखाई देते हैं। इस उपन्यास में ऐतिहासिक घटनाओं को कल्पना मिश्रित बनाते हुए समकालीन और प्रासंगिक बनाने का प्रयत्न किया गया है। गुप्तकाल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थिति के साथ-साथ विशाल भौगोलिक क्षेत्र, विविध समुदायों का परस्पर रहन-सहन, शिक्षा- दीक्षा एवं जीवनचर्या का व्यापक विश्लेषण लेखक ने प्रस्तुत किया है। उपन्यास में आक्रांता हूणों द्वारा कांधार सहित मगध की राजधानी पाटलिपुत्र तक घुसने का वर्णन और इसी कालखंड में काठियावाड़ में शकों और मालवा के पश्चिम में पुष्यमित्र शुंग के आक्रमण का उल्लेख है। गुप्तकाल के कालखंड में लेखक ने वर्तमान समय में प्रचलित व्याधियों आतंकवाद, वर्ण-जाति व्यवस्था एवं शोषण को भी प्रतीक रूप में न केवल चित्रित किया है अपितु इन व्याधियों का युगानुकूल समाधान प्रस्तुत किया है। अपने वक्तव्य में लेखक स्वयं स्वीकारते हैं कि उपन्यास की भावभूमि भले ही ऐतिहासिक हो किन्तु मुद्दे और परिस्थितियां आज के भारत की ही हैं जहां भ्रष्ट और अवसरवादी परिवार एवं जाति आधारित राजनीति के ठेकेदार देश और समाज को ताक पर रखकर व्यक्तिनिष्ठा का प्रमाण देते हैं- खंडित सोच, विभाजितनिष्ठा एवं पश्चिम का अंधानुकरण स्वतंत्र भारत के पीढ़ी-दर-पीढ़ी युवा वर्ग को भारत, भारती, भारतीयता से परांगमुख करते जा रहे हैं। भारत की अस्मिता पर द्यूतजीवियों की लोलुप दृष्टि आ गड़ी है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी की स्मृतियां आनुष्ठानिक बन गई हैं। राष्ट्रवादी साहित्य को नसबंदी कक्ष में पहुंचा दिया गया लगता है।' लेखक ने उपन्यास के माध्यम से ब्राह्मणों और श्रमणों के परस्पर संघर्ष को भी बखूबी चित्रित किया है। चक्रवर्ती सम्राट कुमारगुप्त का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा के किनारे तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में सिन्धु तक फैला था। जिस गुरुकुल में विद्यार्जन करने कुमार स्कन्दगुप्त जाते हैं उसकी और उसके कुलपति पर चर्चा के संदर्भ में ब्राह्मणों और श्रमणों के मध्य विद्यमान द्वन्द्व पर सम्राट कहते हैं- 'महामात्य जी' इतने बड़े साम्राज्य तथा बहुलतामुखी समाज में शांति तथा सामान्य स्थिति शासक को आत्मसंतुष्टि से आगे अकर्मण्य बना देती है जो किसी भी प्रकार वांछित नहीं है' उपन्यास में सम्राट की आकांक्षा व इच्छा को साकार करने हेतु गुप्तकाल की अमूल्य स्मृति के रूप में 'आर्यभट्ट भारतीय विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना' का प्रसंग है, जिसके निर्माण में सम्राट आमजन की सहभागिता का आह्वान करते दिखाई पड़ते हैं- 'भारत की अध्यात्म तथा विज्ञान की शतियों से समानान्तर प्रवहमान महान परंपरा का यह प्रतिनिधि प्रतीक आप सबके सहकार से जीवंत हो, यह मेरी अभ्यर्थना तथा अभिलाषा है।' राष्ट्र के ऐसे कालजयी स्मारक के लिए तत्कालीन समय में विद्यमान गांधार शैली, मथुरा, अजंता, मगध व दक्षिणांचल शैलियों के समावेश की बात और देश के कुशलतम स्थापत्यविदों और शिल्पियों की खोज का विशेष उल्लेख है।
आठ वर्ष तक गुरुकुल में अध्ययन करने के उपरांत स्कन्दगुप्त अपने मित्र एकलक्ष्य के साथ जीवन के अगले पड़ाव में पहुंचते हैं। उपन्यास के प्रथम खंड में अवांतरिका पाटलिपुत्र और नालंदा जैसे परंपरागत सांस्कृतिक केन्द्रों का व्यापक वर्णन किया गया है। राजा किस प्रकार जनता में छोटे-छोटे विषयों और मुद्दों में रुचि लेकर उसका क्रियान्वयन करते थे इसका प्रमाण भी इसमें प्राप्त होता है, स्थानीय मेले की तैयारी और सेतु एवं सड़क के निर्माण में गुणवत्ता को सर्वोपरि रखने का प्रमाण मिलता है। 'कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि यात्रियों को सेतु के कारण कोई क्षति होती है तो यह निर्माण समिति की कार्यक्षमता को अपयश का भागी बना देगा' और तो और राजा मेले में आने वाले पशुओं के चारे और आवागमन की सुविधा आदि की भी चिंता करता था- 'इस बिन्दु को ध्यान में रखकर निकटवर्ती जनपदों, ग्रामांचलों, वनांचलों से आहार की आपूर्ति हेतु पारिश्रमिक पर मध्यस्थ का सहयोग लिया गया है इसलिए आहार की आपूर्ति निर्बाध रहेगी, ऐसी आशा की जा सकती है।' उपन्यास के द्वितीय खंड में अवन्ति-मालवा अध्याय से प्रारंभ कर संक्रांतिक, जिये कांधार और उत्तरा नामक पाठों में कथा विस्तार किया गया है।
उपन्यास में जय जवान-जय किसान का नारा चरितार्थ होता दिखाई पड़ता है। एकलक्ष्य महामात्य पृथवीषेण को बताता है कि- 'शक्ति संतुलन में जवान की (सैनिक की) प्रमुख भूमिका होती है, परंतु शांतिकाल में जवान के साथ ही किसान जब योगदान करता है तब राज्य के विकास का चक्र गतिमान होता है।' राजभवन में हूण राजकुमारी शेरविना के प्रवेश पर स्कन्दगुप्त और एकलक्ष्य के मध्य संस्कारों पर चर्चा होती है- 'संस्कारों की जो बेल न जाने कब से भारतीय जनजीवन के बिटप पर पल्लवित पुष्पित होती चली आ रही है उसमें एक विजातीय को प्रवेश पाना तथा देना थोड़ा दुस्साध्य तो होगा ही।' इसी प्रकार परंपरा को आत्मसात करने का संदेश दिया गया है- 'वत्स'परंपरा के प्रारंभ को असहमति से साक्षात् तो करना ही होता है। फिर धीरे-धीरे समाज उसे आत्मसात कर लेता है।'
कुल मिलाकर यह उपन्यास रोचक एवं पठनीय है। इसमें वर्णित पात्र एवं चित्रित स्थल ऐतिहासिक होते हुए भी वर्तमान जीवन के प्रतीकों से जुड़कर जीवंत दिखाई पड़ते हैं। 'जिये कांधार' शीर्षक भारत की प्राचीन संस्कृति की विश्व व्यापकता का जीवंत दस्तावेज प्रमाणित होता है, संस्कृति, परंपरा, साहित्य एवं इतिहास के अध्येताओं को यह उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए।
– सूर्य प्रकाश सेमवाल










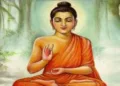

टिप्पणियाँ